
दिनेश चौधरी
: प्रमोशन की चिट्ठी और बर्खास्तगी के आदेश में से बर्खास्त होना चुना था कामरेड टीएन दुबे ने : 14 साल तक नौकरी से बाहर रहे, तब तने रहे, केस जीतकर नौकरी में लौटे तो टूट गए : बेगम अखतर को सुनते हुए फूट-फूट कर रोने लगे : धीरे-धीरे रोना उनके स्वाभाव का स्थायी भाव बनने लगा : उखाड़े गए पौधे की जड़ों की तरह वे उसी जमीन की सुपरिचित गंध की तलाश में छटपटाते रहे : कामरेड दुबे तकलीफ में थे और कामरेड चौबे दुविधा में : यह घर कम, आने वाले दिनों में होने वाली क्रांति का कंट्रोल रूम ज्यादा था : जमाने में इंकलाब के सिवा और भी गम थे : आखिरी बार देखकर मुस्कुराए थे पर कोई शेर नहीं कहा, कहने को अब बचा ही क्या था? : ”फैज दिलों के भाग में है घर बसना भी लुट जाना भी / तुम उस हुस्न के लुत्फो-करम पर कितने दिन इतराओगे” :
शायरों से या शायरी से ट्रेड यूनियन आंदोलन के अपने वरिष्ठ साथी एम.एन. प्रसाद का कोई दूर का भी रिश्ता नहीं है। मगर फिर भी उन्होंने मुझसे कहा कि ”आओ, तुम्हें एक पागल शायर से मिलाता हूं।” साइकल कंपनी की किसी सिरीज का पहला मॉडल रहा होगा, जिस पर यह शायरनुमा व्यक्ति सवार था, हालांकि पागलपन के कोई लक्षण नहीं थे। लंबे, काले व सफेद खिचड़ी बाल जो तेल की पर्याप्त मात्रा के कारण उनके चेहरे की ही तरह चमक रहे थे। क्रीम -पाउडर वाले चाहे कितना भी हल्ला मचायें, ऐसी चमक सिर्फ मेधा के कारण आ सकती है। सफेद कुर्ता-पाजामा और कंधे पर भूदानी झोला। झोले में गोलाकार बंडल बनाये हुए पोस्टर। थोड़ी जल्दबाजी में लग रहे थे। मैंने उनसे हाथ मिलाया और शिष्टाचारवश पूछा, ”कहां निकले हैं?” दुआ न सलाम, उन्होंने सीधे शेर दागा, ” मुकाम फैज़ कोई राह में जंचा ही नहीं/ जो कू-ए-यार से निकले तो सू-ए-दार चले।” दायें पैर के घुटने से उन्होंने साइकल के पैडल पर जोर लगाया और यह जा वह जा।
कामरेड टी.एन. दुबे से यह मेरी पहली मुलाकात थी। यूनियन के किसी जलसे का पोस्टर लगाने निकले थे। लौटकर आए तो एकदम गले लग गये, जैसे बरसों से जानते हों। उन्हें खुशी इस बात की थी कि एक कमउम्र लड़का उनकी उस यूनियन में शामिल हुआ है, जिसे उन्होंने अपने खून-पसीने से सींचा है। वर्किंग कमेटी मीटिंग थी, जहां सिर्फ रिपोर्टिंग वगैरह होती है। मगर उन्होंने भाषण जैसा दिया। शेरो-शायरी भी थी। यूनियन में नया व कच्चा होने के बावजूद मैंने नोट किया कि वे बहक रहे हैं। मगर उनका बहकना लाजमी था। वे नेता नहीं थे, कार्यकर्त्ता थे। ऐसा कार्यकर्त्ता जो दिमाग से नहीं, दिल से काम करता है। ताउम्र करते रहे। और इसलिए ही जब इस असार संसार से कूच किया तो उसका सबब भी यही नामुराद दिल बना। मगर मैं जानता हूं कि यह उनके जाने की उम्र नहीं थी। यह भी कि उन्होंने अपने -आपको थोड़ा-थोड़ा खत्म किया। अंदर ही अंदर रिसते रहे, घुटते रहे, रोते रहे। इंकलाबी भाषण देने वाले, क्रांतिकारी मजदूर नेता-कार्यकर्त्ता का यह बिल्कुल अलहदा, अंतरंग पहलू था जिससे या तो मैं वाकिफ हूं या कामरेड चौबे।
कम लोगों को पता है कि ७४ की ऐतिहासिक रेल हड़ताल के लिये हीरोगिरी छांटने वाले जार्ज फर्नांडिज ने असल में रेल-मजदूरों को डुबाने का काम किया। दुबे जी जैसे हजारों कार्यकर्त्ता थे, जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर कभी नहीं आयेगा पर जिनके कारण ७४ की रेल हड़ताल संभव हो पायी। जार्ज ने रेल मजदूरों के आंदोलन का सत्यानाश करने का काम किया। ऐसा किया कि ७४ के बाद रेल में कोई आम हड़ताल नहीं हो पायी। मगर मैं बात दुबे जी की कर रहा हूं। कामरेड दुबे। एक पागल शायर। शायर कम, पागल ज्यादा। ऐसा पागल, जिसे कहते हैं कि हड़ताल तोड़ने के लिये प्रमोशन की चिट्ठी और बर्खास्तगी का आदेश एक साथ सौंपा गया- विकल्प चुनने की सुविधा के साथ। उन्होंने बर्खास्तगी का विकल्प चुना और १४ साल तक नौकरी से बाहर रहे। झुके नहीं। चेहरे पर शिकन तक नहीं आयी। फिर इतना मजबूत इंसान नौकरी में वापस आकर क्यों टूट गया?
इस सवाल का जवाब मुझे काफी अरसे बाद मिर्ज़ा गालिब के जरिये मिला, लेकिन इसका खुलासा मैं आगे चलकर करूंगा। दुबे जी वर्ष १९८१ में नौकरी से हटाये गये थे। वे मस्तमौला किस्म के इंसान थे, इसलिए नौकरी की परवाह उन्होंने कभी की नहीं। खाने-पीने के शौकीन थे, पर दाल-रोटी से ज्यादा की अपेक्षा नहीं करते थे। कुछ विक्टीमाइजेशन फंड इकट्ठा होता था, जिसका एक हिस्सा उनको जाता। उनकी श्रीमती जी और हमारी आदरणीया भाभी जी अचार, पापड़, बड़ी वगैरह बनाकर साथियों के यहां दे आतीं और बची-खुची जरूरतें पूरी हो जातीं। बच्चों की पढ़ाई में उन्होंने किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी। वैसे भी उन दिनों पढाई इतनी ज्यादा मंहगी थी नहीं। वे लॉबी जाते, साथियों को इकट्ठा करते, शेरो-शायरी करते, बिना दूध की अधप्याली चाय के सहारे अड्डेबाजी करते, विश्व बैक और अंरराष्टीय मुद्रा कोष को गरियाते, दलाल यूनियनों व अफसरों की मां-बहन एक करते और बचा हुआ समय अपने सबसे प्रिय शगल, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज को पढ़ने में व्यतीत करते।
कुल मिलाकर कामरेड दुबे का मन फकीरी में पूरी तरह रम गया था। कोई और समझदार -दुनियावी इंसान होता तो १४ महीनों में ही त्राहि-त्राहि करने लगता, पर वे पूरी तरह मस्त थे और पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि वे इस स्थिति से परिवर्तन चाहते भी नहीं थे। वे ”कर्ज की पीते थे मय और कहते थे कि हां / रंग लायेगी हमारी फाकामस्ती एक दिन” के उसूलों पर चलना चाहते थे। पर नियति को उनकी मिर्जा गालिब की यह शागिर्दी पसंद नहीं आयी। उनका हश्र बहादुर शाह जफर जैसा हुआ।
अस्सी का दशक खत्म होने को था। इलाहाबाद का उपचुनाव जीतने के बाद वी.पी. सिंह ने राजीव गांधी के तख्ता-पलट की तैयारी कर ली थी। दायें-बायें दोनों छोरों से उन्हें सहयोग व समर्थन मिल रहा था। जब उनकी सरकार बनी तो जार्ज साहब रेलमंत्री बने। रेलवे के नौकरशाहों की भवें चढ़ गयीं। एक हड़ताली नेता को रेलमंत्री का ओहदा, यानी बिल्ली से दूध की रखवाली! दुबे जी के साथ कोई ७०० रेल कर्मचारी नौकरी से बाहर थे। रोज रेडियो सुना जाता या अखबार देखे जाते कि आज जार्ज साहब बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली की घोषणा करेंगे। मगर जार्ज साहब अपने खेल में लगे थे। दुबे जी से रिएक्शन मांगा तो उन्होंने अपने अंदाज में कहा, ”हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन / खाक हो जायेंगे हम उनको खबर होने तक।” ठीक यही हुआ।
जार्ज साहब ने बर्खास्त रेल कर्मचारियों की बहाली की घोषणा तो की लेकिन ऐन उसी दिन जिस दिन लालू यादव ने रथ यात्रा को रोकते हुए लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया और यह तय हो गया कि सरकार बस अब गिरने ही वाली है। बाद में -जैसा कि अंदेशा था -सरकार ने जार्ज के ऐलान को आदेश में बदलने से साफ इंकार कर दिया। दुबे जी नौकरी में वापस आये सुप्रीम कोर्ट के दखल से। यह रेलवे की बड़ी हार थी, जिसका बदला उन्होंने कर्मचारियों की बहाली के बाद तबादले के रूप में लिया। दुबे जी के बहादुर शाह जफर मार्ग पर चलने की शुरुआत यहीं से हुई।
संयोग से दुबे जी का तबादला वहां हुआ जहां हम पहले से तैनात थे। हम खुश थे कि हमें एक जुझारू और कर्मठ कार्यकर्त्ता मिल गया है और हम अपनी लड़ाई को धार दे सकते हैं। पर हमें दुबे जी की मनःस्थिति का अंदाजा नहीं था। यह बात पहले भी हजारों बार कही गयी होगी ओर मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं कि कुछ पौधों को जब जमीन से उखाड़ कर नयी जगह पर रोपा जाता है, तो चाहे जितना भी खाद-पानी उन पर खर्च किया जाये, वे पनपने से इंकार कर देते हैं। उनकी जड़े उसी जमीन की सुपरिचित गंध की तलाश में छटपटाती रह जाती हैं, जहां से उन्हें उखाड़ा गया था। दुबे जी कुछ ऐसी ही प्रजाति के थे। उनकी आत्मा कलपती थी उस जगह के लिये जहां वे क्रांति के सपनों को अंजाम देने के लिये रोज सुबह भूदानी झोला लेकर निकल पड़ते थे, जहां लेमन टी के साथ अड्डेबाजी की जाती थी, जहां उनके हमप्याला-हमनिवाला साथ हुआ करते थे, जहां की दीवारें उनके पोस्टर लगाने वाले हाथों को पहचानने लगी थीं।
मैंने अर्ज किया कि वे दिल से काम करते थे और उनके दिल ने इस बात को मानने से साफ इंकार कर दिया था कि क्रांति का केंद्र कोई और स्थान भी हो सकता है। यह बात दिमाग से काम करने वाले वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेताओं के समझ से परे थी क्योंकि क्रांति की उनकी व्याख्या मार्क्स और लेनिन के संदर्भो में होती थी जबकि दुबे जी अपनी व्याख्या को मिर्जा गालिब से किनारा किये बगैर फैज के स्तर से आगे नहीं ले जाना चाहते थे। वे कफस में फकत जिक्रे-यार ही चाहते थे और गमे-जानां को किसी भी सूरत में गमे-दौरां से कमतर आंकने के मूड में नहीं थे। १४ साल नौकरी से बाहर रहने पर जिनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आयी वही दुबे जी तबादले की वापसी के लिये खुलेआम अपने ही नेताओं को कोसने लगे थे।
दुबे जी अपने कस्बे में जब रहने के लिये आये तो एक पुरानी अटैची व झोले के साथ रेलवे चौक में पहुंचे। थोड़े सहमे हुए से थे कि पता नहीं यह अजनबी शहर एक निर्वासित मजदूर नेता के साथ कैसा सलूक करता है। मैंने घर चलने का प्रस्ताव रखा तो वे अपने मूल रूप में आ गये-” कुछ हम ही को नहीं एहसान उठाने का दिमाग / वो तो जब आते हैं माइल-ब-करम आते हैं।”
घर आये तो बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें पता था कि एक क्रांतिकारी किस्म के इंसान की बुनियादी जरूरतों के तमाम इंतजामात यहां पर मौजूद हैं। फैज व ब्रेख्त की किताबें थी, लेनिन का स्केच था, बंगाल के विष्णुपुर से मंगायी मार्क्स की मूर्ति थी, पोस्टर तैयार करने के लिये रंग व कूची थी, मुक्तिबोध व धूमिल की कवितायें थी, ट्रेड यूनियनों की बैठके थीं, ‘इप्टा’ के नाटकों की तैयारियां थी और रात-दिन तमाम किस्म के लोगों का आना -जाना था। गरज यह कि यह घर कम, आने वाले दिनों में होने वाली क्रांति का कंट्रोल रूम ज्यादा था और मुझे ठीक-ठीक तो याद नहीं पर लगता है कि उन दिनों चलते वक्त हमारे पांव जमीन से कोई चार-पांच ईंच ऊपर ही पड़ते रहे होंगे।
कुछ दिनों तक तो दुबे जी को कोई समस्या नहीं रही। सब कुछ उनके मन के मुताबिक ही चल रहा था। वे हमारी बैठकों के स्थायी अध्यक्ष थे। यहां भी अड्डेबाजी जमने लगी। शेरो-शायरी की उनकी खयाति भी फैलने लगी थी। उनका खोया हुआ हास्य-बोध फिर से जागृत हो गया था। अपनी औसत से ज्यादा लंबाई व श्रीमती जी की कदरन कुछ कम ऊंचाई, खुद उनके लिये हंसने का एक बड़ा जरिया था। वे अपनी तुलना टेलीविजन के एंटीना से करते और कहते कि –
में एंटीना हूं
ये मेरी पोर्टेबल टीवी है
मैं खड़ा रहता हूं तनकर धूप व बारिश में
लू व आंधी में
हवाओं के थपेड़े सहते
कौवे मुझ पर बीट कर जाते हैं
पर कोई नजर भी उठाकर नहीं देखता
सब इसे ही देखते हैं
नजरें गड़ाकर
घूरते हैं मेरी ही छाया तले…
हंसने-हंसाने का यह सिलसिला बहुत दिनों तक नहीं चल पाया। वे अपनी ही छवि के शिकार थे इसलिए शायद दिल की बात लबों पर नहीं ला पा रहे थे। उदासी उनके अंदर घर करने लगी थी और हमने कई बार उनसे कहा कि भाभी जी को यहीं ले आयें और नये सिरे से जिंदगी की शुरूआत करें। पर पता नहीं क्या मजबूरी थी कि वे आना नहीं चाहती थीं। कामरेड दुबे उन्हें बेइंतिहां चाहते थे। हरेक दूसरी-तीसरी बात में उनका जिक्र होता। वे चौबीसों घंटे घर की यादों के साये में रहने लगे। चेहरे की चमक जाती रही। गालों में पड़े हुए गड्ढे उभरने लगे। खिचड़ी बालों में सफेद केशों का अनुपात बढ़ने लगा। चुप-चुप-से रहने लगे और एक दिन सब्र का बांध टूट गया।
बारिशों के दिन थे। मैं उनके साथ अपने घर की सीढि़यां चढ रहा था। सीढियों और दीवारों पर हरे रंग की काई उग आयी थी। थोड़ी-सी फिसलन -सी भी थी। दुबे जी के अंदर से आवाज आयी -” उग रहा है दरो-दीवार पर सब्जा गालिब/हम वीराने में हैं और घर पर बहार आयी है।” उनकी आवाज में कुछ ऐसी पीड़ा थी कि मैं अंदर तक हिल गया था। घर की यादों ने उन्हें भीतर से खोखला कर दिया था और यह आवाज इसी सुरंग से होकर निकली थी। इस शेर को मैंने हजारों बार पढ़ा व सुना होगा पर इसके पीछे छुपे एहसास को इतनी शिद्दत के साथ शायद मैं पहली बार महसूस कर पाया था। घर आकर दोनों चुप-से बैठे थे। मैंने माहौल को हल्का करने की कोशिश की और कहा कि चाय बनाता हूं। चाय चढ़ाने के लिये जाने से पहले अपनी आदत के अनुसार कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। बेगम अखतर की आवाज में शकील बदायूनी की ग़ज़ल थी –
मेरे हमनफस, मेरे हमनवा मुझे दोस्त बनकर दगा न दे
मैं हूं दर्दे-इश्क से जां -ब-लब मुझे जिंदगी की दुआ न दे
मेरे दागे-दिल से है रोशनी इसी रोशनी से है जिंदगी
मुझे डर है ऐ मेरे चारागर ये चिराग तू ही बुझा न दे
मुझे ऐ छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारागर
ये तेरी नवाजिशे-मुखतसर मेरा दर्द और बढ़ा न दे
मै चाय चढाकर लौटा तो अचानक विस्फोट जैसा हुआ। उनके जब्त का हौसला टूट चुका था। वे फूट-फूट कर रो रहे थे। गलती या लापरवाही मेरी थी जो मैंने ऐसे संजीदा माहौल को और गमगीन करने वाली ग़ज़ल चला दी थी। मुझे गरज सुर-ताल से थी पर वे एहसास में डूबने-उतराने लगे थे। वे उम्र और तजुर्बें दोनो में मुझसे बहुत बड़े थे। मैं उन्हें ढाढस बंधाता भी तो कैसे बंधाता? मुझे यह भी नहीं सूझा कि कम से कम उनकी पीठ सहला दूं। जैसे किसी बच्चे ने कोई कीमती चीज तोड़ कर अभी -अभी डांट खायी हो, इस तरह चुपचाप खड़ा रहा। वे बदस्तूर रोते रहे। जी कुछ हल्का हुआ तो खुद ही चुप हुए। कुरते की बांह से आंसू पोछे। रेलवे को मां की गाली दी और मुंह धोने के लिये बाहर चले गये।
इस घटना का सबसे खराब परिणाम यह निकला कि हम लोगों के सामने रोने की उनकी झिझक जाती रही। यह उनके स्वाभाव का स्थायी भाव बनने लगा। वे क्रांतिकारी से दयनीय बनने लगे। चाहे जब फूट पड़ने की उनकी आदत से हम असहज होने लगे और कोशिश करते कि उनके साथ कम से कम रहें। इस बीच मेरा तबादला दूसरी जगह हो चुका था। मैं कामरेड दुबे को कामरेड चौबे के हवाले कर चुका था या दूसरे शब्दों में कहूं तो दुबे जी और चौबे जी के बीच से जान छुड़ाकर निकल चुका था।
अब केवल रविवार को मेरा आना होता था। कामरेड चौबे थोड़े अक्खड़ मिजाज किस्म के जीव हैं पर बाज मौकों पर इतनी औपचारिकता बरतते हैं कि खीझ होने लगती है। वे कुछ कह तो नहीं रहे थे पर मैं महसूस करने लगा था। दुबे जी हमनफस थे, हमनवा थे, हमखयाल थे पर हमउम्र नहीं थे। हमारे व उनके बीच उम्र का एक लंबा फासला था जो हर समय एक लिहाज की मांग करता था। हम बंधे हुए-से महसूस करने लगे। आखिरकार क्रांति की बातें चौबीसों घंटे तो नहीं की जा सकतीं। जमाने में इंकलाब के सिवा और भी गम थे।
स्थायी हल के लिये मैंने दुबे जी से भाभी जी को लाकर सेटल होने के बात कही। वे भी यही चाहते थे पर कहना मुश्किल है कि उनके बीच क्या था? मामला लंबा खिंच रहा था। इस बीच दुबे जी ने घर का खर्च शेयर करने का ऑफर हमें दिया। हमने इंकार कर दिया। पर यह हमारी विनम्रता नहीं थी, हमारा बड़प्पन नहीं था- विशुद्ध कमीनापन था। चिंता थी कि घर का खर्च शेयर करके कहीं वे ‘टिक’ न जायें। दुबे जी ने जमाने को देखा था- ” हम इक उम्र से वाकिफ हैं हमें न सिखाओ मेहरबां / कि लुत्फ क्या है और सितम क्या है।” वे चीजों को समझ रहे थे पर मैंने अर्ज किया कि वे हमेशा अपने दिल की पुकार सुनते थे ओर उनका दिल कह रहा था कि यहां से चले गये तो मुश्किल होगी। वे बार-बार मुझसे कहते कि कामरेड चौबे से घर के खर्च को शेयर करने के लिये कहो। मैं क्या करता? कामरेड दुबे तकलीफ में थे और कामरेड चौबे दुविधा में। मैंने चुप रहकर यथास्थिति बनाये रखी क्योंकि इस समस्या का कोई हल तो था ही नहीं।
हल दुबे जी के पास भी नहीं था। उन्होंने अपने उस्ताद फैज साहब से पूछा। फैज साहब एक दिन दबे पांव आये और चुपके-से उनके कानों में कहा -”फैज दिलों के भाग में है घर बसना भी लुट जाना भी / तुम उस हुस्न के लुत्फो-करम पर कितने दिन इतराओगे।” दुबे जी ने अपनी अटैची और झोला समेट लिया। वे अलग रहने के लिये चले गये। हमने उन्हें रोका नहीं और सिर्फ इसी वजह से – अल्लाह माफ करे- हमें हमेशा ऐसा लगता रहा कि हमने उन्हें अपने घर से निकाल दिया है। हालांकि हमारे बीच सिर्फ छतें बदली थीं, और कुछ नहीं बदला था, पर हम हमेशा एक अपराध-बोध में रहे। बाद में भाभी जी भी आकर उनके साथ रहीं। रिटायरमेंट के बाद दुबे जी बहुत दिनों तक नहीं चल पाये। आखिरी बार उन्हें अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस के एसी कोच में चढते हुए देखा था। बाईपास सर्जरी हुई थी। बेहद कमजोर लग रहे थे। भाभी जी भी साथ में थी। देखकर मुस्कुराए पर कोई शेर नहीं कहा। कहने को अब बचा ही क्या था?
लेखक कामरेड दिनेश चौधरी इप्टा से जुड़े हुए हैं और एक मैग्जीन में भी कार्यरत हैं. उनसे संपर्क [email protected] के जरिए किया जा सकता है.














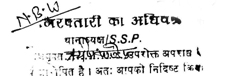
यशवंत सिंह
October 4, 2010 at 6:32 am
का महराज.
आपको तो पढ़ने के बाद एक बार को आदमी संज्ञाशून्य हो जाता है. जैसे लगता है कि उसी की कहानी आप बयान कर रहे हैं.
दिनेश भाई, दरअसल हर आदमी में बहुत प्यारा व बहुत अच्छा दिल होता है. ज्यादातर लोग दुनियादारी में उस दिल को दलित बना देते हैं, थोड़े बहुत लोग अपने दिल को अपना सम्राट घोषित कर खुद जिंदगी भर चक्कर काटते रहते हैं. लेकिन यह चक्कर भले दुनिया को घनचक्कर वाला लगे, पर पूछें उनके दिल से जिन्हें राजपाठ भाता नहीं, आधी रात में गौतम बुद्ध की माफिक सब छोड़कर कहीं कुछ खोजने निकल जाने को तत्पर रहते हैं. ऐसे ही लोग हैं जिन्हें अब तक का कठिनतम अर्थशास्त्र मुनाफे का मतलब समझा नहीं सका, सबसे बड़ी तोपें उन्हें उड़ा न सकीं, सबसे बड़ी व खूंखार जेलें कैद न कर सकीं, सबसे तेज गति से चलने वाली राइफलें छलनी न कर सकीं. बड़े से बड़े सरकार लोग मुंह बंद न करा सकें. क्योंकि ये लोग जिस्म होते ही नहीं, ये तो रूह की शक्ल लिए जिस्म होते हैं, कभी इस जिस्म में कभी उस जिस्म में. ये जिंदा प्लैटोनिक लवमैन होते हैं, जिन्हें मैं कहता हूं असली ही-मैन होते हैं, बाकी बचे हुए सब हू मैन होते हैं, हू-मैन बोले तो एक क्वेश्चन मार्क की माफिक दिखता आदमी.
आपका लिखा पढ़कर आपके बारे में, खुद के बारे में सोचने लगता हूं. साथ-साथ आपके-अपने जैसे कुछ और वरिष्ठ-कनिष्ठ साथियों के बारे में सोचने लगता हूं. रूह ही तो है, कभी इस शरीर में तो कभी उस शरीर में. कभी वो हंसा तो ये रोया. कभी वो रोया तो ये हंसा. कभी दोनों रोने लगे. तो अन्य दो चुप कराने लगे. ये आंसू इनकी आंखों के नहीं हैं. सदियों से चली आ रही अदभुत मानवीय परंपराओं-संवेदनाओं के आंसू हैं जिन्हें बार-बार नियम-कानून बनाकर सुखा दिया जाता है. क्या-क्या कहूं. लिखता रहूं तो एक आलेख तैयार हो जाए और कमेंट से हटाकर पोस्ट करने के बारे में सोचने लगूं. इस झंझट से बचते हुए विषय बदलता हूं.
हां, वो कमेंट पढ़ा, लफंटूस वाला 🙂
उनसे कहिए, सच है भाई, दिल्ली के लफंटूस ही हैं यशवंत, क्योंकि ऐसा बने रह पाने में जो सुख मिल रहा है यशवंत को, वो शराफत की राह पकड़ने के लिए मिले जाने कितने छोटे-बड़े मौकों में महसूस न कर सका. फटी बिहाई वाले ही पीर पराई जानते हैं, उसी तरह लफंटूस लोग ही जिंदगी के ताले की चाभी के पास पहुंच पाते हैं.
खैर, उन्हें क्या समझाना जो घोषित तौर पर (ना)समझदारी का सार्टिफिकेट रखे हुए हैं. खुद को क्या समझना जब घोषित तौर पर (आ)वारा-न्यारा करने को हर पल तैयार बैठे हुए हैं. 🙂
आभार
यशवंत सिंह
Sankalp
October 5, 2010 at 2:55 pm
Dear Yashwant ji,
“There are countless ways of attaining greatness, but any road to reaching one’s maximum potential must be built on a bedrock of respect for the individual, a commitment to excellence, and a rejection of mediocrity.”
Thats why I feel Let Mr.Dinesh should be left in exile for better creativity.
Regards
amitabh shukla
October 9, 2010 at 1:23 am
hi dinesh,
i can’t understand which part of your writing hurt mr.sankalp .that he has written in such bad english.very difficult to understand what he says.bahut achcha lekh hai.ghalib aur faiz chacha ki yad dila di.kafi imandari se likha hai .
happy writings.
amitabh
DEEPAK CHOUDHARI
October 9, 2010 at 3:30 am
sanvedanaun ke es estar ko chchune wale vyakti se puchcho ki gabhirata ki chadar odhakar usne apne maan ke pariwarik, samajik, mansik, bhawatmak aur arthik jaruraton ko nazar andaj kyun kya. mansik aiyyashi aur anubhuti ham bhi samjhate hain.
sankalp
November 16, 2010 at 6:45 pm
Dear Amitab ji,
Aap ne thiek hi likha ki meri angreji achi nahin hai.Par apne meri baat ka galat arth nikala.Main to sahab dinesh bhai ki tareef karne ki kosisih kar raha tha.
Namaskar
sankalp
November 16, 2010 at 6:45 pm
Dear Amitab ji,
Aap ne thiek hi likha ki meri angreji achi nahin hai.Par apne meri baat ka galat arth nikala.Main to sahab dinesh bhai ki tareef karne ki kosisih kar raha tha.
Namaskar