 धंधे में सीधे शिरकत करने वाला सफल मीडियाकर्मी! : मीडिया से कौन निकल कर कहेगा कि माई नेम इज गणेश शंकर विद्यार्थी और मैं पत्रकार नहीं हूं : लोकतंत्र के चार खम्भों में सिनेमा की कोई जगह है नहीं, लेकिन सिल्वर स्क्रीन की चकाचौंध सब पर भारी पड़ेगी यह किसने सोचा होगा। “माई नेम इज खान” के जरिये सिनेमायी धंधे के मुनाफे में राजनीति को अगर शाहरुख खान ने औजार बना लिया या राजनीति प्रचार तंत्र का सशक्त माध्यम बन गयी, तो यह एक दिन में नहीं हुआ है। एक-एक कर लोकतंत्र के ढ़हते खम्भों ने सिनेमा का ही आसरा लिया और खुद को सिनेमा बना डाला। 1998-99 में पहली बार बॉलीवुड के 27 कलाकारों ने रजनीति में सीधी शिरकत की। नौ बड़े कलाकारों से राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने संपर्क साधा और उन्हें संसद में पहुंचाया, 62 कलाकारों ने चुनावी प्रचार में हिस्सा लिया। और, 2009 तक बॉलीवुड से जुड़े 200 से ज्यादा कलाकार ऐसे हो गये, जिनकी पहुंच-पकड़ अपने-अपने चहेते दलों के सबसे बड़े नेताओं के साथ भी सीधी हो गयी।
धंधे में सीधे शिरकत करने वाला सफल मीडियाकर्मी! : मीडिया से कौन निकल कर कहेगा कि माई नेम इज गणेश शंकर विद्यार्थी और मैं पत्रकार नहीं हूं : लोकतंत्र के चार खम्भों में सिनेमा की कोई जगह है नहीं, लेकिन सिल्वर स्क्रीन की चकाचौंध सब पर भारी पड़ेगी यह किसने सोचा होगा। “माई नेम इज खान” के जरिये सिनेमायी धंधे के मुनाफे में राजनीति को अगर शाहरुख खान ने औजार बना लिया या राजनीति प्रचार तंत्र का सशक्त माध्यम बन गयी, तो यह एक दिन में नहीं हुआ है। एक-एक कर लोकतंत्र के ढ़हते खम्भों ने सिनेमा का ही आसरा लिया और खुद को सिनेमा बना डाला। 1998-99 में पहली बार बॉलीवुड के 27 कलाकारों ने रजनीति में सीधी शिरकत की। नौ बड़े कलाकारों से राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने संपर्क साधा और उन्हें संसद में पहुंचाया, 62 कलाकारों ने चुनावी प्रचार में हिस्सा लिया। और, 2009 तक बॉलीवुड से जुड़े 200 से ज्यादा कलाकार ऐसे हो गये, जिनकी पहुंच-पकड़ अपने-अपने चहेते दलों के सबसे बड़े नेताओं के साथ भी सीधी हो गयी।
गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्यप्रदेश के विधानसभा से लेकर आम चुनाव के दौरान सिल्वर स्क्रीन के करीब छोटे-बडे तीन सौ से ज्यादा कलाकारो ने प्रचार भी किया और अपने हुनर से नेताओ की सभा को बांधा भी रखा। कलाकारों के वक्त के लिहाज से नेताओ को अपना वक्त निकालना पड़ता लेकिन आम जनता के लिये नेताओ के पास वक्त ही नहीं रहता। मुश्किल तो यह हुई कि इस दौर की राजनीति को इसमें कोई खामी भी दिख रही। 26-11 के बाद ताज होटल का निरीक्षण करने निकले तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख का फिल्मकार रामगोपाल वर्मा को अपने साथ ले जाना इसका एक उम्दा उदाहरण है। जब देशमुख पर आरोप लगे तो उन्होंने मासूमियत से कहा- इसमें गलती क्या है। सत्ताधारी राजनीतिक दलों से जुड़े होने का लाभ नौकरशाही ने भी कलाकारों को खूब दिया। सुविधा, टैक्स माफ और राष्ट्रीय पुरस्कार दिखायी देने वाला सच है। और ना दिखायी देने वाली हकीकत यही रही कि राजनीति भी सिनेमायी तर्ज पर खुद को देखने-समझने लगी।
दरअसल, यह पूरा दौर आर्थिक सुधार का है, जिसमें सबसे ताकतवर बाजार हुआ और हर हालत में मुनाफे की सोच ने सामूहिकता के बोध खत्म कर दिया। इस दौर में कल्याणकारी राज्य यानी जनता के प्रति जवाबदेही होने की समझ भी राजनीतिक सत्ता से काफूर हो गयी। सबकुछ प्रतिस्पर्धा बताकर मुनाफे पर टिकाने का अद्भुत खेल शुरु हुआ। इस राजनीतिक शून्यता ने समाज में एक संदेश तो साफ दिया कि संसदीय राजनीति का लोकतंत्र भी अब मुनाफे की बोली ही समझता है। इन परिस्थितियों को समझते हुये समझाने की जरुरत चौथे खम्भे यानी पत्रकारिता की थी। लेकिन पत्रकारिता ने भी आर्थिक सुधार के इस दौर में बाजार और मुनाफे का पाठ ही पढ़ना शुरू किया। जिस राजनीतिक सत्ता पर उसे निगरानी रखनी थी, उसी सत्ता की चाटुकारिता उसके मुनाफे का सबब बनी। और पत्रकारिता झटके में मीडिया में तब्दील होकर धंधे और मुनाफे का सच टटोलने लगी। धंधा बगैर सत्ता की सुविधा के हो नहीं सकता और राजनीति बगैर मीडिया के चल नहीं सकती। इस जरूरत ने बाजारवादी धंधे में मीडिया और राजनीति को साझीदार भी बनाया और करीब भी पहुंचाया।
पत्रकार भी इटंरप्नयूर बनने लगा। जो पत्रकारिता शिखर पर पहुंचकर राजनीति का दमन थामती थी और पत्रकार संसद में नजर आते उसमें नयी समझ कारपोरेट मालिक बनने की हुई। क्योंकि राजनीति बाजार के आगे नतमस्तक तो बाजार में मीडियाकर्मी की पैठ उसे राजनीति से करीबी से कहीं ज्यादा बड़ा कद देती। किसी मीडिया संस्थान में बतौर पत्रकार काम करने से बेहतर खुद का संस्थान बनाने और धंधे में सीधे शिरकत करने वाले को ही सफल मीडियाकर्मी माना जाने लगा। लेकिन चौथे खम्भे का संकट इसके बाद से शुरू हुआ जब वोट बैंक की राजनीति में सिनेमायी समझ घुसी और विकास का खांचा भी सिनेमायी तर्ज पर बनना शुरु हुआ। मीडिया सत्ता के उसी विकास को असल भारत मानने लगी जिसका खंचा राजनीति ने सिनेमा की चकाचौंध में बनाया। मीडिया ने भी इसका दोहरा दोहन किया। धंधे और मुनाफे के लिये राजनीतिक सत्ता की विकास की लकीर को ही असल इंडिया और किसी ने नहीं मीडिया ने ही बताया।
जाहिर है नौ फीसदी खेती योग्य जमीन इसी दौर में औद्योगिक विकास के नाम पर स्वाहा की गयी। देशभर में छह फीसद जंगल खत्म किये गये। शहरों में 22 फीसदी तक की हरियाली खत्म हुई और कंक्रीट का जंगल 19 फीसद जमीन पर तेजी के साथ पनपा। उसी दौर में तीस हजार से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की और करीब छह लाख से ज्यादा लोगों का वैसा रोजगार खत्म हुआ जो उत्पादन से जुड़ा था। पैसा लगाने और पैसा बनाने के इस सट्टा बाजार अर्थव्यवस्था के खेल ही राजनीतिक सत्ता की नीति बन गयी। मीडिया के लिये यह कोई मुद्दा नहीं बना और राजनीति ने कभी उस भारत को देश के विकास से जोड़ने की नहीं सोची जो इस चकाचौंघ की वजह से कहीं ज्यादा अंधेरे में समाता जा रहा था। राजनेताओ की सभा में राजू श्रीवास्तव सरीखे चुटकुले होने लगे और न्यूज चैनलों ने भी राजू की हंसी ठिठोली में अपने धंधे को आगे बढ़ते देखा। लोकतंत्र के चौथा खम्भा होने का भ्रम टीआरपी से निकले विज्ञापन ने कुछ यूं तोडा कि खबरों की परिभाषा भी बदली गयी और राजनीतिक सत्ता ने नयी परिभाषा को यह कह कर मान्यता दी कि मीडिया चलाने के लिये पूंजी तो चाहिये ही। यानी मीडिया की विश्वसनीयता का नया आधार पूंजी और उससे बनने वाले मुनाफे के दायरे में घुस गया। सरकार ने बाजार आगे घुटने टेक कर अनकही नीतियों के आसरे मीडिया को अपनी सिनेमायी सोच में ढाला भी और निर्भर भी बना दिया। विश्वसनीय न्यूज चैनलों में सिल्वर स्क्रीन के कलाकारों के प्रोग्राम तो छोटी बात हुई। कलाकारो से एंकरिंग करा कर पत्रकारिता के नये मापदंड बनाये गये।
ऐसा भी नहीं है कि यह सब नयी पीढ़ी ने किया जिसने पत्रकारिता के संघर्ष को ना देखा-समझा हो। बल्कि प्रिंट पत्रकारिता से न्यूज चैनलों में आये वह पत्रकार ही इंटरप्यूनर की तर्ज पर उबरे और अपने सामने ध्वस्त होती राजनीति या कहें सिनेमायी राजनीति का उदाहरण रख नतमस्तक हो गये। जिस तरह सिनेमायी धंधे के लिये देश भर में महंगे सिनेमाघर बने और इन सिनेमाघरो में टिकट कटा कर सिनेमा देखने वालो की मानसिकता की तर्ज पर ही फिल्म निर्माण हो रहा है तो राजनीतिक सत्ता ने भी वैसी ही नीतियों को अपनाया, जिससे पैसे की उगाही बाजार से की जा सके। यानी मल्टीप्लैक्स ने सिनेमा के धंधे का नया कारपोरेट-करण किया तो विकास नीति ने पूंजी उगाही और कमीशन को ही अर्थव्यवस्था का मापदंड बना दिया। और मीडिया ने सिल्वक स्क्रीन की आंखो से ही देश की हालत का बखान शुरु किया। खुदकुशी करते किसानो की रिपोर्टिंग फिल्म दो बीघा जमीन से लेकर मदर इंडिया के सीन में सिमटी। 2020 के इंडिया को दुबई की सबसे ऊंची इमारत दिखाकर सपने बेचे गये। नीतियों पर निगरानी की जगह मीडिया की भागेदारी ने सरकार को यही सिखाया कि लोग यही चाहते हैं, यह ठीक उसी प्रकार है जैसे टीआरपी के लिये न्यूज चैनल सिनेमायी फूहड़ता दिखाकर कहते है कि दर्शक तो यही देखना चाहते हैं।
धंधे पर टिके सिनेमा की तर्ज पर मीडिया और उसी तर्ज पर राजनीतिक सत्ता के ढलने से तीस फिसद इंडिया में ही समूचा भारत देखने की समझ नीतिगत तौर पर उभरी। स्पेशल इकनामी जोन से लेकर टाइगर प्रोजेक्ट के घेरे में ग्रामीण समाज और आदिवासी हाशिये पर चला गया लेकिन ग्लोबल बाजार की पूंजी इन परियोजनाओ से जुड़ती चली गयी और सरकार को फायदा ही हुआ। वहीं मीडिया में विकास का आधार भी सत्ता के अनुकूल हो गया। यानी उपभोक्ता बनाकर बाजार पर निर्भर करने की मानसिकता से जुड़े तमाम खबरें हो या प्रचार विज्ञापन सबकुछ मीडिया ने आंख बंद कर छापा भी और न्यूज चैनलों में दिखाया भी। इतना ही नहीं सरकार की जिन नीतियों ने स्कूलों से खेल मैदान छिने, मोहल्लो से पार्क छिने। रंगमंच खत्म किया । खेल स्टेडियम को फीस और खेल विशेष से जोड़ दिया उसमें समाज के सामने मनोरंजन करना भी जब चुनौती बनने लगा तो सिनेमा और सिनेमायी तर्ज पर न्यूज चैनलों को उसी राजनीतिक सत्ता ने प्रोत्साहित किया, जिसका काम इन तमाम पहलो को रोकना था। पूंजी पर मीडिया को टिकाकर सत्ता की सिनेमायी सोच ने पत्रकारिता के आयामों को ही बदल दिया।
पत्रकारिता खुद ब खुद उस लघु पत्रिका का हिस्सा बन गयी जो नब्बे के दशक तक मुख्यधारा की पत्रकारिता को भी चुनौती देती थी। लेकिन उस दौर में मुख्यधारा की पत्रकारिता का मतलब कहीं ना कहीं सत्ता को चुनौती देते हुये बहुसंख्य लोगों से जुडे सवालों को उठाना होता था। और लघु पत्रकारिता विकल्प की सोच लिये विचारों का मंच बनाती थी। लेकिन नयी परिस्थितियों ने मुख्यधारा का मतलब सत्ता से करीबी और कारपोरेट पूंजी के तौर तरीकों से मीडिया को व्यवसायिक बनाकर आगे बढ़ाना है। इसमें खबर का मतलब सरकार की नीतियों का प्रचार और कारपोरेट धंधे के नये गठजोड़ होते हैं। और मनोरंजन से जुड़ी खबरें जो सिनेमायी धंधे को समाज का असल आईना बताती है। न्यूज चैनल का एंकर किसी नायक-नायिका की तर्ज पर खुद को रखता है और संपादक फिल्म प्रोड्यूसर की तर्ज पर नजर आता है। राजनेता का मापदंड भी उसके औरे से तय होता है। नेता का ग्लैमर, उसका लोगों से कटकर न्यूज चैनल के पर्दे पर लगातार बोलना ही उसकी महत्ता है। यानी एक तबके भर के लिये सिनेमा, उसी के लिये राजनीतिक सत्ता की नीतियां और उसी के मानसिक मनोरंजन के लिये मीडिया, लोकतंत्र का नया सच कुछ इसी परिभाषा में सिमट गया है। और लोकतंत्र बार-बार पारंपरिक खम्भों की दुहाई दे कर एहसास करता है कि देश में सबका हक बराबर का है। हर कोई बराबर का नागरिक है। जिसका मापदंड चुनाव है जिसमें हर कोई वोट डाल सकता है और सभी का मत बराबर का होता है। यह अलग बात है कि वोट बैंक डिगाने के लिये नेता पूरी तरह सिनेमायी नायक-नायिका पर जा टिका है और मीडिया सिलवर स्क्रीन का आईना बन गया है।
कह सकते है पहले समाज का आईना फिल्म होती थी अब फिल्म का आईना समाज माना जाने लगा है। इसलिये सवाल माई नेम इज खान का नहीं है, सवाल यह भी नहीं है कि है मनमोहन सिंह भी कहें, “माई नेम इज मनमोहन और मै पीएम नहीं हूं।” क्योंकि मै सीईओ हूं। लेकिन मीडिया से कौन निकल कर कहेगा कि माई नेम इज गणेश शंकर विद्यार्थी और मै पत्रकार नहीं हूं।
मशहूर टीवी जर्नलिस्ट पुण्य प्रसून बाजपेयी के ब्लाग पर 21 फरवरी 2010 को प्रकाशित













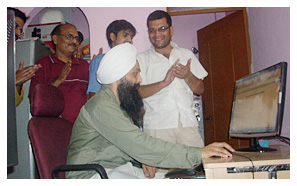
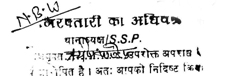
harendra thakur
March 6, 2010 at 10:21 am
prasun sir aksar aap jab kadwi baatein likhte hai to kuchh logon ko chubh hi jata hai.
कुमार विनोद
March 6, 2010 at 9:11 am
राम जी, पता नहीं आप किस युग के राम हैं, आप तो हिंदी की पूंछ पकड़ कर बैठ गए, यहां बात भाषा की कम सोच की ज्यादा है. प्रसून जी ने जो लिखा है, टुकड़ों टुकड़ों में बयां हुए उस सच के किसे इंकार हो सकता है, खासकर उसे जो मीडिया में ही काम करता है, लेकिन मसला यहां उलझाव का है…भाषा तो सिखा दीजिएगा, सिखाने के लिए विचारों में वो लय कहां से लाइएगा?
राकेश उपाध्याय
March 6, 2010 at 6:03 am
प्रसूनजी का आलेख आज की संसदीय राजनीति का बेहतरीन विश्लेषण है। बाजारवाद ने किस कदर हमें अपनी गिरफ्त में लिया है, उसकी एक बानगी हम यहां देख सकते हैं। सचमुच, क्या हम अपने मन से कुछ भी सोच पाने को स्वतंत्र हैं, तो उत्तर है नहीं। आज बाजार हमारी सोच और जीवन के सारे क्रियाकलापों का निर्धारण कर रहा है। मीडिया कोई अपवाद नहीं है।
बाजार का रास्ता प्रगति का रास्ता है। यह आज की सार्वजनिक मान्यता है, और इसके विपरीत यदि कोई सच है तो फिलहाल उसकी जगह किताबें और पुस्तकालय ही हैं और वे भी इसी बाज़ार की माया से प्रभावित हैं। कहना लाजिमी होगा कि बाजार है इसलिए किताबें धड़ाधड़ प्रकाशित हो रही हैं, चैनल चल रहे हैं, अखबार बिक रहे हैं।
इसलिए बाजार जिस प्रकार से आज हमारी प्रेरणा का केंद्र बन चुका है, पहले कभी नहीं था। रिश्ते भी अब बाजार के आधार पर बन और बिगड़ रहे हैं। इस कलिकाल में मनुष्य की प्रेरणा उसका धर्म और ईमान नहीं है, उसके कर्म और कार्मिक गुण नहीं हैं, मन और मानसिकता नहीं हैं, मूल प्रेरणा आज बाजार है, मार्केट है। वही गुण हमें प्रेय है जो मार्केट को भाए, वही चीज या प्रोडक्ट हम प्रस्तुत करेंगे या कहिए पेशे खिदमत करेंगे जो मार्केट में छाए।
इसलिए तो राहुल महाजन आज मस्त खड़ा है। बीते जमाने में ऐसे चरित्र के इंसानों को हमने गली-गुच्चे में धूल-धक्कड़ खाते देखा है, नशे में मदमस्त….। मीडिया का क्या चरित्र है…जिस ड्रग एडिक्ट को प्रमोद महाजन के मरने के तुरंत बाद खलनायक बना दिया था…आज उसके लिए पलक पांवडे बिछा दिए हैं। कोई है जो अब उसके पुराने प्रोफाइल पर डिस्कस करे। नहीं कर सकता क्योंकि वह बाजार का खड़ा माल है और हर कोई उस माल की कीमत जानता है। उसकी बाइट कीमती है, उसे नाराज़ कर कौन चैनल कल उसके इन्टरव्यू से हाथ धोना चाहेगा।
तो राहुल ब्रांड के जमाने के हम भी हैं। संसदीय राजनीति इससे इतर कहां है। हो भी नहीं सकती। 100 साल पहले इसे वैश्या बताने का काम गांधी ने यूं ही नहीं किया था। इस राजनीति में लूटेरों को गिरोह हिंदुस्तान में विविध रूपों में काबिज हो कर बैठ गया है। ये दे दनादन माल काट रहा है, खुले हाथ दौलत बटोर रहा है। इसके बिस्तर के नीचे दौलत है, इसके कार्यालय में दौलत है। ये भोग के चरम पर है, और तब चरम पर है जब हिंदुस्तान का औसत आदमी दो जून की रोटी के लिए तड़प रहा है। ये वर्ग उसकी तड़प को शांत करने के लिए नरेगा और मनरेगा का नारा उछाल रहे हैं। हिंदुस्तान का जो वर्ग कभी असल मालिक था, पिछले तीन सौ साल की औपनिवेशिक लूट के कारण सीधे तौर पर बेबस और लाचारी की हालत में जा पहुंचा है।
वह आज भूखा मजदूर है, आत्महत्या करने वाला किसान है। और यही असल हिंदुस्तान है जिस तक पहुंचने और पहुंचाने का वायदा भी आज एक बड़े राजनीतिक और विज्ञापनीय कारोबार में बदल चुका है लेकिन तस्वीर जस की तस है।
सवाल है कि कौन बदल करेगा। माओ ने कहा था कि सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है सो कुछ परिवर्तनकारियों ने बंदूकें हाथ में थाम लीं हैं। लेकिन वे भी आज एक अंतरराष्ट्रीय कारोबार के मकड़जाल में नहीं फंस चुके हैं इस बात की गारंटी कौन दे सकता है। आज बदल की वकालत करने वाले ही बदल जा रहे हैं।
इसलिए रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरत जो पूरी करे वही विचार, वही औजार हिंदुस्तान को चाहिए। आर्थिक उदारीकरण की आंधी का जो सबब है, वह तो कम से कम हमारी रंक और दरिद्र गति का खात्मा नहीं कर सकेगा। हां, इसके चक्कर में स्वाहा बहुत कुछ हो जाएगा।
यह वक्त है कि चिंतन करने वाले सतह की बजाए गहराई में चिंतन करें। इफरात अन्न, दूध, सब्जी, दाल और चावल, रहने को सुंदर छत भले ही खपरैल की हो, पीने को साफ पानी, लेने को प्रदूषण मुक्त हवा और हरियाली, खुला आसमान और तपने-तपाने वाला सूर्य यही संपूर्ण दुनिया के लिए अपरिहार्य तत्व हैं। यह देने का और इसे बचाए और बनाए रखने का जो विचार और व्यवहार हो, वह देने वाला नेतृत्व समूह चाहिए हिंदुस्तान को, जहां किसी को रोटी-पानी-रोजगार के लिए परप्रांतीय और गैरजनपदीय न बनना पड़े। जब तक और जिससे यह ना हो सके तो कैसे नेता, कैसी मीडिया, क्या पत्रकार और क्या पत्रकारिता। सब बकवास…. प्रसून जी से मैं सौ फीसदी सहमत हूं।
devesh charan
March 6, 2010 at 5:42 am
hello
Prasun ji
Namsate
first i introduce myself that i am same devesh who has interviewed for DASH.
now ur article– it is very difficult to comment on ur article because i beleive u have lived journalism. Unfortunately u have to see this phase also. Bt it is nt about journalism. what it is and what it ought to be? what are the parameters to define who is ganesh shankar vidyarthi and who is nt journalsit bt he is an activist
today we are living in an era where the who environment is in degenration. look at anything around u -i feel there is a constant degenration at an incresing rate. whether it is climate institution relationship or indvidual human being. So journalists come from same environment. so i do not think it is irony . i agree we are now body without soul. Bt atleast we have to accept that WE ARE NOT JOURNALIST BT A PAID WORKER WHO WORKS WITH PEN WORKING ON IDEA OF CAPITALIST–ceo OR SO CALLED EDITORS.
bt i have firm belief that people have recognised that this is a problem and problem identified is half solution .
राकेश उपाध्याय
March 6, 2010 at 6:02 am
प्रसूनजी का आलेख आज की संसदीय राजनीति का बेहतरीन विश्लेषण है। बाजारवाद ने किस कदर हमें अपनी गिरफ्त में लिया है, उसकी एक बानगी हम यहां देख सकते हैं। सचमुच, क्या हम अपने मन से कुछ भी सोच पाने को स्वतंत्र हैं, तो उत्तर है नहीं। आज बाजार हमारी सोच और जीवन के सारे क्रियाकलापों का निर्धारण कर रहा है। मीडिया कोई अपवाद नहीं है।
बाजार का रास्ता प्रगति का रास्ता है। यह आज की सार्वजनिक मान्यता है, और इसके विपरीत यदि कोई सच है तो फिलहाल उसकी जगह किताबें और पुस्तकालय ही हैं और वे भी इसी बाज़ार की माया से प्रभावित हैं। कहना लाजिमी होगा कि बाजार है इसलिए किताबें धड़ाधड़ प्रकाशित हो रही हैं, चैनल चल रहे हैं, अखबार बिक रहे हैं।
इसलिए बाजार जिस प्रकार से आज हमारी प्रेरणा का केंद्र बन चुका है, पहले कभी नहीं था। रिश्ते भी अब बाजार के आधार पर बन और बिगड़ रहे हैं। इस कलिकाल में मनुष्य की प्रेरणा उसका धर्म और ईमान नहीं है, उसके कर्म और कार्मिक गुण नहीं हैं, मन और मानसिकता नहीं हैं, मूल प्रेरणा आज बाजार है, मार्केट है। वही गुण हमें प्रेय है जो मार्केट को भाए, वही चीज या प्रोडक्ट हम प्रस्तुत करेंगे या कहिए पेशे खिदमत करेंगे जो मार्केट में छाए।
इसलिए तो राहुल महाजन आज मस्त खड़ा है। बीते जमाने में ऐसे चरित्र के इंसानों को हमने गली-गुच्चे में धूल-धक्कड़ खाते देखा है, नशे में मदमस्त….। मीडिया का क्या चरित्र है…जिस ड्रग एडिक्ट को प्रमोद महाजन के मरने के तुरंत बाद खलनायक बना दिया था…आज उसके लिए पलक पांवडे बिछा दिए हैं। कोई है जो अब उसके पुराने प्रोफाइल पर डिस्कस करे। नहीं कर सकता क्योंकि वह बाजार का खड़ा माल है और हर कोई उस माल की कीमत जानता है। उसकी बाइट कीमती है, उसे नाराज़ कर कौन चैनल कल उसके इन्टरव्यू से हाथ धोना चाहेगा।
तो राहुल ब्रांड के जमाने के हम भी हैं। संसदीय राजनीति इससे इतर कहां है। हो भी नहीं सकती। 100 साल पहले इसे वैश्या बताने का काम गांधी ने यूं ही नहीं किया था। इस राजनीति में लूटेरों को गिरोह हिंदुस्तान में विविध रूपों में काबिज हो कर बैठ गया है। ये दे दनादन माल काट रहा है, खुले हाथ दौलत बटोर रहा है। इसके बिस्तर के नीचे दौलत है, इसके कार्यालय में दौलत है। ये भोग के चरम पर है, और तब चरम पर है जब हिंदुस्तान का औसत आदमी दो जून की रोटी के लिए तड़प रहा है। ये वर्ग उसकी तड़प को शांत करने के लिए नरेगा और मनरेगा का नारा उछाल रहे हैं। हिंदुस्तान का जो वर्ग कभी असल मालिक था, पिछले तीन सौ साल की औपनिवेशिक लूट के कारण सीधे तौर पर बेबस और लाचारी की हालत में जा पहुंचा है।
वह आज भूखा मजदूर है, आत्महत्या करने वाला किसान है। और यही असल हिंदुस्तान है जिस तक पहुंचने और पहुंचाने का वायदा भी आज एक बड़े राजनीतिक और विज्ञापनीय कारोबार में बदल चुका है लेकिन तस्वीर जस की तस है।
सवाल है कि कौन बदल करेगा। माओ ने कहा था कि सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है सो कुछ परिवर्तनकारियों ने बंदूकें हाथ में थाम लीं हैं। लेकिन वे भी आज एक अंतरराष्ट्रीय कारोबार के मकड़जाल में नहीं फंस चुके हैं इस बात की गारंटी कौन दे सकता है। आज बदल की वकालत करने वाले ही बदल जा रहे हैं।
इसलिए रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरत जो पूरी करे वही विचार, वही औजार हिंदुस्तान को चाहिए। आर्थिक उदारीकरण की आंधी का जो सबब है, वह तो कम से कम हमारी रंक और दरिद्र गति का खात्मा नहीं कर सकेगा। हां, इसके चक्कर में स्वाहा बहुत कुछ हो जाएगा।
यह वक्त है कि चिंतन करने वाले सतह की बजाए गहराई में चिंतन करें। इफरात अन्न, दूध, सब्जी, दाल और चावल, रहने को सुंदर छत भले ही खपरैल की हो, पीने को साफ पानी, लेने को प्रदूषण मुक्त हवा और हरियाली, खुला आसमान और तपने-तपाने वाला सूर्य यही संपूर्ण दुनिया के लिए अपरिहार्य तत्व हैं। यह देने का और इसे बचाए और बनाए रखने का जो विचार और व्यवहार हो, वह देने वाला नेतृत्व समूह चाहिए हिंदुस्तान को, जहां किसी को रोटी-पानी-रोजगार के लिए परप्रांतीय और गैरजनपदीय न बनना पड़े। जब तक और जिससे यह ना हो सके तो कैसे नेता, कैसी मीडिया, क्या पत्रकार और क्या पत्रकारिता। सब बकवास….
Ram
March 6, 2010 at 2:51 am
Prasoon Ji,
pandit dukharan, kumar vinod aur kamta prasad jaiso commentkaron ko pahle hindi sikhaiye.
Pata nahi kis praydeep ke jeev hai.
Gaurav bevaak,jaipur.
March 6, 2010 at 2:21 am
prasun ji salaam,aapaki soch,aapake lekhan ko salaam karata hu,main aapaka badi khabar dekhata hu phir apane aapako improve karata hu,aapake article jansatta main bhi padata hu,prabhash joshi ji,aapako ,vedpratap vaidik,rahul barpute ji,vinod dua ji,rajdip sardesai ,rambahadur roy,p.kamal dixit ji ko apana adarsh manata hu,main jald hi patrakarita ke manch par aa raha hu,mere se pehle jo aapake bare mein jo negative comments likhein hai unaki ye bachkani harkat hai,inako maaf kar dena inako abhi time lagega patrakarita samajhane mein,
Manish
March 5, 2010 at 11:44 pm
Prassun Ji,
Es tarah Ka report Ek documentary film he Pasand kerte hail log …or yeh Nyay sangat nahi hai.Aisa Pure Desh Me ho raha hai sayd ap jante honge ..Basically I already belong to media and i know very well what is reality ..so let’s see …manish from Patna
पंडित दुखहरण दास
March 5, 2010 at 9:31 pm
माननीय प्रसून जी….
कभी-कभी आप भी ढेंसरा जाते हैं। 1988-89 में पहली बार बॉलीवु़ड ने अगर राजनीति में दस्तक दी तो 1984 को क्या कहेंगे, जब परम श्रद्धेय अमिताभ बच्चन, श्रीमती बैजयंती माला बाली और स्वर्गीय सुनील दत्त जी को क्या कहेंगे। इसी इलेक्शन में इन महानुभावों ने क्रमश: इलाहाबाद, मद्रास और मुंबई से चुनाव जीत कर लोकसभा की हरी कालीन पर पांव रखा था।
rupesh gupta
March 5, 2010 at 12:43 pm
सच यही है
कुमार विनोद
March 5, 2010 at 12:17 pm
ब्लॉग पर एंकरिंग…सर आप ‘आज तक’ की पीढ़ी के पत्रकार हैं, आप तो ‘सीधी बात’ कीजिए…ऐसी सीधी और सरल बात, जो बौद्धिकता के उलझे ताने बाने में न बुनी हो, हिंदी के समान्य अक्षर ज्ञान वाले आम आदमी को लाइन बाइ लाइन समझ आए.
kamta prasad
March 5, 2010 at 9:29 am
बड़े मियां आदाब। ई आपकी समझ को क्या होता जा रहा है अजी कम से कम ब्लाग पर सही तरह से बात रखा करें। प्रसून जी किसको और काहे को उल्लूo बना रहे हैं। दिल पर हाथ रखकर बताइये प्रेस लोकतंत्र का चौथा खंभा है या राज्य का और राज्यउ का चरित्र क्याै है।
क्या यह जनता का राज्यउ है या धनिकों का। लगता है पहले की सारी पढ़ाई-लिखाई शक्कर में घोलकर पी गये। अल्लाह-ताला भला करे आपका।