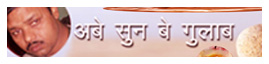 अखबारों के दफ्तर में दो तरह के लोग जरूर आते हैं। पहला वाला बेखटके घुस जाता है, दूसरा वाला सिकूरिटी में फंस जाता है। पहला इस अंदाज में एकाग्र प्रकट होता है जैसे चील चूहा तलाशती है। चूहा तलाश लेने के बाद वह सेवा का प्रस्ताव करते हुए खबरनुमा चीज सरकाता है। ढीठ हुआ तो पूछ भी लेता है कितना लगेगा? (हालांकि यह पेड न्यूज के दौर में निहायत पिछड़ी बात है, कितना दोगे, अब यह पूछने का दायित्व संपादक जैसे किसी सीनियर का हो गया है।)
अखबारों के दफ्तर में दो तरह के लोग जरूर आते हैं। पहला वाला बेखटके घुस जाता है, दूसरा वाला सिकूरिटी में फंस जाता है। पहला इस अंदाज में एकाग्र प्रकट होता है जैसे चील चूहा तलाशती है। चूहा तलाश लेने के बाद वह सेवा का प्रस्ताव करते हुए खबरनुमा चीज सरकाता है। ढीठ हुआ तो पूछ भी लेता है कितना लगेगा? (हालांकि यह पेड न्यूज के दौर में निहायत पिछड़ी बात है, कितना दोगे, अब यह पूछने का दायित्व संपादक जैसे किसी सीनियर का हो गया है।)
दूसरे किस्म का आदमी फटेहाल होता है। उसकी आंखों में बुखार का आभास देती खफीफी चमक होती है। उसके हाथ में भी कोई कागज ही होता है। उलझी-पुलझी लिखावट और चित्रों में उसके एकालाप, दुःस्वप्न, कुंठाएं, अधूरी इच्छाएं, आशाएं छिपी होती हैं। इस कागज के जरिए वह ईश्वर, प्रकृति, सरकार, राष्ट्र आदि से फरियाद करता है और उन्हें आदेश भी दे डालता है। ऐसे अबूझ लोगों को पागल कह कर भगा दिया जाता है और उनके कागज की चिंदियां कई दिनों तक पत्रकारों को चकित और मनोरंजित करती रहती हैं। अपनी समझदारी के फ्रेम के बाहर के आदमी को पागल कह कर पल्ला झाड़ लेना समझदारी का सबूत है।
पहले आदमी को पता होता है कि पत्रकारिता ऐसी एजेंसी में बदल चुकी है जो मुद्रा लेकर आपका मैसेज (आत्मप्रचार, चरित्रहनन, परनिन्दा, भंडाफोड़ादि) अपनी पीठ पर विज्ञापन की तरह चिपका कर घर-घर घूमती है। वह अपने सर्किल में जीट उड़ाता है, अरे, पत्रकारों का क्या है। उनकी कीमत एक पौवा दारू और एक मुर्गे की टांग है। किसी रिपोर्टर की गाड़ी की टंकी फुल करा दो, जो चाहे लिखवा लो। इस आदमी के लिए घूस वेतन का विस्तार है और नैतिकता मरी हुई चिड़िया जिसमें भुस भर कर आवश्यकतानुसार कहीं भी सजाया जा सकता है। ऐसा कोई मूल्य नहीं है जिसका कोई मूल्य न हो। यहां बड़े खिलाड़ियों की बात नहीं हो रही है जिनके प्रलोभन के तरीके बेहद महीन हैं और भ्रष्टाचार के औचित्य का नैतिकशास्त्र रचने का काम वे पूरा कर चुके हैं।
मक्खन में चाकू की तरह चलते इस लेन-देन के काऱण पत्रकारिता ही नहीं, उन सारे पेशों क ी विश्वसनीयता में भुस भर चुका है जिनका कभी एक आभामंडल हुआ करता था। वकील, डाक्टर, अध्यापक, कलाकार, नेता, धर्माचार्य, साहित्यकार, राजनेता… सभी की साख पुरानी दीवार के जर्जर पलस्तर की तरह रफ्ता-रफ्ता झर रही है। …यह पहला आदमी उस विशाल पूंजी के तंत्र का अदना सा पुर्जा है।
पत्रकार नाम के प्राणी की साख स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पीड़ित की आह को स्वर देते हुए बनी थी। उस दौर का पत्रकार आई.कार्ड रखने तक को बेइज्जती मानता था, वह आम आदमी जितना ही अनारक्षित होने में गौरव महसूस करता था। इसलिए उसने खुद को लोकतंत्र का चौकीदार, कटखना कुत्ता जैसे रुमानी विशेषण दिए। उसी परंपरा का दबाव है कि पत्रकारिता में अपनों की खाल उधेड़ने या आत्मालोचना की प्रवृत्ति जरा ज्यादा ही है। जी हां, अब भी।
उस परंपरा के बुलावे पर ही आंखों में बुखार की चमक वाला नीमपागल अपना अगड़म-बगड़म कागज छपवाने के लिए सबसे पहले अखबार की तरफ लपकता है। ये पागल अपने समुदाय के सबसे दुस्साहसी लोग होते हैं जो यहां तक पहुंच आते हैं वरना ऐसे लोगों की तादात करोड़ों में है जिन्हें किसी से सुनवाई की कोई उम्मीद युगों से नहीं है। इस देश में वे मानों अवैध घुसपैठियों की तरह रहते हुए लोकतंत्र का सर्कस देखते रहते हैं। बाजार के नजरिए से भी देखें तो उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि उनकी अवहेलना करना मुमकिन नहीं लेकिन उनकी बात समझने की पहली शर्त पक्षधरता और विश्वसनीयता है। अगर उत्कोचिया प्रलोभनों को दरकिनार कर मीडिया जल्दी ही अपने बुनियादी चरित्र के मुताबिक उनके साथ खुद को नहीं जोड़ता तो वे एक दिन अपना कोई नया मीडिया बना लेंगे।
हमें याद रखना चाहिए कि हमारे देश में पहले अखबार का जन्म ही न्याय की आकांक्षा और सत्य के प्रति आग्रह से हुआ था। अब भी हमारे समाज में ये दोनों चीजें इतनी विशाल तादाद में बिखरी हुई हैं कि सारी दुनिया की दौलत देकर भी उन्हें कभी खरीदा नहीं जा सकेगा।
….तो ऐसे पत्रकारों की बेहद जरूरत है जो पागलों के अगड़म-बगड़म कागज पढ़ सकें।
-अनिल यादव













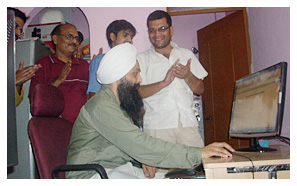
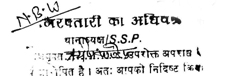
kamta
May 1, 2010 at 6:33 am
अनारक्षित की जगह अरक्षित वलनरेबल शब्द ज्यादा ठीक लगता है, अशोक पांडेय अरक्षेय को ठीक मानते हैं। आलेख के एक हिस्से में कमूनिस्ट के एक पैरे को प्रकारांतर से उद्धृत किया गया है। चित्र उपस्थितिकरण दुरुस्त है पर समाधान वह सुबह कभी तो आएगी टाइप है।
kamta
May 1, 2010 at 7:05 am
प्रथमार्द्ध का जो शब्दचित्र प्रस्तुत किया गया है उसके लिए वाह पर उत्तरार्द्ध में जो रूमानियत प्रदर्शित होती है उस पर ठहरकर बात करने की जरूरत है। बीड़े पीने वाले जनकवि मुक्तिबुद्ध ने अपनी रचनाओं में एकालाप, दुःस्वप्न, अधूरी इच्छाओं आशाओं के साथ-साथ अवाम के मुख्तलिफ हिस्सों की कुंठा का भी तफसील से जिक्र किया है। यह सब तो ठीक है लेकिन जनता की स्वत:स्फूर्ति का जो महिमामंडन झलकता है वह नेतृत्कारी शक्तियों की जरूरत को दरकिनार कर देता है। खांटी भावनावादी पहुंच-पद्धति। अतीत में तमाम काबिल लेखकों कवियों का इस तरह के जनप्रेम ने सत्यानाश किया है। तर्क-विचार के एसिड में डुबोकर इस तरह के बचकाने जनप्रेम को खत्म कर दिया जाना चाहिए।
श्रमजीवी लोग जब सचेतन तौर पर अपना वर्ग-रूपांतरण करेंगे बात तभी बनेगी।
उम्मीद है मेरी बात से मॉडरेटर महोदय इत्तेफाक रखते होंगे।
Ved Ratna Shukla
May 1, 2010 at 1:01 pm
Bahut Khoob.
Rahul Chouksey
May 1, 2010 at 1:14 pm
Anil ji aapke lekh mein ek tadap si mehsus pratit hoti hai…….Aaj patrakarita jis daur se gujar rahi hai ……jo pesha kaha jaane lagaa hai wo samaaj ko aaina dikha hakikat se rubarooo karwata tha…..par us aaine par lagi dhool hatana tedhi kheer lag rahi hai….kintu abhi ek kranti aur aayegi jab paisaa raaj karega angrezo ki tarah aur fir GANESH SHANKAR VIDHYARTHI paida honge, fir LOKMANYA ki kalam dahadegi….fir MAKHANLAL aur DHARAMVEER BHARTI likhenge ….DESH NIRMAAN K LIYE na ki T.G.(target group) k liye…..
Animesh
May 1, 2010 at 5:53 pm
Jab koi patrakar/sampadak vyavastha se ladhte hue likhta hai, to janata uske lekh ko dhoond dhoond kar padhti hai, chahe M K Gandhi Young India/Navjivan me likhen, ya Tilak Kesari me likhen. Angrezi akhbar us zamaane me bhi the par wey Angrezon ke talchatuwe they. Woh dour azaadi ka tha, janata ko azaadi chahiye thi, sarkar jab akhbaron ko ban aur printing press ko seal karti thi to janata chhup chhup kar bhi aise mahan patrakaron/sampadakon ko padhti thi. Azaadi se theek pahle dhanna sethon ne dekha ki akhbar chhapna fayde ka souda hoga, aur hua bhi wahi. Ab akhbar sirf khabaren dene lage, chaaploosi ka daur shuru hua, sampadak, kavi Rajya Sabhasad ban gaye, reporters packets dhoondhne me lag gaye aur jo hona tha wahi hua. Ab marketing ka zamaana hai, maalik hi khud khabron ki marketing kar raha hai, lekin yeh public hai jo sab jaanti hai. Insaaf ke liye ladhne wale ka woh saath to degi, lekin use maaloom hai ki ladhai kaafi lambi hai.
atulgaur
May 2, 2010 at 6:14 am
bahoot accha
Abhishek sharma
May 2, 2010 at 3:35 pm
bhai mere premchand ke gulab ki khushbu aap le rahe hai?
banarasi pandit
May 6, 2010 at 10:29 am
bahut khuub bete
rajesh patel
May 8, 2010 at 2:58 am
anil tumne aaina dikha diya hai aaj ke sampadako aur patrakaro ko.