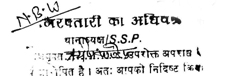![]() : क्या आपने लोहिया का पढ़ा है? : अगर पूछा जाए कि किस एक बुद्धिजीवी को मैं सबसे ज्यादा मिस करता हूं तो दिमाग में सबसे पहला नाम अरविंद नारायण दास का आएगा। 1990 में वे टाइम्स ऑफ इंडिया के असिस्टेंट एडिटर और एडिट पेज के इंचार्ज हुआ करते थे, लेकिन पंद्रह एक साल पहले हमारी पार्टी में गया जिले के सेक्रेटरी भी रह चुके थे। समाज, संस्कृति, विचारधारा और राजनीति में उनकी सहज गति थी। दृष्टि की व्यापकता के अलावा उनके यहां ऊंचाई और गहराई भी थी, जो भारतीय बौद्धिकता में प्रायः एक साथ नहीं मिलती।
: क्या आपने लोहिया का पढ़ा है? : अगर पूछा जाए कि किस एक बुद्धिजीवी को मैं सबसे ज्यादा मिस करता हूं तो दिमाग में सबसे पहला नाम अरविंद नारायण दास का आएगा। 1990 में वे टाइम्स ऑफ इंडिया के असिस्टेंट एडिटर और एडिट पेज के इंचार्ज हुआ करते थे, लेकिन पंद्रह एक साल पहले हमारी पार्टी में गया जिले के सेक्रेटरी भी रह चुके थे। समाज, संस्कृति, विचारधारा और राजनीति में उनकी सहज गति थी। दृष्टि की व्यापकता के अलावा उनके यहां ऊंचाई और गहराई भी थी, जो भारतीय बौद्धिकता में प्रायः एक साथ नहीं मिलती।
अपने इर्द-गिर्द की चीजों के बारे में वे नई बातें कहते थे, लेकिन इस तरह कि सुनने-पढ़ने वाले लगता था, यह सब मैंने पहले ही सोच रखा है। हम जैसे नए लोगों की बातें भी ऐसे सुनते थे जैसे इनमें हर  बार कुछ नया मिल जाने की उम्मीद कर रहे हों। 1990 के उस जटिल दौर को समझने में अरविंद एन. दास से बड़ी मदद मिलती थी। देवीलाल प्रकरण में एक बार मैंने उत्तेजना में उन्हें रात बारह बजे फोन कर दिया। फोन उनकी बेटी ने उठाया और कहा- यह क्या कोई समय है किसी शरीफ आदमी के घर फोन करने का। अगले दिन मैंने माफी मांगी तो उन्होंने जवाबी माफी मांगने के से स्वर में कहा कि उसने नींद में फोन उठाया होगा, और आपको वह जानती भी तो नहीं।
बार कुछ नया मिल जाने की उम्मीद कर रहे हों। 1990 के उस जटिल दौर को समझने में अरविंद एन. दास से बड़ी मदद मिलती थी। देवीलाल प्रकरण में एक बार मैंने उत्तेजना में उन्हें रात बारह बजे फोन कर दिया। फोन उनकी बेटी ने उठाया और कहा- यह क्या कोई समय है किसी शरीफ आदमी के घर फोन करने का। अगले दिन मैंने माफी मांगी तो उन्होंने जवाबी माफी मांगने के से स्वर में कहा कि उसने नींद में फोन उठाया होगा, और आपको वह जानती भी तो नहीं।
भारतीय मीडिया जगत और उसके वैचारिक नेता टाइम्स ऑफ इंडिया में आ रहे एक बुनियादी बदलाव में अरविंद एन. दास की जगह एक मायने में वाटरमार्क जैसी थी। अगले दो वर्षों में हमारा मीडिया देखते-देखते दोटकिया हिंदूवाद और देहदर्शनी उथलेपन से भर गया। बीच-बीच में मैं अरविंद जी से मिलने टाइम्स हाउस आता था तो वहां जिम्मेदार अंग्रेजी पत्रकारों के बीच होने वाली चर्चा भी सुनने को मिलती थी। उनकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि टाइम्स ऑफ इंडिया भी अब हिंदुस्तान टाइम्स बनने की राह पर बढ़ रहा है। अगले ही साल अरविंद नारायण दास और दिलीप पडगांवकर ने टाइम्स ऑफ इंडिया छोड़ दिया और आपसी सहयोग से एक टीवी प्रोग्राम फर्स्ट एडिशन और फिर समीक्षाओं पर आधारित एक टेब्लॉयड मैगजीन बिब्लियो निकालने की राह पर बढ़ चले। अरविंद जी की कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई। पचास के लपेटे में कुशल और ईमानदार बौद्धिकों की मौत की काफी लंबी सूची में इस तरह मेरे लिए वह पहले नाम बने। टाइम्स ग्रुप के वरिष्ठ हिंदी पत्रकारों में मेरा हल्का-फुल्का संपर्क राजकिशोर से था। राजेंद्र माथुर का नाम पटना से ही सुनता आ रहा था, लेकिन मिलने का मौका कभी नहीं मिला। 1991 में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु का एक राजनीतिक आयाम भी था, जिस पर अभी बात नहीं हो सकती।
अक्टूबर-नवंबर 1990 के ही किसी दिन मैं रघुवीर सहाय से मिलने उनके घर गया। मेरे प्रधान संपादक महेश्वर ने उनसे कॉलम लिखवाने के लिए कहा था। रघुवीर सहाय से मेरी मुलाकात बहुत अच्छी नहीं रही। उनके बारे में मेरी राय एक आत्मलीन खड़ूस बूढ़े जैसी ही बनी। इसके महीने भर के अंदर ही उनके मरने की खबर आई और उनसे हुई कुल दो मुलाकातों में दूसरी केवल उनकी निर्जीव देह से ही हो सकी। बहरहाल, मेरी समझ इतनी मैच्योर होने में पूरे दस साल लगे कि मैं रघुबीर सहाय के बारे में अपनी राय बदल सकूं और घंटे भर की उस एकमात्र बातचीत में उनकी कही बातों का कोई कायदे का मतलब निकाल सकूं। हुआ यह कि साउथ दिल्ली की एक बिल्कुल ताजातरीन हाउसिंग सोसाइटी प्रेस एन्क्लेव में उनके खाली-खाली से फ्लैट में पहुंचकर उन्हें मैंने अपना परिचय एक पोलिटिकल होलटाइमर के रूप में दिया तो पहला सवाल उन्होंने मुझसे यही किया कि क्या मैंने लोहिया को पढ़ा है। मैंने कहा- बस, थोड़ा सा। रघुवीर सहाय इतने पर ही भड़क गए। आप खुद को होलटाइमर कहते हैं, देश बदलना चाहते हैं, लेकिन लोहिया को नहीं पढ़ा है…..
फिर मैंने उनसे मिलने के मकसद के बारे में बताया- क्या आप जनमत के लिए आठ-नौ सौ शब्दों का एक साप्ताहिक कॉलम लिख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनमत और आईपीएफ का नाम तो उन्होंने सुन रखा है और कॉलम लिखना भी पसंद करेंगे, लेकिन इसके लिए पैसे कितने मिलेंगे। उस समय तक जनमत में लिखने के लिए किसी को पैसे तो नहीं ही दिए गए थे, इस बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। कम से कम मेरे लिए तो यह बात कहीं राडार पर भी नहीं थी। उनकी मांग से मैं खुद को सकते की सी हालत में महसूस करने लगा और बात जारी रखने के लिए उनसे पूछ बैठा कि कॉलम के लिए वे कितने धन की अपेक्षा रखते हैं। रघुवीर सहाय जैसा संवेदनशील और कुशाग्र व्यक्ति मेरे शब्दों में मौजूद अनमनेपन को ताड़े बिना नहीं रह सकता था। उन्होंने कहा, आप अपने एडिटर या मालिक, जो भी हों, उनसे बात करके बताइएगा। साथ में यह भी पूछा कि आप लोगों को भी तो काम के लिए कुछ मिलता होगा, फिर मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए। मैंने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता, न मैंने कभी इस बारे में सोचा। उन्होंने कहा, लेकिन कहीं रहते तो होंगे, खाते तो होंगे, इधर-उधर आते-जाते तो होंगे। मैंने कहा, पार्टी ऑफिस में रहता हूं, वहीं बनाता-खाता हूं, हर महीने आने-जाने और चाय-पानी के लिए सौ रुपये मिलते हैं। कभी कम पड़ जाते हैं तो पहले भी मांग लेता हूं, बचे रह जाते हैं तो कह देता हूं कि अभी काम चल रहा है, बाद में ले लूंगा।
रघुवीर सहाय उस वक्त फ्लैट में तनहा अकेले थे। दूरदर्शन में काम करने वाली एक बेटी उनके साथ रहती थीं लेकिन वे उस वक्त ड्यूटी पर थीं। तीन-चार साल पहले उन्हें टाइम्स ग्रुप से बाहर आना पड़ा था। कवि वे तब भी थे, लेकिन हिंदी के साथ जुड़ा अफसर कवि का टैग उनसे हट चुका था। बाद में दूरदर्शन, रेडियो या अखबार में अपनी हैसियत के बल पर काव्य जगत पर छाए कुछ और कवियों से मेरी मुलाकात हुई और इन पदों से हटने के बाद उनके आभामंडल का उतरना भी देखा। कौन जाने ऐसा ही कुछ पिछले कुछ सालों से रघुवीर सहाय के साथ भी हो रहा हो, जिसने उन्हें जरूरत से ज्यादा चिड़चिड़ा और आग्रही बना दिया हो। किसी कवि से उसकी कविताओं को जाने बगैर मिलने से बड़ी कृतघ्नता और कोई हो नहीं सकती। काव्य व्यक्तित्व के प्रति अगले का अज्ञान कोई मायने ही  न रखे, इसके लिए कवि का त्रिलोचन जैसा कद्दावर होना जरूरी है, जो शायद रघुवीर सहाय नहीं थे। लेकिन उनके पास खरेपन की शक्ति थी और भव्यता का कवच-कुंडल छोड़ कर किसी से भी मिल पाने की अद्भुत क्षमता थी। उनसे मिलने के बमुश्किल छह साल बाद मुझे भी पैसे-पैसे के बारे में सोचना पड़ा और लिखवा कर पैसे न देने वालों के लिए जुबान से कटु वचन न सही, लेकिन दिल से बद्दुआएं जरूर निकलीं। लोगों के बारे में झट से राय बना लेने की दुष्प्रवृत्ति न होती तो शायद रघुवीर सहाय से मिलने के एक-दो मौके मुझे और मिले होते।
न रखे, इसके लिए कवि का त्रिलोचन जैसा कद्दावर होना जरूरी है, जो शायद रघुवीर सहाय नहीं थे। लेकिन उनके पास खरेपन की शक्ति थी और भव्यता का कवच-कुंडल छोड़ कर किसी से भी मिल पाने की अद्भुत क्षमता थी। उनसे मिलने के बमुश्किल छह साल बाद मुझे भी पैसे-पैसे के बारे में सोचना पड़ा और लिखवा कर पैसे न देने वालों के लिए जुबान से कटु वचन न सही, लेकिन दिल से बद्दुआएं जरूर निकलीं। लोगों के बारे में झट से राय बना लेने की दुष्प्रवृत्ति न होती तो शायद रघुवीर सहाय से मिलने के एक-दो मौके मुझे और मिले होते।
इस दौर में मेरे लिए सबसे ज्यादा यादगार मौका चंडीगढ़ में जस्टिस अजित सिंह बैंस से मिलने का था। अपने लिए सिरे से अनजाने एक शहर में अनजानी जुबान वालों से रास्ता पूछते हुए आप एक घर के सामने पहुंचते हैं। घंटी बजा कर एक ऐसे बुजुर्ग आदमी के ड्राइंग रूम में उससे मिलने जाते हैं, जिसका नाम कई सालों से सुनते आ रहे हैं और जिसका मन ही मन बहुत सम्मान भी करते हैं। जैसे-तैसे करके आप उससे बात शुरू करते हैं और दूसरे ही वाक्य में वह आप पर चीखने लगता है- यू ब्लडी स्काउंड्रल्स… यू बर्न्ट अस पुटिंग बर्निंग टायर्स अराउंड अवर नेक्स……यू ट्राइड टु डिमॉलिश अवर रेस……हमारे केश नोच लिए…..नस्लकुशी करनी चाही हमारी …..भाड़ में गया तुम्हारा देश…..ले जाओ अप्णा देश…..हमें नीं रैणा यहां……। और इससे काफी मिलता-जुलता दूसरा मौका महज तीन दिन बाद इसी पंजाब यात्रा के दौरान आया। अमृतसर युनिवर्सिटी में पार्टी के एक पुराने साथी संधू ने अपने एक मित्र, एक स्थानीय नक्सली ग्रुप के कार्यकर्ता रहे केमिस्ट्री के रीडर…..सिंह से कराई। जैसे ही उन्हें पता चला, मैं सीपीआई एमएल लिबरेशन से हूं, वे मेरे ऊपर लगभग टूट ही पड़े……तुम लोग साले गोर्बाचोव के चमचे…..लिथुआनिया में टैंक चलवा दिए…..यहां इंडिया में भी टैंक चलाना चाहते हो पंजाब पर….।
1984 के दंगों के बाद से सिखों के मन में बैठी दहशत और उत्तर भारतीय हिंदुओं के प्रति इससे जुड़ी घृणा से मैं परिचित था, लेकिन पंजाब में इसका सामना मुझे इतने तीखेपन के साथ करना पड़ेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं था। यह 1990 का दिसंबर और 1991 का जनवरी था- एक हफ्ता इधर, एक उधर। इस वक्त भी पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट का असर कम नहीं हुआ था। गैर-सिखों के बसों से निकाल कर मारे जाने की खबरें हर दूसरे-तीसरे दिन अखबारों में आ ही जाती थीं। लेकिन सब कुछ के बाद भी मैं पंजाब में था और जस्टिस बैंस जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ता और अपनी विचारधारा के एक व्यक्ति से इतनी अपेक्षा तो करता था कि वे मुझे सिखों के जनसंहार का दोषी नहीं मान लेंगे। बहरहाल, पंजाबी सिखों से अपने इस पहले इंटरैक्शन में सारा कुछ बुरा ही बुरा नहीं हुआ। इसका एक पहलू यह भी था कि उनकी मेहरबानी से चंडीगढ़ में ही मैंने पहली बार छक कर शराब पी। शराब चखने का इससे पहले अकेला मौका इलाहाबाद में पीएसओ ऑफिस के बगल में रहने वाले धोबी परिवार में होली के दिन मिला था। चंडीगढ़ में पार्टी के एक सिंपैथाइजर दलजीत मुझे अपने मामा के घर लिवा गए, जिनके यहां बड़े लड़के के पंजाब हॉकी टीम में सिलेक्ट होने पर सेलिब्रेशन चल रहा था। दस्तूर के मुताबिक मेरे सामने भी लाई गई तो मैंने मना कर दिया। फिर मुझे लगा कि यह तो कोई एटीकेट नहीं हुआ। मैंने कहा, ठीक है एक गिलास पानी में दो बूंद डाल दीजिए। मेरा ख्याल है उस रात मैंने करीब डेढ़ बोतल ह्विस्की पी, जिसके अंत में बूढ़े सरदार जी ने कहा- चंगा मुंडा ए। उस रात अकेली अच्छी बात यह रही कि बाथरूम कमरे से सटा हुआ था और उसमें पहुंचकर जी भर उल्टियां करने की ताकत मेरे अंदर बची हुई थी।
: आंच पर खदबदाती जिंदगी : लंबी पंजाब यात्रा के बाद दिल्ली वापस लौटा तो 40, मीनाबाग का व्यवस्था पक्ष देखने वाले पार्टी के एक होलटाइमर तिवारी जी ने बताया कि आपके भाई आए थे एक आदमी के साथ, फोन नंबर देकर गए हैं। फोन किया तो पता चला तीन-चार दिन पहले ही दिल्ली पहुंचे हैं, बिड़ला मिल घंटाघर के पास अपने एक पुराने परिचित के साथ रह रहे हैं। 1983 में बहन की मौत और मंझले भाई की खुदकुशी के बाद से बड़े भाई गांव में ही रह रहे थे। खेती से खाने भर को अनाज निकाल लेते थे और कुछ पूजा-पाठ से थोड़ी-बहुत नकदी का इंतजाम कर लेते थे। पिता जी की स्थिति अब कुछ कमाने की रह नहीं गई थी और उनकी मुख्य भूमिका पोते-पोतियों का मनोरंजन करने की ही रह गई थी। इन आठ सालों में भाई दिल्ली का अपना जीवन लगभग भूल ही गए थे।  मुलाकात हुई तो घड़े में रखी हुई सी मुचड़ी-खुचड़ी पैंट-शर्ट और दोनों पैरों में बिना मोजे के दो अलग-अलग आकार वाले लाल रंग के जूते पहने हुए थे। पूछने पर पता चला कि दो दिन पहले ही इन्हें लाल किले के पीछे वाले कबाड़ी बाजार से खरीदा गया है। बोले, मेरे पास कोई पेन नहीं है, एक पेन खरीद दो, और क्या इधर-उधर आने-जाने भर को कुछ पैसों का इंतजाम हो सकता है। मैंने दीपंकर जी से 100 रुपये लेकर उन्हें दिए और नीचे आकर उन्हें बस स्टॉप तक छोड़ने के क्रम में एक पेन भी खरीद दिया। अपने से 13 साल बड़े और 1976 के एम.ए. पास अपने भाई को इस रूप में देखना अजीब था।
मुलाकात हुई तो घड़े में रखी हुई सी मुचड़ी-खुचड़ी पैंट-शर्ट और दोनों पैरों में बिना मोजे के दो अलग-अलग आकार वाले लाल रंग के जूते पहने हुए थे। पूछने पर पता चला कि दो दिन पहले ही इन्हें लाल किले के पीछे वाले कबाड़ी बाजार से खरीदा गया है। बोले, मेरे पास कोई पेन नहीं है, एक पेन खरीद दो, और क्या इधर-उधर आने-जाने भर को कुछ पैसों का इंतजाम हो सकता है। मैंने दीपंकर जी से 100 रुपये लेकर उन्हें दिए और नीचे आकर उन्हें बस स्टॉप तक छोड़ने के क्रम में एक पेन भी खरीद दिया। अपने से 13 साल बड़े और 1976 के एम.ए. पास अपने भाई को इस रूप में देखना अजीब था।
महत्वाकांक्षी लोग सपनों को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। मुझे किशोरावस्था का जो अपना सबसे महत्वाकांक्षी सपना याद है, उसमें मैंने अपने बड़े भाई को हाथ में घड़ी बांधे, नई साइकिल पर पान चबाते हुए बाजार से घर की तरफ आते देखा था। वह सपना हकीकत कभी नहीं बन सका। घड़ी और साइकिल लंबे समय तक हमारे लिए सपना ही बनी रही और फिर जेहन से ऐसे उतर गई, जैसे ऐसी चीजें दुनिया में होती ही न हों। और अब उन्हीं भाई को मैं दोनों पांवों में दो अलग-अलग साइज के लाल जूते पहने देख रहा था- आठ साल गांव में खेती-किसानी करते गुजार देने के बाद, साल-साल भर के अंतर से पैदा हुए चार बच्चों का बाप बन जाने के बाद दिल्ली में एक बार फिर अपनी रोजी-रोटी का सिलसिला शुरू करने का मन बनाते हुए। उनकी कोई मदद मुझसे नहीं हो पाई, सिवाय एक बार पटना में उनके लिए कुछ काम खोजने के मामूली से प्रयास के। मेरे दोस्त राजीव के पापा उसके मौसा जी के साथ मिल कर बेगूसराय में आम और लीची का पल्प और सॉफ्ट ड्रिंक बनाने का कारखाना खोलने का मन बना रहे थे। भाई को मैंने उनसे मिलवाया और उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में मार्केट पोटेंशियल का पता लगाने की जिम्मेदारी भाई को सौंपी। पंद्रह-बीस दिन यह कसरत उन्होंने की भी लेकिन वह कारखाना ही जमीन पर नहीं उतर सका।
भाई के गांव प्रवास के इन आठ सालों में सात मेरी होलटाइमरी के थे और इस बीच कुल तीन या चार बार मेरी उनसे मुलाकात हो picपाई थी। कभी किसी संयोग से घर चला जाता था तो वह जगह बिल्कुल मेरी पहचान में नहीं आती थी। वह अब भाभी और उनके बच्चों का घर था, जो मुझे लगभग किसी अजनबी की तरह ही देखते थे। गांव के दोस्त-मित्र ज्यादातर नौकरी-चाकरी में चले गए थे। जो बचे थे, वे यह जानकर हैरान रह जाते थे कि इतना पढ़-लिख कर भी मैं नौकरी-चाकरी कुछ नहीं करता। इसके बावजूद भाई गांव में मेरे लिए यह माहौल बनाए रखते थे कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूं और पैसे भले न कमाऊं लेकिन मेरा लिखा बंबई तक पढ़ा जाता है। मैं नहीं जानता कि उस दिन 40, मीनाबाग में मिले 100 रुपये भाई के कितने काम आए, लेकिन दिल्ली में धीरे-धीरे करके अपना धंधा उन्होंने जमा ही लिया। इसके पांच-छह साल बाद जब दिल्ली में मुझे रोजी-रोटी की फिक्र करनी पड़ी तो उनकी हैसियत हर मामले में मेरे बड़े भाई जैसी हो चुकी थी। एक बार कमरे का किराया देने के लिए मैंने उनसे एक महीने के लिए एक हजार रुपया उधार भी लिया, लेकिन सिर्फ एक बार ही, क्योंकि ऐसी किसी मदद के एवज में अपनी होलटाइमरी और लेफ्टिस्ट पागलपंथी पर उनकी एक हजार बातें सुनने की हिम्मत मैं दोबारा नहीं जुटा सकता था।
1990 के माहौल पर वापस लौटें तो देश के व्यापक राजनीतिक परिवेश से हमारे केंद्रीय नेतृत्व का कटाव इस बात से समझा जा सकता है कि जब दिल्ली में मंडल और मंदिर की रूपरेखा तैयार हो रही थी तब दिल्ली में हम लोग मार्क्सवाद के सैद्धांतिक पक्ष को लेकर एक पार्टी प्लेनम में जुटे हुए थे। इस विसंगति के बावजूद विचारधारा को लेकर यह मेरे जीवन की सबसे सघन एक्सरसाइज थी। रूस के भीतर येल्त्सिन फिनोमेना की शुरुआत हो गई थी और गोर्बाचेव का आभामंडल तक तक क्षीण होने लगा था, लेकिन दुनिया के समाजवादी हलकों में उनके विचारों की ऊष्मा अब भी बनी हुई थी। सीपीआई-एमएल को उनके बारे में कोई स्थिर राय बनानी थी और दिल्ली पार्टी प्लेनम का मुख्य उद्देश्य यही था। यह कहना किसी को शायद मेरा बड़बोलापन लगे लेकिन इस प्लेनम और 1992 की कोलकाता पार्टी कांग्रेस में विचारधारा को लेकर सबसे ज्यादा बहसें मैंने ही कीं।
पार्टी का मैं एक सामान्य कार्यकर्ता था और बहस के ऊंचे मंचों से मेरी कोई वाकफियत नहीं थी। लेकिन मन में यह आग जरूर थी कि जिंदगी अगर एक सपने के लिए होम की जा रही है तो वह कोई घटिया सपना नहीं होना चाहिए। भारत में कम्युनिज्म को रूसी और चीनी सीमाओं के साथ अमल में लाने की बात को मैं बिल्कुल पचा नहीं पाता था। भला यह कैसा सिस्टम है, जिसमें सत्य, न्याय और स्वतंत्रता कोई मूल्य नहीं है। एक दिन पटना में रूसी क्रांति के युवा नेता बुखारिन पर एक खोजी रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैंने अपने नेता वीएम को घेर लिया- कॉमरेड, स्तालिन का रूस आखिर कैसा समाज था, जिसमें सत्य कोई मूल्य ही नहीं था, जिसमें क्रांति के चौदह साल बाद लगभग सारे क्रांतिकारी नेताओं को क्रांति विरोधी करार देकर मार दिया गया। वीएम ने बहुत सोचने के बाद एक लाइन का जवाब दिया- ट्रुथ इज नॉट समथिंग टु बी फाउंड ऑन सर्फेस, ट्रुथ इज समथिंग टु बी सीक्ड आउट (व्याकरण के अनुसार शायद यह सॉट आउट हो, लेकिन वीएम ने कहा यही था)। मैं उनकी इस बात से तो सहमत था कि रूस की सच्चाइयां जानने के लिए हमें इंतजार करना चाहिए, लेकिन खुद को पेटी बुर्जुआ बता दिए जाने के डर से अपने सवालों को ठंडे बस्ते में डाल देने के लिए कतई तैयार  नहीं था।
नहीं था।
हम सर्वहारा के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अपने लिए भी तो लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई जमीन और नौकरी के लिए नहीं, मनुष्य को उसकी सभी आजादियों के साथ देखने के लिए है- उसके लिए है, जिसे मार्क्स क्रांति कहा करते थे और जिसका वादा लेनिन और माओ ने भी अपने समाज से कर रखा था। 1990 में मुझे लगता था कि गोर्बाचेव की डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की अवधारणा ही हमारे सपनों के समाज के सबसे ज्यादा करीब है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और सोशल डेमोक्रेसी में बुनियादी फर्क विशेषण और विशेष्य का है, जिसके बारे में यहां विस्तार में जाने की जगह नहीं है। सोशल डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी मिसालें नॉर्वे और स्वीडन को माना जाता है लेकिन ये देश भी एकाधिकारवादी पूंजी की बुराइयों से मुक्त नहीं हैं- खासकर स्वीडन की बोफोर्स तोप को लेकर उस समय चल रही कुछ ज्यादा ही सघन चर्चा यह साफ करने के लिए काफी थी। मुझे गोर्बाचेव की राजनीति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, रूसी समाज में उनकी राजनीतिक हैसियत के बारे में भी मुझे खास पता नहीं था। लेकिन उनकी पेरेस्त्रोइका मैंने ठीक से पढ़ी थी। यह कोई दिलचस्प किताब नहीं थी। रूस की गैर साहित्यिक किताबें वैसे भी काफी बोर हुआ करती हैं और यह तो बाकायदा एक राष्ट्रपति की लिखी हुई किताब ही थी। लेकिन इसकी कई बातों में दम था इसलिए कई सिटिंग में जैसे-तैसे करके मैं इसे पढ़ ही गया था। पार्टी की राय 1990 प्लेनम में गोर्बाचेव को खारिज करने की थी, लेकिन मैंने मंच से कई-कई बार उनके बारे में इंतजार करने की दलीलें दीं। यहां तक कहा कि गोर्बाचेव रहें या भाड़ में जाएं, लेकिन सोशलिज्म विद डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन फेस वाली उनकी बात को कतई छोड़ा न जाए।
इन गंभीर बहसों से परे हमारे राजनीतिक गढ़ बिहार में एक नया ही खेल शुरू हो गया था। बिहार में एक अजीब राजनीतिक बीजगणित के जरिए सत्ता में आए लालू यादव ने अपनी डगमगाती सत्ता के लिए दो बड़े मजबूत पाए खोज लिए थे। मंडल आयोग की अनुशंसाओं के जरिए अपने इर्द-गिर्द पिछड़ा गोलबंदी बनाने के साथ ही उन्होंने बिहार पहुंची राम रथयात्रा के अगुआ लाल कृष्ण आडवाणी की सांकेतिक गिरफ्तारी करके राज्य के मुसलमानों को भी अपना भक्त बना लिया था। बिहार की राजनीति अभी तक कांग्रेस के पक्ष या विपक्ष के दो ध्रुवों के बीच ही घूमती आई थी, जिसमें हमारे लिए अच्छी-खासी जगह बन गई थी। लेकिन अक्टूबर 1990 के सिर्फ एक महीने में इस विशाल राज्य में कांग्रेस की जड़ ही खत्म हो गई। राजनीति में इतना बड़ा बदलाव इतने कम समय में शायद ही कभी आया हो। हमें इसका पता नहीं चला तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बिहारी राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी जगन्नाथ मिश्रा भी यही मानते थे कि लालू यादव एक साल से ज्यादा बिहार की गद्दी पर नहीं रह पाएंगे। लेकिन हमें इसका अंदाजा नहीं था कांग्रेस की तरह हमें भी अपनी इस नासमझी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालत यह हुई कि चंद्रशेखर की सरकार गिरने के बाद अप्रैल-मई 1991 में जब नए आम चुनाव के लिए मैं दिल्ली से आरा पहुंचा तो लोगों के बीच घूमते हुए लगता ही नहीं था कि यह वही जगह है जहां मात्र सवा साल पहले हमने इतनी अच्छी जीत हासिल की थी।
: कहो कटुआप्रेमी, आड़ में क्यों हो? : राजनीति और पत्रकारिता में रहते हुए आदमी इंपर्सनल होना सीख लेता है। मुश्किल उन लोगों के साथ होती है, जिनकी बुनावट में इंपसर्नल होने की ज्यादा जगह नहीं होती। उनका काम उन्हें एक तरफ खींचता है और मन दूसरी तरफ ले जाता है। 1990 में दिल्ली में अपना रहना कुछ ऐसी ही उधेड़बुन से भरा हुआ था। बहुत सारी प्रोजाइक यादें दिमाग में भरी हुई हैं, पर कुछ भी ऐसा नहीं है, जो नजदीकी से बांधता हो। बाहर जारी राजनीति के हाहाकार में मन के करीब सिर्फ दो या तीन किताबें थीं। टॉमस हार्डी की फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड (कानों में फुसफुसाते हुए से लगते उसके प्राकृतिक दृश्य। खासकर उसकी रातें, जिन्होंने दिल की तहों तक मुझे रात का राही ही बना डाला), अल्बर्टो मोराविया की डिसीक्रेशन (जो लगाव से ज्यादा अपनी वितृष्णा के लिए याद आती है), और दोस्तोएव्स्की की ईडियट (जिसने अपने लाखों पाठकों की तरह मुझे भी जिंदगी से दूर ले जाकर जिंदगी के करीब ला दिया)। गैर-साहित्यिक किताबों में विनायक पुरोहित की लिखी और जेएनयू की लाइब्रेरी से किसी मित्र के जरिए इशू कराकर पढ़ी गई बहुत लंबे टाइटल वाली एक किताब- शायद आर्ट एंड कल्चर इन ट्वेंटीथ सेंचुरी ट्रांजिशनल इंडिया याद आती है- भारतीय कला-संस्कृति के बारे में वैसा मूर्तिभंजक नजरिया फिर कभी पढ़ने को नहीं मिला।
: मुलायम बनाम वीपी : अक्टूबर 1990 से मार्च 1991 के बीच की घटनाओं का सीक्वेंस पकड़ने में मुझे सबसे ज्यादा परेशानी होती है। फ्लैशेज की शक्ल में चीजें याद आती हैं। बड़ा कन्फ्यूज्ड किस्म का समय था। मुलायम सिंह यादव को यूपी में मंडल का सबसे ज्यादा फायदा मिला और कमंडल विरोध का सबसे ज्यादा श्रेय भी। पिछले कुछ सालों में जो लोग मंडल-मंदिर के फॉर्मूले से भारतीय राजनीति को देखने के आदी हो चले हैं, वे इसके आधार पर इस नतीजे तक पहुंच सकते हैं कि मुलायम सिंह वीपी सिंह के काफी करीबी रहे होंगे। लेकिन सचाई यह है कि जनता दल के भीतर वीपी सिंह को सबसे ज्यादा विरोध मुलायम सिंह का ही झेलना पड़ा- मंडल आने के पहले भी और इसके बाद भी। संसद में वीपी की सरकार से बीजेपी की समर्थन वापसी के बाद जनता दल के दफ्तर पर कब्जे के लिए पार्टी के वीपी और चंद्रशेखर गुटों के बीच बने जबर्दस्त तनाव की याद भी मुझे है, जिसमें वीपी की सारी मंडल छवि के बावजूद यूपी के ज्यादातर बैकवर्ड नेता बरास्ता मुलायम, चंद्रशेखर गुट के साथ खड़े थे, जबकि इलाहाबाद युनिवर्सिटी में ब्राह्मण गुंडई के पुरोधा समझे जाने वाले कमलेश तिवारी जैसे नेता जयपाल रेड्डी के बगल में खड़े होकर वीपी गुट की तरफ से हांफ-हूंफ करते हुए गालियां बक रहे थे।
: आड़ खोजता गुनाह!! : पता नहीं इसके पहले या इसके बाद, शायद इसके पहले ही, 30 अक्टूबर को मैं लखनऊ में था। अरुण पांडे (फिलहाल न्यूज 24 के इनपुट एडिटर) और मैं हजरत गंज चौराहे  पर खड़े थे। बीजेपी के लोग अयोध्या में विवादित स्थल पर लगी घेरेबंदी और कारसेवकों को फैजाबाद पहुंचने से रोके जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहां से खबरें आनी अभी तक शुरू नहीं हुई थीं लेकिन अफवाहों की चक्की रात से ही चल रही थी। अचानक भीड़ उग्र हो गई। चौराहे पर तोड़फोड़ शुरू हो गई। पुलिस लाठियां चलाने लगी और भीड़ पत्थर। वहां खड़े बाकी पत्रकारों की तरह हम लोग भी आड़ खोज रहे थे। तभी अरुण के परिचित, लगभग रोज ही कॉफी हाउस में उनके साथ उठने-बैठने वाले एक युवा पत्रकार ने सड़क के उस पार से नारा सा लगाते हुए अरुण और उनके साथ खड़े मुझे ललकारा- ”कहो कटुआप्रेमी, वहां आड़ में क्या कर रहे हो।” अचानक समझ में नहीं आया कि अब हम लोग पुलिस से खुद को बचाएं या भीड़ से। लगा कि ऐसी ही है पत्रकारिता की लाइन, जहां आप कभी नहीं जान पाते कि कौन क्या है और किसके लिए काम कर रहा है।
पर खड़े थे। बीजेपी के लोग अयोध्या में विवादित स्थल पर लगी घेरेबंदी और कारसेवकों को फैजाबाद पहुंचने से रोके जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहां से खबरें आनी अभी तक शुरू नहीं हुई थीं लेकिन अफवाहों की चक्की रात से ही चल रही थी। अचानक भीड़ उग्र हो गई। चौराहे पर तोड़फोड़ शुरू हो गई। पुलिस लाठियां चलाने लगी और भीड़ पत्थर। वहां खड़े बाकी पत्रकारों की तरह हम लोग भी आड़ खोज रहे थे। तभी अरुण के परिचित, लगभग रोज ही कॉफी हाउस में उनके साथ उठने-बैठने वाले एक युवा पत्रकार ने सड़क के उस पार से नारा सा लगाते हुए अरुण और उनके साथ खड़े मुझे ललकारा- ”कहो कटुआप्रेमी, वहां आड़ में क्या कर रहे हो।” अचानक समझ में नहीं आया कि अब हम लोग पुलिस से खुद को बचाएं या भीड़ से। लगा कि ऐसी ही है पत्रकारिता की लाइन, जहां आप कभी नहीं जान पाते कि कौन क्या है और किसके लिए काम कर रहा है।
: अयोध्या बनाम जलियांवाला : दोपहर बाद से अखबारों के दफ्तरों में संख्याओं का खेल शुरू हुआ। अयोध्या में मुल्ला मुलायम की चलाई गोलियों से कितने लोग मारे गए। मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन बाद में कवि और संपादक वीरेन डंगवाल से उस दिन के किस्से सुने। एजेंसियों ने पांच लोगों के मारे जाने की खबर चलाई थी। लखनऊ के एक अखबार ने शाम को निकाले अपने एक विशेष संस्करण में सीधे ही एक जीरो बढ़ाकर इसे पचास कर दिया था। शाम को उसके प्रतिद्वंद्वी अखबार में संपादक और डेस्क के वरिष्ठ जनों के बीच एक गंभीर बहस चली, जिसका नतीजा यह निकला कि अगर हम अयोध्या कांड को जलियांवाला बाग कांड जैसा या उससे भी बड़ी घटना बता रहे हैं तो पचास से बात नहीं बनेगी। इस तरह रातोंरात बात सैकड़ों में- पांच से उछलकर सीधे पांच सौ तक पहुंच गई। गालियों से भरे, अतार्किक, सांप्रदायिक लोगों को भी सांप्रदायिक लगने वाले भाषणों का दौर। जातिगत विद्वेष से गले तक भरे हुए लोग, जो मंडलीकृत माहौल में अपने को जाति से ऊपर दिखाने के लिए खुद को ब्राह्मण-ठाकुर के बजाय हिंदू बताने में जुटे थे। एक ऐसा समय, जब आप बिना दस बार सोचे किसी से एक बात नहीं कर सकते थे। ऐसे दौर में बाकी लोगों की तरह मुझे भी कहीं कोई छोटी सी जमीन चाहिए थी, जहां पांव टिका कर खड़ा हुआ जा सके।
: असंतोष के दिन : पार्टी इस नतीजे तक पहुंच चुकी थी कि वीपी की विदाई के बाद कांग्रेस के समर्थन से बनी चंद्रशेखर सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं थी। संसद किसी भी दिन भंग हो सकती थी। संसद में अपनी अब तक की एकमात्र सीट बचाने के लिए नहीं, सैकड़ों कुर्बानियों की कीमत पर तैयार किया गया अपना जनाधार बचाने के लिए अपने सभी संसाधन तत्काल अपने आधार इलाकों में झोंक दिए जाने चाहिए। चंद्रशेखर की सरकार कुल चार महीने चली लेकिन उसका अंत  देखने के लिए मैं दिल्ली में नहीं था। शायद जनवरी के अंत में पटना पहुंचने के बाद कुछ दिनों के लिए नेपाल गया। वहां 1990 के विराट जनांदोलन के बाद पहली बार संसदीय चुनाव होने जा रहे थे। जनमत की तरफ से मैं उस आंदोलन को भी कवर करने नेपाल गया था लेकिन मौका सिर्फ रक्सौल का पुल पार करके बीरगंज जाने भर का मिला। पूरे देश में तोडफोड़ और पुलिस कार्रवाई का माहौल था। काठमांडू के लिए कोई सवारी मिल पाने का कोई लक्षण अगले कई दिनों तक दिखाई नहीं दे रहा था, लिहाजा वहीं से मुझे वापस लौटना पड़ गया था। इसके अगले कदम के रूप में 1991 की फरवरी में की गई अपनी नेपाल यात्रा पर पांच किस्तें मैं अपने ब्लॉग पहलू में लिख चुका हूं। मुझे लगता है, उन्हें पढ़कर आज के नेपाल को समझने में थोड़ी मदद मिल सकती है।
देखने के लिए मैं दिल्ली में नहीं था। शायद जनवरी के अंत में पटना पहुंचने के बाद कुछ दिनों के लिए नेपाल गया। वहां 1990 के विराट जनांदोलन के बाद पहली बार संसदीय चुनाव होने जा रहे थे। जनमत की तरफ से मैं उस आंदोलन को भी कवर करने नेपाल गया था लेकिन मौका सिर्फ रक्सौल का पुल पार करके बीरगंज जाने भर का मिला। पूरे देश में तोडफोड़ और पुलिस कार्रवाई का माहौल था। काठमांडू के लिए कोई सवारी मिल पाने का कोई लक्षण अगले कई दिनों तक दिखाई नहीं दे रहा था, लिहाजा वहीं से मुझे वापस लौटना पड़ गया था। इसके अगले कदम के रूप में 1991 की फरवरी में की गई अपनी नेपाल यात्रा पर पांच किस्तें मैं अपने ब्लॉग पहलू में लिख चुका हूं। मुझे लगता है, उन्हें पढ़कर आज के नेपाल को समझने में थोड़ी मदद मिल सकती है।
: जनमत के बंद होने की भूमिका : अगड़ा-पिछड़ा राजनीति के पेच समझने के लिए 1991 का बिहार एक अद्भुत जगह थी।मंडल लहर में जब बसें रोक-रोक कर अगड़े गांवों में पिछड़ों की और पिछड़े गांवों में अगड़ों की पिटाई हो रही थी तो हमारी पार्टी के एक पुराने नेता एक दिन ऐसी ही बस में फंस गए। बाकी यात्रियों की तरह उनकी भी जात पूछी गई तो उन्होंने हाथ जोड़ कर खुद को पासी बता दिया और सिर्फ गालियां खाकर बच निकले। अगड़ों-पिछड़ों की इस लड़ाई में खुद को मुसलमान बताना भी खतरनाक था, लेकिन दलितों को दोनों खेमे गाली-गुफ्ता देकर छोड़ देते थे। बहरहाल… बिहार में इस साल की राजनीतिक शुरुआत तिसखोरा जनसंहार कांड से हुई थी। पटना ग्रामीण के तिसखोरा गांव में दबंग यादव जाति के कुछ लोगों का कुम्हार बिरादरी के कुछ लोगों से टकराव चल रहा था। बिहार की बाकी सभी अति पिछड़ी जातियों की तरह कुम्हार जाति भी सीपीआई-एमएल लिबरेशन के साथ हमदर्दी रखती आई है, हालांकि तिसखोरा की गिनती उस समय तक हमारे मजबूत जनाधार वाले गांवों में नहीं हुआ करती थी।
इस टकराव को लेकर गांव के दबंग यादवों ने अपनी बिरादरी के ताकतवर नेताओं से संपर्क किया और उस समय- मुख्यमंत्री पद पर लालू यादव की मौजूदगी के बावजूद राज्य के सबसे ताकतवर यादव समझे जाने वाले राम लखन सिंह यादव का संरक्षण प्राप्त किया। इसके अगले कदम के रूप में उन्होंने कुम्हार टोली पर हमला किया, जिसमें कुल पंद्रह लोग मारे गए। लिबरेशन ने इसके विरोध में बिहार बंद का आह्वान किया लेकिन हम यह जानकर चकित थे कि जनता दल के अलावा सीपीआई और सीपीएम ने भी हत्याकांड के मुद्दे को पीछे छोड़ते हुए यह कहना शुरू कर दिया कि माले वाले लोग इस घटना में यादवों को फंसा रहे हैं और राम लखन सिंह का नाम उछाल रहे हैं- इसलिए क्योंकि वे पिछड़ा विरोधी और मंडल विरोधी लोग हैं। मुझे लोकलहर और पीपुल्स डेमोक्रेसी में सीताराम येचुरी के नाम से लिखी इस आशय की रिपोर्ट के कई शब्द अब तक याद हैं।
यही राम लखन सिंह यादव आरा संसदीय क्षेत्र से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ने आए और उनके सामने खड़े हुए चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में धनबाद के कोल  माफिया सूर्यदेव सिंह। बता चुका हूं कि इससे ठीक पहले हुए चुनाव में इस सीट से हमारे प्रत्याशी किसान नेता रामेश्वर प्रसाद चुनाव जीते थे, जो नोनिया बिरादरी से आते थे, जिसकी कुल जनसंख्या दस लाख से आबादी वाले इस संसदीय क्षेत्र में पांच हजार से ज्यादा नहीं थी। यह पहला चुनाव था, जिसमें मुझे खुलेआम जातीय टकराव की राजनीति देखने को मिली। आरा में यादवों और राजपूतों के बीच टकराव का कोई इतिहास नहीं है। जहां-तहां भूमिहार बिरादरी और यादवों के बीच लड़ाई जरूर रही है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर इसका रूप संगठित वैचारिक लड़ाई का ही रहा है, चाहे वह सोशलिस्ट मूवमेंट के हिस्से के रूप में रही हो या सीपीआई के, या फिर माले के। अलबत्ता इन दोनों बिरादरियों की आबादी क्षेत्र में लगभग कांटे की है और ललकारने पर ताव खा जाने की प्रवृत्ति भी लगभग एक सी ही है। गनीमत रही कि इस ध्रुवीकरण में किसी बड़े कतल-बलवे की नौबत नहीं आई। अलबत्ता पोलिंग के दिन दोनों में जिसका भी जहां वश चला, उसने हमारे, यानी तीसरे खेमे के वोट लूट लिए। चुनाव नतीजा सुनाए जाने से ठीक पहले सूर्यदेव सिंह की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई लेकिन काउंटिंग के दौरान उनके समर्थकों की आक्रामकता इससे घटने के बजाय और बढ़ गई थी। उन्हें दो लाख से ज्यादा वोट मिले थे। पौने तीन लाख लेकर राम लखन सिंह चुनाव जीते। रामेश्वर जी न सिर्फ पहले से तीसरे पर आ गए बल्कि हमारे वोटों की संख्या भी पौने दो लाख से घटकर डेढ़ लाख पर आ गई। पार्टी के लिए यह एक धक्के जैसी स्थिति थी और बाकी सबकी तरह मुझे भी इससे निकलने के लिए कुछ करना जरूरी लग रहा था।
माफिया सूर्यदेव सिंह। बता चुका हूं कि इससे ठीक पहले हुए चुनाव में इस सीट से हमारे प्रत्याशी किसान नेता रामेश्वर प्रसाद चुनाव जीते थे, जो नोनिया बिरादरी से आते थे, जिसकी कुल जनसंख्या दस लाख से आबादी वाले इस संसदीय क्षेत्र में पांच हजार से ज्यादा नहीं थी। यह पहला चुनाव था, जिसमें मुझे खुलेआम जातीय टकराव की राजनीति देखने को मिली। आरा में यादवों और राजपूतों के बीच टकराव का कोई इतिहास नहीं है। जहां-तहां भूमिहार बिरादरी और यादवों के बीच लड़ाई जरूर रही है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर इसका रूप संगठित वैचारिक लड़ाई का ही रहा है, चाहे वह सोशलिस्ट मूवमेंट के हिस्से के रूप में रही हो या सीपीआई के, या फिर माले के। अलबत्ता इन दोनों बिरादरियों की आबादी क्षेत्र में लगभग कांटे की है और ललकारने पर ताव खा जाने की प्रवृत्ति भी लगभग एक सी ही है। गनीमत रही कि इस ध्रुवीकरण में किसी बड़े कतल-बलवे की नौबत नहीं आई। अलबत्ता पोलिंग के दिन दोनों में जिसका भी जहां वश चला, उसने हमारे, यानी तीसरे खेमे के वोट लूट लिए। चुनाव नतीजा सुनाए जाने से ठीक पहले सूर्यदेव सिंह की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई लेकिन काउंटिंग के दौरान उनके समर्थकों की आक्रामकता इससे घटने के बजाय और बढ़ गई थी। उन्हें दो लाख से ज्यादा वोट मिले थे। पौने तीन लाख लेकर राम लखन सिंह चुनाव जीते। रामेश्वर जी न सिर्फ पहले से तीसरे पर आ गए बल्कि हमारे वोटों की संख्या भी पौने दो लाख से घटकर डेढ़ लाख पर आ गई। पार्टी के लिए यह एक धक्के जैसी स्थिति थी और बाकी सबकी तरह मुझे भी इससे निकलने के लिए कुछ करना जरूरी लग रहा था।
चुनाव खत्म होने के बाद पटना में वापस जनमत के डेरे पर पहुंचकर मैंने रामजी भाई से कहा कि जनमत में अब मेरा मन नहीं लग रहा है और अब मैं आरा जाकर पार्टी का काम करना चाहता हूं। मेरी तरफ से यह एक किस्म का बिट्रेयल, एक तरह की गद्दारी थी। लेकिन जिस तरह का ठहराव मैं अपने भीतर महसूस कर रहा था, उससे निकलने का अकेला तरीका मुझे यही समझ में आ रहा था। जनमत का प्रकाशन पिछले दो महीने से चुनाव के लिए स्थगित था। 1991 का संसदीय चुनाव भी खुद में बड़ा अजीब सा था। पांच दौर के चुनाव में दूसरे या शायद तीसरे दौर में राजीव गांधी की हत्या हो जाने से चुनाव स्थगित हो गए थे। इस तरह एक महीने का चुनाव कुल ढाई महीनों में संपन्न हो पाया था। जनमत के भविष्य को लेकर राजवंशी नगर स्थित महेंद्र सिंह के विधायक फ्लैट में- जो एक साल से जनमत के दफ्तर का काम कर रहा था- एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें पत्रिका के अलावा पार्टी महासचिव विनोद मिश्र और कुछ अन्य बड़े पार्टी नेता भी शामिल हुए। पार्टी 1990 में विधानसभा चुनाव और लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही धक्के का सामना कर रही थी और अकेली जीती हुई संसदीय सीट चले जाने से इस धक्के का जोर और भी बढ़ गया था। पार्टी के सामने सवाल यह था कि इस घोर जातिवादी और सांप्रदायिक माहौल में, साथ में सोवियत संघ से लगातार आ रही कम्युनिज्म विरोधी खबरों के बीच पार्टी के जनाधार को कैसे टिकाया जाए। ऐसे में जनमत के बजाय सीधे पार्टी का काम करने के मेरे प्रस्ताव को जनमत में न सही लेकिन पार्टी में काफी उत्साह के साथ लिया गया था। लेकिन समस्या यह थी कि इतने सारे लोगों के इधर-उधर होने के बाद जनमत निकलेगा कैसे।
विष्णु राजगढ़िया को पार्टी के छह सदस्यीय विधायक दल के लिए वैचारिक सामग्री तैयार करने की जिम्मेदारी मिली हुई थी और जनमत के लिए वे समय बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे थे। प्रदीप झा को पटना शहर की पार्टी इकाई अपने लिए मांग रही थी। महेश्वर जी की तबीयत भी उन्हीं दिनों खराब होनी शुरू हुई थी, जो बाद में किडनी ट्रांसप्लांटेशन और फिर उनकी असामयिक मृत्यु तक गई। खुद रामजी राय की भी पार्टी जिम्मेदारियां पहले से ज्यादा बढ़ गई थीं। लब्बोलुआब यह कि जनमत के पास वर्क फोर्स का अकाल हो गया। मीटिंग में रामजी भाई ने बड़ी हतक के साथ जनमत बंद करने का प्रस्ताव रखा, जो शायद सेंट्रल कमिटी का फैसला भी था। इस मीटिंग में मैंने जिंदादिल महेश्वर जी को बहुत ही उदास देखा। इस तरह अपने साप्ताहिक रूप में जनमत बंद हो गई, हालांकि इसे प्रकाशन स्थगित करने का नाम दिया गया। महेश्वर और इरफान इसके बाद पटना में सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा करने में जुटे और इसमें कुछ मील के पत्थर कायम किए।
: आरा में वह पहली रात : आरा शहर में बतौर पोलिटिकल होलटाइमर अपनी पहली रात मुझे हमेशा याद रहेगी। पार्टी इस समय भूमिगत थी और जिला सेक्रेटरी दीना जी एक अचर्चित ठिकाने पर हमें भोजपुर के अभी के हालात के बारे मे बता रहे थे। हमें से मतलब मुझे और कुणाल जी से है, जो भोजपुर के डिप्टी पार्टी सेक्रेटरी के रूप में पिछले कुछ महीनों से यहां मौजूद थे। रात के कोई ९ बज रहे होंगे। आरा में बिजली का हाल अभी कैसा है, मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय बिजली वाले घंटे २४ में २-४ ही हुआ करते थे। बाहर अंधेरा इतना घना था कि लग रहा था, बहुत रात हो गई है। अचानक बाहर बहुत जोर का हल्ला मचा। कई परिवारों की रिहाइश वाली उस डब्बानुमा इमारत में हम लोग तीसरे तल्ले पर थे। दीना जी शोर सुनते ही बिल्ली की तरह चौकन्ने हो गए और खिड़की से  बाहर या पाइप के सहारे आंगन में कूदकर निकल लेने का उपक्रम करने लगे। नीचे पुलिस के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए लगाया गया एक लड़का तभी दौड़ा हुआ आया और बोला कि नीचे कुछ बदमाश टाइप लोग किसी को धमका रहे हैं।
बाहर या पाइप के सहारे आंगन में कूदकर निकल लेने का उपक्रम करने लगे। नीचे पुलिस के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए लगाया गया एक लड़का तभी दौड़ा हुआ आया और बोला कि नीचे कुछ बदमाश टाइप लोग किसी को धमका रहे हैं।
जिन साथी के यहां हम रुके हुए थे वे नीचे गए और थोड़ी देर में मामला रफा-दफा करके लौटे। पता चला कि नीचे कोई धंधे वाली औरत अपनी बेटी के साथ रहती है। उसी के यहां कुछ बदमाश आये थे और औरत से लड़की को अपने साथ भेज देने के लिए झगड़ा कर रहे थे। औरत खुद उनके साथ जाने के लिए तैयार थी क्योंकि यही उसका पेशा था। लेकिन लड़की को वह इस काम से बाहर रखना चाहती थी। लोगों के जमा हो जाने के बाद मार-पीट पर उतारू गुंडे ठिठक गए लेकिन जाते-जाते धमकी देते गए कि रात में १ बजे वे फिर आएंगे और लडकी को लेकर ही जायेंगे। दीना जी उसूलन रात का खाना जहां भी खाते थे वहां ठहरते नहीं थे। यह अंडरग्राउंड लाइफ की एक जरूरी शर्त थी। लिहाजा करीब ११ बजे हम तीनों लोग अपने साथी गया जी के यहां से उठे और एक मोहल्ला फांदकर एक समर्थक के यहाँ जाकर सो गए।
सुबह-सुबह अपनी आदत के मुताबिक टहलते हुए जब मैं रात वाली जगह पर पहुंचा तो वहां देर रात में घटी घटनाओं की गंध मौजूद थी। धमकी देने वाले वाले उस रात ठीक १ बजे सचमुच वहाँ आये थे। उन्होंने गेट पर फायरिंग की, दरवाजा तोड़ा और टारगेट की हुई लड़की को बाहर तक खींच लाए। पूरी बिल्डिंग में किसी की हिम्मत नहीं पडी़ कि उनसे पंगा ले। तब ऊपर से हमारे साथी गया जी ने कट्टे से फायर मारा और चिल्लाये। रात में गूंजती हुई उनकी आवाज पड़ोस में ही मौजूद उनकी पुश्तैनी बस्ती श्रीटोला तक पहुंची। पास में ही दिन-रात जागने वाला बस स्टैंड भी था जहाँ उनकी दुसाध बिरादरी का दबदबा चलता था। गया जी की आवाज सुनकर लोग ललकारते हुए आगे बढ़े तो बदमाशों को लगा कि वे लड़की को लेकर निकल नहीं पाएंगे। आखिरकार वे उसे छोड़कर इधर-उधर हो गए।
मजे की बात यह कि घटना स्थल से पुलिस थाने की दूरी बस स्टैंड या श्रीटोला जितनी ही, बल्कि उनसे कुछ कम ही थी, लेकिन रात में तो दूर, सुबह भी वहां से किसी ने इधर आना जरूरी नहीं समझा। जिस इमारत में यह सब हुआ था वहां सभी किरायेदार ही रहते थे। पुलिस से कुछ कहने का कोई मतलब उन्हें भी समझ में नहीं आया। अलबत्ता सभी ने मिलकर महिला से कहीं और मकान तलाश लेने के लिए कहा।
मैंने दीना जी से पूछा कि जवान लड़की के साथ यह बेचारी औरत कहां जायेगी। यहां तो किसी तरह बच गयी लेकिन किसी और जगह कैसे बचेगी? बेचारगी में उन्होंने सिर हिला दिया क्योंकि इस मामले में कुछ भी बोलने का मतलब कुछ और ही लगाया जाता और फिर गया जी के लिए वहां रहना मुश्किल हो जाता। आरा में मेरे लिए यह एक तरह की शॉक-लैंडिंग थी। आने वाले दिनों में ऐसे ही माहौल में मुझे रहना और काम करना था, जहां शहराती विकृतियाँ अपने चरम पर थीं लेकिन कायदे-कानून की हालत बिल्कुल पिछडे़ देहाती इलाकों से भी गई-गुजरी थी।
भोजपुर में मेरी पहली राजनीतिक कार्रवाई दो मैराथन बैठकें थीं। पहले बक्सर के चौगाईं गांव में तीन दिन लंबी जिला कमिटी और फिर उदवंतनगर के पता नहीं किस गांव में पूरे पांच दिन जिला कार्यकारिणी। इस नतीजे को लेकर सभी के बीच आम सहमति थी कि बिहटा हत्याकांड के बाद से भोजपुर में पार्टी के काम को धक्का लगा है। लेकिन खोजबीन के बाद पता चला कि कई ज्यादा गहरी आंतरिक समस्याएं पार्टी को भीतर ही भीतर खा रही हैं। आईपीएफ में सक्रिय पार्टी के जननेता व्यापारियों और ठेकेदारों से बड़े-बड़े चंदे वसूलते हैं और उनका वर्गचरित्र भी दिनोंदिन उनके जैसा ही होता जा रहा है। पार्टी के आम कार्यकर्ताओं में संघर्ष चेतना कुंद पड़ी है। जहां भी जम कर मोर्चा लेना होता है, वे कुछ भाषण वगैरह देकर पतली गली से कहीं और निकल लेते हैं। संघर्ष के नाम पर हथियारबंद दस्तों की धमकी भर से काम चलाते हैं। वह धमकी भी ज्यादा असरदार नहीं साबित होती, क्योंकि बिहटा के जवाब में कोई उतनी ही बड़ी कार्रवाई पार्टी नहीं कर पाई है। इस कलंक से उबरने के लिए हथियारबंद योद्धा कम से कम एक जवाबी जनसंहार करने की इजाजत न जाने कब से मांग रहे हैं, और न मिलने पर उनमें से कुछ तो पार्टी छोड़ कर बागी बन जाने की धमकी भी देने लगे हैं।
बक्सर की मीटिंग में दीनाजी ने मेरा परिचय जनमत के साथी के रूप में कराया था, फिर धीरे-धीरे यह खुलासा किया था कि ये अब यहीं रहकर पार्टी का काम करने आए हैं। किस तरह का काम करेंगे, इसके जवाब में मैंने कहा कि बिल्कुल जमीनी काम। संगठन खड़ा करना, वर्ग संघर्ष के पॉकेट बनाना, छोटे-मोटे आंदोलन चलाना, चंदा-चुटकी करना। गांव में करेंगे या शहर में। मैंने कहा, कोई आग्रह नहीं है लेकिन गांव में ज्यादा सही रहेगा। जिला कमिटी की राय बनी कि आरा शहर से जुड़े पार्टी के दोनों बड़े नेता- सुदामा प्रसाद और अजित गुप्ता फिलहाल जेल में हैं, लिहाजा मेरा आरा में ही रहकर काम करना पार्टी के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। गांव से जुड़े रहने के लिए आरा शहर से सटे मोफस्सिल ब्लॉक का प्रभार मुझे सौंपा गया, साथ में अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में पार्टी के प्रवक्ता का काम भी दिया गया। उस समय तक पार्टी के सिर्फ एक, केंद्रीय प्रवक्ता कॉमरेड बृजबिहारी पांडे हुआ करते थे, लेकिन बक्सर की मीटिंग में भोजपुर जिला कमिटी को लगा कि पार्टी की सही छवि जनता के बीच ले जाने के लिए एक प्रवक्ता उसके पास भी होना चाहिए।
….जारी…
 चंद्रभूषण को उनके जानने वाले चंदू या चंदू भाई के नाम से पुकारते हैं. चंदू भाई हिन्दी के वरिष्ठ पत्रकार हैं. इलाहाबाद, पटना और आरा में काम किया. कई जनांदोलनों में शिरकत की. नक्सली कार्यकर्ता भी रहे. ब्लाग जगत में इनका ठिकाना ”पहलू” के नाम से जाना जाता है. सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर बहुआयामी सरोकारों के साथ प्रखरता और स्पष्टता से अपनी बात कहते हैं. इन दिनों दिल्ली में नवभारत टाइम्स से जुड़े हैं. चंदू भाई से यह डायरी लिखवाने का श्रेय वरिष्ठ पत्रकार और ब्लागर अजित वडनेरकर को जाता है. अजित जी के ब्लाग ”शब्दों का सफर” से साभार लेकर इस डायरी को यहां प्रकाशित कराया गया है.
चंद्रभूषण को उनके जानने वाले चंदू या चंदू भाई के नाम से पुकारते हैं. चंदू भाई हिन्दी के वरिष्ठ पत्रकार हैं. इलाहाबाद, पटना और आरा में काम किया. कई जनांदोलनों में शिरकत की. नक्सली कार्यकर्ता भी रहे. ब्लाग जगत में इनका ठिकाना ”पहलू” के नाम से जाना जाता है. सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर बहुआयामी सरोकारों के साथ प्रखरता और स्पष्टता से अपनी बात कहते हैं. इन दिनों दिल्ली में नवभारत टाइम्स से जुड़े हैं. चंदू भाई से यह डायरी लिखवाने का श्रेय वरिष्ठ पत्रकार और ब्लागर अजित वडनेरकर को जाता है. अजित जी के ब्लाग ”शब्दों का सफर” से साभार लेकर इस डायरी को यहां प्रकाशित कराया गया है.