हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पीपली लाइव ने धूम मचा रखी है. फिल्म के मूल में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का फटीचरपन दिखाया गया है. वैसे तो फिल्म में मीडिया के अलावा भी समाज के अन्य पहलुओं को छुआ गया है. पर पूरा फोकस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ही है. फिल्म में आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर रूप के दर्शन हो जायेंगे. फिल्म में एक खास बात है फिल्म में एक स्ट्रिंगर राकेश की मौत. राकेश संवेदनशील पत्रकार था. किसी बड़े मीडिया चैनल में नौकरी पाना उसका सपना था. सब कुछ खत्म होने के बाद कोई भी राकेश को याद नहीं रखता और वह नेपथ्य में ही गुम हो जाता है.
राकेश सबसे पहले नत्था की आत्महत्या की खबर अपने एक छोटे से अखबार में छापता है जिसको आधार बनाकर एक अंगरेजी समाचार चैनल स्टोरी करता है और फिर सारी दुनिया के मीडिया का जमावड़ा लग जाता है. ये स्ट्रिंगर मीडिया की दुनिया के नत्था हैं. ये मीडिया की दुनिया की वो गरीब जनता है जिस से मीडिया का जलाल कायम है किसी भी समाचार को ब्रेक करने का काम इन्हीं मुफ्फसिल पत्रकारों द्वारा किया जाता है.
आमतौर पर स्ट्रिंगर को ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो श्रमजीवी पत्रकार न होकर आस पास की खबरों की सूचना समाचारपत्र या चैनल को देता है. बाकि समय वह अपना काम करता है. पर समाज के हित से जुड़ी बड़ी खबरें सामने लाने में स्ट्रिंगर की बड़ी भूमिका रही है.
ये वो लोग होते हैं जो या तो छोटे समाचार पत्रों में काम करते हैं या भाड़े पर चैनलों को समाचार, कहानी उपलब्ध कराते हैं वो चाहे भूख से होने वाली मौतें हों या किसानों की आत्महत्या की खबर. महानगरों में काम करने वाले पत्रकारों के सामने इनका कोई औचित्य नहीं होता क्योंकि अक्सर इनकी खबरें जमीन से जुड़ी हुई होती हैं जिन पर पर्याप्त शोध और मेहनत की जरूरत होती है.
आजकल के मुहावरे के हिसाब से इनकी खबरें लो प्रोफाइल वाली होती हैं. दरअसल देश के गांवों को मीडिया ने स्ट्रिंगरों के भरोसे छोड़ दिया गया है देश का सारा प्रबुद्ध मीडिया महानगरों में बसता है. मीडिया ऐसी बहुत जगहों पर नहीं पहुँच पा रहा है, जहां पर बहुत सारी रोचक चीजें हो रही हैं. इन सब तक यही स्ट्रिंगर पहुंच पाते हैं. सूखा या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा हो या कोई अपराध इनकी खबर सबसे पहले देने वाले स्ट्रिंगर ही होते हैं ये चैनल या अखबार की रक्त शिराओं जैसे होते हैं.
इनके भरोसे नाग-नागिन और भूत प्रेतों की कहानियां ही करवाई जाती हैं. ऐसी कहानियों के लिए किसी वैचारिक तैयारी और शोध की जरूरत नहीं पड़ती और न ही स्ट्रिंगर को अलग से कोई निर्देश देने की आवश्यकता. बाद में टीआरपी के नाम पर ऐसी हरकतों को जायज ठहराने की कोशिश की जाती है.
देश में सन 2000 का साल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए क्रांति का साल था. 24 घंटे वाले समाचार चैनल एक के बाद एक शुरू हुए. लेकिन उस अनुपात में योग्य पत्रकारों की नियुक्ति न तो की ही गयी और न ही बाजार का अर्थशास्त्र उन्हें इसकी इजाजत देता था. चैनल के पत्रकारों को सेलेब्रिटी स्टेटस मिलने लगा तो बड़े पैमाने पर लोग इस ग्लैमर की तरफ आकर्षित हुए. यहीं से स्ट्रिंगर कथा का आरम्भ हुआ, वे इस धंधे का हिस्सा हैं भी और नहीं भी इसी गफलत में अक्सर वे शोषण का शिकार भी होते हैं.
चैनल की तरफ से उनके प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था होती नहीं, और योग्यता के रूप में उनके पास एक कैमरा होना पर्याप्त है. चैनल के लिए वर्षो काम करने के बाद भी वे अक्सर अनाम रहते हैं. उन्हें हर बार अपनी पहचान बतानी पड़ती है. ब्रेकिंग न्यूज़ की मारामारी में जो सबसे पहले अपने चैनल को दृश्य भेज देता है उसी की जय जय कार होती है.
पत्रकारों के लिए तो सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई हैं जिनसे उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता है. पर स्ट्रिंगर उस दायरे में नहीं आते. इनको होने वाला भुगतान समय पर नहीं होता है. ऐसे में अक्सर इन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप भी लगाया जाता है. इनका हाल भारत के उन किसानों जैसा है जो हमारे लिए अन्न और सब्जियां उगाते हैं लेकिन उनसे बने पकवान खुद नहीं खा पाते हैं.
पीपली लाइव के बहाने ही सही कम से कम स्ट्रिंगरों की समस्या पर बहस तो शुरू हुई. अब वक्त आ चुका है कि स्ट्रिंगरों के पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए. समय समय पर इनके लिए ओरिएंटेशन कोर्स चलाये जाएं. मीडिया में उन्हें सम्मान मिले यह तो खैर जरूरी है ही.
लेखक डा. मुकुल श्रीवास्तव का यह लिखा आज दैनिक हिंदुस्तान में प्रकाशित हुआ है. वहीं से साभार लेकर यहां प्रकाशित कराया गया है.














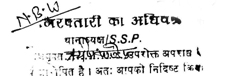
sunil monga
August 22, 2010 at 2:29 pm
श्रीवास्तव जी ,आप ने सही लिखा है स्ट्रिंगर नाम का जीव अपना जीवन खर्च कर के मीडिया का भोजन पैदा कर रहा है लेकिन उस के भोजन का कोई ठिकाना नहीं है ….जाने कौन सी मजबूरी उन से ये काम करा रही है…लेकिन आज तो स्टाफ रिपोर्टर कहलाने वाले पत्रकारों का भी जम कर शोषण हो रहा है …उन्हें ना तो नियुक्ति पत्र दिया जाता है और ना ही सम्मान …. कांट्रेक्ट के जरिये उन्हें बड़ी चालाकी से श्रमजीवी पत्रकारों के दायरे से बाहर कर दिया गया है …. सब से ज्यादा बुरा हाल टीवी चैनलों में है जहाँ काम करा कर पैसा नहीं देने का रिवाज सा चल पड़ा है … ऐसे में प्रबुद्ध स्वाभिमानी लोग पत्रकारिता से दूर होते जा रहें हैं …लगता है एक दिन मीडिया में पत्रकार नहीं सिर्फ चाटुकार ही रह जायें गे ….
rajiv
August 22, 2010 at 3:03 pm
बिलकुल सही यहाँ एक स्ट्रिंगर की रिअल लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताने की कोशिश की गयी है मै भी एक नामी नेशनल चैनल से जुड़ा हुआ हूँ खबरों के लिए जो मारामारी करनी पड़ती है वो तो सब है ही लेकिन कुछ ऐसी बाते भी होती है जो की इस पत्रकारों की भीड़ में कभी कभार हमें गुमनाम कर देती है कहने को तो हम भी पत्रकार है लेकिन सपनो से हकीकत में तब आते है जब कोई ऐसा वाकया हो जाए अभी हाल की ही बात है स्वतंत्रता दिवस का कार्यकर्म था सो मै भी चल पड़ा ये सोचकर की शायद कुछ मिल ही जाये चेनल पर चलने लायक बेग लेकर जैसे ही गेट पर पंहुचा तो सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया
हाँ जी कहा जा रहे है जनाब बेग लेकर ?
जी, मै प्रेस से हु और कवरेज के लिए आया हु
अच्छा, तो अपना पहचान पत्र दिखाइए
जी , वो तो नहीं है
नहीं है तो हम इस बेग के साथ प्रवेश नहीं दे सकते
सो क्या करता इस मुद्दे पर बहस तो कर नहीं सकता था ये भी नहीं बता सकता था की हमारे चेनल वालो ने कोई पहचान पत्र नहीं दिया है
वो तो दूर की बात है एक माइक आई डी के लिए महानगर बैठे अपने बॉस को कितनी बार कह चुके है लेकिन कोई सुनवाई नहीं
मैं वापिस आते हुए बार बार यही सोच रहा था के यदि आज यहाँ ऐसा कुछ मिल जाता जोकि चेनल पर चलने लायक होता तो दुसरे चेनलो पर देख कर तो चेनल वालो के बार बार फोन आने थे तब तो ये नारजगी जाहिर करते भी देर नहीं लगाते
यार तुम कहा थे तुम्हारे शहर से खबर ब्रेक हो रही है ………………………………………
digvijay singh
August 23, 2010 at 4:24 am
mukul ji ne sahi likha hai. media ki duniya ke ye natte puri jindagi uhi gujar dete hai.inke bare main likhne ke niye dhanaywad
vishnu
August 27, 2010 at 12:46 am
नत्था को लेकर अब और मत पकाओ..
ओ यारों छोड़ो जाओ…
खोपड़ी मत खाओ…
जइसे कुर्सी दोनो ओर हत्थे होते हैं,
वइसे ही न्यूज चैनलो में भी कई नत्थे होते हैं..
फिल्मी नत्थे के लिए…अब कितना पकाओगे?
खोपडि़या फट जाएगी क्या पाओगे?
फालतू में मरेंगे दो चार…
होगा लाइव, खोपड़ी फटी चार मरे..
इसीलिए मनुहार है…
बेवजह हत्या मत कराओ…
ओ यारों छोड़ो जाओ…
खोपड़ी मत खाओ,
फिल्मी नत्था का
इस्लेशण..हुआ…विश्लेषण..हुआ…
अब क्या नत्था का ट्रांसलेशन कराओगे?
जरा दिमाग लगाओ..और बताओ…
के नत्था कहां पाया जाता हैं…
क्या सिर्फ पिपली गांव में…
डूबती हुइ नाव में? बाढ़ के चपेटो में
या बंजर पड़े खेतो में..
गंदी सी धोती में…जली हुई रोटी में…
बढ़ी हुई दाढ़ी में…या मिसेज नथिया की फटी हुई साड़ी में?
बूझो और बताओ..ना समझ आए तो सुनकर जाओ…
सच तो ये है…के
बड़ी सी एक बिल्डिंग के…एसी की ठंड़ी में…
कुर्सी पर बैठकर की बोर्ड की डंडी में..
फुटेज, इंजेस्टिंग में..सपनों की डंपींग में
दुधिया से रौशनी के हिडेन सी गर्दिश में…
मर चुके विचारो में..टीआरपी के जुगाड़ो में…
नौकरी बचाने में…बॉसवे को पटाने में…
…जिंदगी गुजार दी…
पत्रकार तो बन ना सके नथ भी उतार दी…
तो फर्क क्या है भाई….
पिपली का नत्था
मरता है..खेत की बुआई में…
दिल्ली के वुडलैंडी नत्थे मरते हैं… छटाई में..
अंतर बस इतना सा…रह गया है यारों…
कि फिल्मी नत्था की कहानी…शुरु हुई आत्म हत्या से
अपुन न्यूज के नत्थों की कहानी कही आत्म हत्या पे बंद न हो…
इसीलिए मनुहार है…के जरा खुद पे तरस खाओ…गफलत से अच्छा है…
कि मिडिया के नत्थों के फ्यूचर का अंदाजा लगाओ
वो नत्था फिल्मी था…उसका इंसाफ फिल्मी होगा…
तुम रिअल नत्थे हो कही..अंजाम फिल्मी ना हो..
तो यारों छोड़ो जाओ…
खोपड़ी मत खाओ…
जइसे कुर्सी दोनो ओर हत्थे होते हैं,
वइसे ही न्यूज चैनलो में भी कई नत्थे होते हैं..