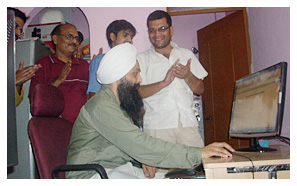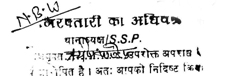आलोक तोमर के आलेख ‘नेट का भी अपना समाज है प्रभाष जी’ के क्रम में प्रभाष जी और उन जैसे तमाम लोगों को, जो नेट की हैसियत नहीं जानते या मानते, को यह बताना वाजिब होगा कि नेट के पाठक बिखरे हुए हैं, पर हैं काफी। यह अजीब बात है कि प्रभाष जी जनसत्ता में तो लिखते हैं पर नेट के पाठकों की संख्या को गंभीर नहीं मानते हैं। यहां मैं जनसत्ता के प्रसार की चर्चा नहीं करूंगा पर बताना चाहूंगा कि इंटरनेट गवरनेंस फोरम के मुताबिक भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 8 करोड़ 10 लाख है। इसके अलावा दुनिया भर में फैले सैकड़ों भारतीय और हिन्दीभाषी नेट पर भारत से संबंधित और भारतीय लेखकों की सामग्री को पढ़ते हैं। इन्हें मिलाकर, इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री को पढ़ने वालों की संख्या अखबारों पत्रिकाओं के मुकाबले कई गुना ज्यादा होगी।
आलोक तोमर के आलेख ‘नेट का भी अपना समाज है प्रभाष जी’ के क्रम में प्रभाष जी और उन जैसे तमाम लोगों को, जो नेट की हैसियत नहीं जानते या मानते, को यह बताना वाजिब होगा कि नेट के पाठक बिखरे हुए हैं, पर हैं काफी। यह अजीब बात है कि प्रभाष जी जनसत्ता में तो लिखते हैं पर नेट के पाठकों की संख्या को गंभीर नहीं मानते हैं। यहां मैं जनसत्ता के प्रसार की चर्चा नहीं करूंगा पर बताना चाहूंगा कि इंटरनेट गवरनेंस फोरम के मुताबिक भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 8 करोड़ 10 लाख है। इसके अलावा दुनिया भर में फैले सैकड़ों भारतीय और हिन्दीभाषी नेट पर भारत से संबंधित और भारतीय लेखकों की सामग्री को पढ़ते हैं। इन्हें मिलाकर, इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री को पढ़ने वालों की संख्या अखबारों पत्रिकाओं के मुकाबले कई गुना ज्यादा होगी।
इसीलिए, तमाम सक्षम और संपन्न (जनसत्ता शायद इन दोनों में नहीं है) पत्र-पत्रिकाएं नेट पर भी मौजूद हैं या अपनी उपस्थिति बना रही हैं। वैसे भी, इंटरनेट पर लिखे या छपे को पढ़ना काफी आसान है और इसे कभी भी, कहीं भी पढ़ा जा सकता है और किसी के लिखे को कभी भी, कहीं से भी ढूंढ़ा जा सकता है। मिनटों में हजारों लोगों से कहा जा सकता है कि फलां लेख को पढ़कर प्रतिक्रिया दें और प्रतिक्रियाएं प्राप्त भी की जा सकती हैं। 1987 में जनसत्ता में उपसंपादकी करने दिल्ली आने के बाद पता चला कि नौकरी सिर्फ छह घंटे की है और वह भी शाम छह से 12 या रात आठ से दो की। एक साल के लिए प्रशिक्षु रखा गया था और पहले ही बता दिया गया था कि जो पैसे मिलेंगे उतने में दिल्ली में रहना मुश्किल है। उस समय तो पत्रकारिता का भूत सवार था, सो कोई चिन्ता नहीं हुई। बाद में लगा कि लिखने-पढ़ने के लिए काफी समय है। सोचा कि कुछ और काम किया जाए जिससे समय तो कटे ही, पैसे भी बनें। अखबार की नौकरी के साथ सबसे अच्छा काम दूसरे अखबारों में लिखना ही हो सकता था (मेरी हैसियत और योग्यता के अनुसार)।
दिल्ली में रहकर देश के छोटे शहरों से निकलने वाले सैकड़ों हजारों पत्र-पत्रिकाओं के लिए बहुत ही आसानी से बहुत कुछ लिखा जा सकता है। लोग लिखते ही हैं और छपता भी है। पर समस्या यह थी (और अब भी है) कि नए लेखकों को हिन्दी की ज्यादातर पत्र-पत्रिकाएं पारिश्रमिक नहीं देती हैं या जो देती हैं वह न के बराबर होता है। अखबार में आलेख छप गया इसकी सूचना देने की भी कोई पक्की व्यवस्था उस समय तो नहीं ही थी। अब टिकट लगा, पता लिखा लिफाफा भेजने के लिए तो नहीं कहा जाता लेकिन आमतौर पर ई-मेल से यह भी नहीं बताया जाता कि रचना प्राप्त हो गई है और प्रकाशन तारीख की सूचना दी जाएगी। इसमें लगने वाला पैसा और श्रम नगण्य है फिर भी आम लेखकों को ऐसी कोई सूचना देने का रिवाज मेरी जानकारी में नहीं है।
ऐसे में मुझे अखबारों में लिखने में कोई मजा नहीं आया और मैंने तमाम लोगों के समझाने और हतोत्साहित करने के बावजूद खाली समय में अनुवाद करने का काम चुना जो अब मेरा मुख्य व्यवसाय बन गया है। अखबारों में लिखना बहुत कम होता है क्योंकि आलेख प्रकाशित हुआ या नहीं इसका ट्रैक रखना लगभग असंभव है। जिसे इसकी परवाह या जरूरत नहीं है उसकी बात अलग है। जो लोग बहुत ज्यादा लिखते हैं वे इसके लिए शायद कोई व्यवस्था भी कर सकें। लेकिन कभी-कभी लिखने वालों के लिए यह बहुत मुश्किल है। दूसरी ओर, किस अखबार को भेजा गया कौन सा आलेख छप गया – यह जानकर खुश होने से मैं अब तक उबर नहीं पाया हूं। ऐसे में किसी वेबसाइट पर लिखने का सबसे बड़ा लाभ तो यह है प्रकाशित (अपलोड) हुआ या नहीं यह पता करने में कोई दिक्कत नहीं है और ज्यादातर साइटों से मेल भी आ जाता है। प्रभाष जी के साथ भले ही ऐसी कोई समस्या न हो लेकिन नेट पर होने का मजा ही अलग है। इसका वर्णन लिख कर नहीं किया जा सकता है, इसे महसूस ही किया जा सकता है।
नेट का अपना समाज है – इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके पाठकों में वे भी है जो अखबार और पत्र-पत्रिकाएं भी पढ़ते हैं। इसलिए, अगर आप अखबारों में छपे अपने आलेख को नेट पर भी अपलोड कर दें तो उसके पाठक बढ़ेंगे ही – घटेंगे नहीं। जनसत्ता की नौकरी और फिर जनसत्ता पढ़ना छोड़ने के बाद भी प्रभाष जी के कॉलम कागद कारे को पढ़ने की इच्छा रहती है। मानना पड़ेगा कि कागद कारे पढ़कर अक्सर मजा आता है। नेट पर जहां कहीं, जब कभी मिलता है पढ़ लेता हूं पर इसके लिए जनसत्ता खरीदने लगूं (इतवार को ही) यह संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरा भी प्रभाष जी से विनम्र आग्रह है कि वे इंटरनेट की दुनिया में पधारें और अपना यह कॉलम किसी वेबसाइट को भी दें। यह भड़ास4मीडिया, आलोकतोमर डॉट कॉम, डेटलाइन इंडिया या प्रभाषजोशी डॉट कॉम कुछ भी हो सकता है।
लेखक संजय कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं. पत्रकारिता को बाय-बाय बोलने के बाद वे इन दिनों अनुवाद का काम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। उनसे संपर्क [email protected] या 9810143426 के जरिए कर सकते हैं.