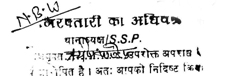सिद्धेश्वर सिंह
सूत्र वाक्यों की उदात्तता पर शंका इसलिए भी है सूत्रकारों तथा उन्हें बरतने के कार्य व्यापार में लगे देहधारियों के जीवन – जगत का यथार्थ अब कोई जादुई बिम्ब नहीं रह गया है। आज हर अभिव्यक्ति चाक्षुष है – दृश्य और श्रव्य की निरन्तरता में घटित होती हुई। न चाहते भी हरेक दृश्य को देखना है और हर आवाज को सुनना है, यह जानते – बूझते हुए कि निरर्थकता को निरर्थक मानना ही सार्थक होने की जिद जैसी कोई चीज है जिसका होना सार्वजनिक संसार में अक्सर द्युतिमान करता दीखता है किन्तु निज के एकांत आईने में दैन्य व दारिद्र्य की छवि ही दिखलाता है।
मैं यह सबकुछ अनिल यादव की कहानी ‘क्योंकि नगरवधुयें अख़बार नहीं पढ़तीं‘ के सिलसिले में कह रहा हूँ जिसमें सतही तौर पर तो वर्णनात्मकता का प्राधान्य है हिन्दी के पुराने खेवे के कथाकारों के यहाँ आम बात थी और हिन्दी कथा साहित्य के विचार व शिल्प की सरिता में ढेर सारा पानी बह जाने के बाद भी अब तक कारगर औज़ार बनी हुई है। कहानीकार ने इस औज़ार की गर्द व जंग को खरोंच – पोंछकर जिस तरीके से इस्तेमाल किया है व मात्र वर्णनात्मकता नहीं वरन आज की शब्दावली में कहें तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का एक अच्छा और उत्कॄष्ट उदाहरण है। इस कहानी का कथातत्व या कथानक एक ऐसी दुनिया है जो हमारे सामने रोज बनती है। इस दुनिया में तात्कालिकता जल्दबाजी का पर्याय नहीं है और न ही सफलता कोई तिरस्करणीय कर्म। यहाँ सब कुछ वह और वैसा ही है जैसा उसे होना है , हो जाना है। यह वर्तमान का विधान है -अतीत और आगत को मुँह बिराता, ठेंगा दिखाता हुआ। यह सुखद है और संतोष का विषय भी कि एक युवा कथाकार वर्तमान के इस वितान को उसी कालखंड में, उसी जमीन पर, उसी भाषा में और बहुत सपाट होकर करें तो उसी काशी में रच रहा है जहाँ रहते हुए धूमिल ने ‘वसन्त’ शीर्षक कविता की अंतिम पंक्तियों कहा था कि –
सौन्दय में स्वाद का मेल
जब नहीं मिलता
कुत्ते महुवे के फूल पर
मूतते हैं।
‘क्योंकि नगर वधुयें अख़बार नहीं पढ़ती’ में पात्र हैं, घटनायें हैं, कथानक का आरम्भ, उत्थान, व अवसान है किन्तु कोई चरमोत्कर्ष नहीं। यहाँ सब कुछ चीन्हा हुआ है। नया कुछ भी नहीं। न कोई नया पात्र , न कोई नई घटना। यह उस भयावह समय की कथा है, उस उर्वर प्रदेश की भी, जहाँ नया कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ नया चाहने की कोई नई उम्मीद भी नहीं। जहाँ नया न होने की निरर्थकता से उपजती हुई कोई नई ऊब व निराशा भी नहीं जिसके बरक्स कुछ कहने के लिए नई भाषा के नए तेवर, नए मुहावरों के ईजाद की बात की जाय। यही वजह हो सकती है कथाकार ने वर्णनात्मकता को बरतने में किंचित नयापन भले ही दिखाया हो लेकिन कहानी को कहने की शैली में कहा है। यह एक ऐसी कहानी है जिसका पूर्वकथन तथा पूर्वापरकथन कहीं कोई कोई रहस्य नहीं रचता। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें हिन्दी कहानी के कलेवर में लम्बे समय  से इस्तेमाल की जाने वाली चेख़वियन शैली वाली पूँछ में छिपा डंक मार कर आश्चर्य से भर नहीं देती। हिन्दी कहानी के नए – पुराने इतिहास और आलोचना की किताबों बताए गए सूत्रवाक्यों का सायास नकार इस कहानी में हो यह कहना सही नहीं होगा। इसमें वे सब हैं लेकिन वैसे नहीं जैसे कि वे होते बताए जाते रहे हैं, कथाकार का यह आग्रह भी नहीं जान पड़ता कि उन्हें ऐसा होना चाहिए। कथाकार को लगता है कि वे अब ऐसे हो गए हैं तमाम अकादेमिक और आलोचकीय मेड़ों और बाड़ों के बावजूद।
से इस्तेमाल की जाने वाली चेख़वियन शैली वाली पूँछ में छिपा डंक मार कर आश्चर्य से भर नहीं देती। हिन्दी कहानी के नए – पुराने इतिहास और आलोचना की किताबों बताए गए सूत्रवाक्यों का सायास नकार इस कहानी में हो यह कहना सही नहीं होगा। इसमें वे सब हैं लेकिन वैसे नहीं जैसे कि वे होते बताए जाते रहे हैं, कथाकार का यह आग्रह भी नहीं जान पड़ता कि उन्हें ऐसा होना चाहिए। कथाकार को लगता है कि वे अब ऐसे हो गए हैं तमाम अकादेमिक और आलोचकीय मेड़ों और बाड़ों के बावजूद।
किसी कहानी से यह माँग करना करना कि उसमें कोई याद रह जाने योग्य पात्र, याद रह जाने योग्य घटना और चकित कर देने योग्य शिल्प हो तो व संभवत: कोई कथा जैसी चीज हो जाय तो जाय हमारे समय व समाज के उस हिस्से की कहानी नहीं हो सकती जिसे हम सबने मिलजुल कर एक ‘स्टोरी’ में बदल दिया है और उसे रात के अँधेरे में छपकर सुबह का अख़बार बन जाना है, जिसे मिठास का भ्रम बनए रखने वाली चाय के साथ बाँचना है, यह जानते हुए कि इसमें नया कुछ भी नहीं है। हिन्दी कहा्नी का आज जो भी सृजनात्मक माहौल है उसमें ‘क्योंकि नगरवधुयें अख़बार नहीं पढ़तीं‘ एक अलग रचना के रूप में दिखाई देती है। यह अपने लम्बे कलेवर में खुद को पढ़वा ले जाने की क्षमता रखती है और यह कोई कम महत्वपूर्ण बात नहीं है।
‘क्योंकि नगरवधुयें अख़बार नहीं पढ़ती’ के बारे में मुझ जैसे एक सामान्य पाठक को बाकी तमाम पाठको के साथ यह अनुभव साझा करते हुए कहना है कि- जरा सोचिए, अगर अख़बार पढ़ते हुए सचमुच का अख़बार लगे और कहानी पढ़ते हुए सचमुच की कहानी तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अख़बार इस कहानी की काया में है और कहानी इसकी आत्मा में । हाँ , काया के बारे में कोई भ्रम नहीं किन्तु अगर आत्मा जैसी चीज होती है अथवा होनी चाहिए तो ..
ख़ैर, युवा कथाकार अनिल यादव को एक उम्दा कहानी के लिए बधाई !
हिन्दी के कवि, अनुवादक और आलोचक सिद्धेश्वर सिह उत्तराखण्ड के खटीमा नगर में राजकीय महाविद्यालय में हिन्दी पढ़ाते हैं. नैनीताल के डी एस बी कैम्पस से हिन्दी में महत्वपूर्ण शोध कर चुके सिद्धेश्वर “कर्मनाशा” नाम का ब्लाग भी संचालित करते हैं. उनका एक कविता संग्रह और अनुवाद की दो किताबें इस साल जल्द छप कर आने को हैं.