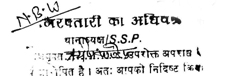![]() : होलटाईमरी की उलटबासियां : शुरुआत पिछली कड़ी पर आई अनुराग जी (स्मार्ट इंडियन) की एक प्रतिक्रिया से करते हैं. उनका कहना है- ”लेख से ऐसा प्रभाव बन रहा है जैसे आपके संगठन के अलावा बाकी सब हथियारबंद गुंडों के ही गैंग थे. क्या यह सच है? यदि ऐसा है तो तब से अब तक इन साम्यवादी संगठनों द्वारा हिंसा और अनाचार में उन गुंडों को पीछे छोड़ देने का क्रान्तिकाल कब और कैसे आया – कुछ प्रकाश डालेंगे कभी आगे की कड़ियों में?”
: होलटाईमरी की उलटबासियां : शुरुआत पिछली कड़ी पर आई अनुराग जी (स्मार्ट इंडियन) की एक प्रतिक्रिया से करते हैं. उनका कहना है- ”लेख से ऐसा प्रभाव बन रहा है जैसे आपके संगठन के अलावा बाकी सब हथियारबंद गुंडों के ही गैंग थे. क्या यह सच है? यदि ऐसा है तो तब से अब तक इन साम्यवादी संगठनों द्वारा हिंसा और अनाचार में उन गुंडों को पीछे छोड़ देने का क्रान्तिकाल कब और कैसे आया – कुछ प्रकाश डालेंगे कभी आगे की कड़ियों में?”
खुद लिखने वाला होने के चलते थोड़ा-बहुत अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की गुंजाइश तो बची ही रह जाती है, लेकिन संगठन को लेकर इस तरह का प्रभाव क्यों बन रहा है, मेरे लिए समझना मुश्कल है। कुछ कड़ियों पहले मैं बता चुका हूं कि आरा शहर में बतौर पत्रकार मेरी एंट्री एक गुंडे का इंटरव्यू लेने के साथ हुई थी, जिसका मकसद अपनी पार्टी के पक्ष में उसकी जाति का समर्थन बनाना था। इसी शख्सियत के बारे में कुछ और बातें आपको इस कड़ी में भी पढ़ने को मिलेंगी। कोई संगठन जिस समाज में काम करता है, उसकी बुराइयों से वह पूरी तरह बच नहीं सकता। कभी-कभी ये बुराइयां संगठन पर कुछ ज्यादा ही हावी हो जाती हैं और उसका चरित्र बदल देती हैं।
आरा में बतौर राजनीतिक कार्यकर्ता मैं काम करने पहुंचा तो लग रहा था कि हमारा संगठन भी वहां ठीक ऐसे ही मोड़ पर खड़ा था। लेकिन आप चाहे कोई संगठन हों या व्यक्ति, आपकी पहचान इस बात से नहीं बनती कि आप कभी पतित हुए या नहीं, बुराई से कभी आपका साबका पड़ा या नहीं। यह बनती है इस बात से कि आपमें गिर कर उठने का माद्दा है या नहीं। बता दूं कि मैं यहां समाज  सुधार या संगठन सुधार करने नहीं, क्रांतिकारी राजनीति करने आया था। पता नहीं क्यों अब यह सब कहते हुए दिल दुखता है और मिर्जा गालिब का एक शेर याद आता है- घर में था क्या जो तेरा ग़म उसे ग़ारत करता, थी जो इक हसरत-ए-तामीर सो वो आज भी है।
सुधार या संगठन सुधार करने नहीं, क्रांतिकारी राजनीति करने आया था। पता नहीं क्यों अब यह सब कहते हुए दिल दुखता है और मिर्जा गालिब का एक शेर याद आता है- घर में था क्या जो तेरा ग़म उसे ग़ारत करता, थी जो इक हसरत-ए-तामीर सो वो आज भी है।
बहरहाल, मेरे सामने सवाल था, कहां से शुरू करें। सबसे पहले तो यह कि शेल्टर कहां रखा जाए। रहा कहां जाए। आरा में पार्टी के दो-तीन जाने-पहचाने शेल्टर थे जो भूमिगत नेताओं के काम आते थे। मुझे यहां खुले तौर पर काम करना था, लिहाजा इन शेल्टरों पर जाकर इन्हें एक्सपोज करना ठीक नहीं था। दूसरे, पार्टी के बाकी नेता आरा शहर में हफ्ते या महीने में कभी एक-दो बार आते थे जबकि मुझे यहां लगातार रहना था। तीसरे, किसी मध्यवर्गीय ठिकाने पर डेरा डालकर मुझे रहना ही नहीं था, क्योंकि यही करना होता तो पटना या दिल्ली के सुकून में रहते हुए जनमत का काम करना ही क्या बुरा था।
ऐसे में स्थायी ठिकाने जैसी बात को तो अजेंडे से ही हटा देना पड़ा। शहर में भरोसे की तीन-चार जगहें ऐसी थीं, जहां देर-सबेर अचानक पहुंचने पर खाना और सोने की जगह मिल सकती थी। तब हर खाने में स्वाद आता था और कहीं भी लेटने पर नींद आ जाती थी, लिहाजा परेशानी की तो कहीं कोई बात ही नहीं थी। ठहराने वालों को भी यहां-वहां के किस्से, कुछ हंसी-मजाक और थोड़ी-बहुत बौद्धिक गप्पें सुनने को मिल जाती थीं लिहाजा उनके लिए भी सौदा ज्यादा बुरा नहीं था। शुरू में एक-दो महीने ऐसे ही चला, फिर धीरे-धीरे नए लोग मिलने लगे, नई जगहें बनने लगीं। एक समय ऐसा भी आया, जब किसी मोहल्ले में दोबारा पहुंचने का मौका काफी बाद आता था और लोग नाराज होकर शिकायत करते थे कि लगता है साथी को अब बढ़िया खाने और पंखा चला कर सोने का शौक लग गया है।
शहर में पार्टी का काम बिखरा-बिखरा सा था। 1970 के दशक से ही जहां-तहां कुछ संपर्क थे और थोड़े-थोड़े समय के लिए सक्रिय रही असंगठित मजदूरों की कुछ छोटी-छोटी ट्रेड यूनियनें भी थीं। बक्सा मजदूर यूनियन, दर्जी यूनियन, रिक्शा-ठेला चालक संघ, फुटपाथ विक्रेता संघ वगैरह। इन सभी के साथ विडंबना यह थी कि जैसे ही कहीं मजदूरों की लड़ाई उग्र रूप लेती थी, मालिक मजदूरों को काम से हटा देते थे, या पासा पलटते देख अपना धंधा ही बंद कर देते थे। नतीजा यह था कि दर्जी यूनियन के जुझारू कार्यकर्ता सैलून पर काम करते नजर आते थे और बक्सा यूनियन के सबसे बड़े नेता अबरपुल चौराहे पर करछुल में अंडे का पोच बनाकर बेचते थे।
यह संयोग था कि इनमें काफी बड़ी संख्या मुसलमान मजदूरों की थी, जिनमें से कुछ आईपीएफ के उदय के साथ ही मजदूर से राजनीतिक कार्यकर्ता बनने की ओर बढ़ गए थे। पारंपरिक सामंती वर्चस्व वाले इस शहर में कुछ यूनियनें दबंगों की रंगदारी से बचकर अपनी जीविका चलाने के लिए भी खड़ी हुई थीं। जैसे, रिक्शा, ठेला चलाने वाले या फुटपाथ पर कंघी-शीशा बेचने वालों को पता था कि दबंगों के सामने खड़े होने का दम यहां सिर्फ सीपीआईएमएल के पास है, इसलिए वे हर दुख-सुख में पार्टी के साथ रहते थे। पल्लेदारी वगैरह करने वाले बहुत सारे असंगठित मजदूर भी पार्टी के पुख्ता आधार में शामिल थे।
ठीकठाक दुकानें चलाने वाले या नौकरी-चाकरी करने वाले कुछ लोग पिछड़ा वर्ग की चेतना के तहत पार्टी को चंदा और वोट देते थे। इनके अलावा पार्टी को शहर के लगभग समूचे दलित समुदाय और सांप्रदायिक माहौल के सताए हुए गरीब मुसलमानों का भी समर्थन प्राप्त था, भले ही इसकी सोच और विचारधारा से उन्हें कोई खास मतलब न रहा हो। लेकिन इस सबके बावजूद, एक एमपी एलेक्शन जीत लेने और एमएलए के चुनाव में लगातार सेकंड रहने के बावजूद आरा शहर में संगठन का कोई व्यवस्थित ढांचा नहीं था। एक सांस्कृतिक टीम थी। कुछ अच्छे कार्यकर्ता थे जो किसी कार्यक्रम के लिए दिन-रात काम कर सकते थे, लेकिन घर से निकल कर काम करने, होलटाइमर बनने की मानसिकता किसी की नहीं थी।
जहां तक सवाल शहर में पार्टी ढांचे का है तो इसके साथ यहां कुछ अजीब किस्से भी जुड़े थे। दोहरा दें कि भूमिगत पार्टी सीपीआईएमएल उस समय अपने ज्यादातर राजनीतिक काम इंडियन पीपुल्स फ्रंट (आईपीएफ) के जरिए करती थी, जिसका ढांचा और कामकाज हर मायने में किसी मुख्यधारा की पार्टी जैसा था। पता चला कि आरा शहर में आईपीएफ के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शराब के दो ठेकों के मालिक हैं और पार्टी का पिछला जुझारू संघर्ष एक गुंडे के हमले से उनकी दुकान बचाने के लिए ही हुआ था। यह गुंडा और कोई नहीं, वही विश्वनाथ यादव था, जिसका एक हास्यास्पद सा इंटरव्यू मैंने करीब डेढ़ साल पहले किया था।
राजेंद्र जी का एक ठेका शहर के मेन मार्केट में था, जिस पर विश्वनाथ की नजर काफी समय से गड़ी थी। ठेके पर उसके आदमियों का हमला शराब खरीदने के सिलसिले में हुआ था लेकिन उसका एक पहलू दुकान पर कब्जा करने या रंगदारी टैक्स वसूलने से भी जुड़ा था। शहर के यादवों और पिछड़ों में विश्वनाथ यादव की प्रतिष्ठा इस बात के लिए थी कि अपने गैंग के जरिए उसने आरा शहर पर राजपूतों का दबदबा तोड़ दिया था, जबकि राजेंद्र प्रसाद तो आईपीएफ के अध्यक्ष ही थे। सीपीआईएमएल का संपर्क किसी न किसी रूप में दोनों ही के साथ था लिहाजा शुरुआती मारपीट के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया था। लेकिन इस पूरे प्रकरण से शहर में पार्टी की स्थिति के बारे में एक अंदाजा लगाया जा सकता था।
राजेंद्र प्रसाद की दुकान पर काम करने वाले पार्टी के एक साथी का किराये का कमरा दीनाजी का शेल्टर हुआ करता था। उनकी खासियत यह थी कि जीवन भर शराब की दुकान पर काम करने के बावजूद उन्होंने कभी इसकी एक बूंद भी नहीं चखी थी। इसी तरह विश्वनाथ यादव के कब्जाए बंगले में एक कमरा किराए पर लेकर रहने वाले एक मास्टर साहब पार्टी के बहुत पुराने समर्थक थे और बाद में वे मेरे भी बहुत गहरे मित्र बने। दारू का ठेका चलाने वाले या बाकायदा एक गुंडा गिरोह के संचालक का खुद को क्रांतिकारी कहने वाली एक पार्टी से भला क्या लेना-देना हो सकता था। लेकिन जो था सो था। हम हकीकत में अपने फैसले चुन सकते हैं। हकीकत तो नहीं चुन सकते।
शहर में पार्टी के दो-चार गिने-चुने ही मध्यवर्गीय संपर्क थे, जिनमें एक तो शराब की ठेकेदारी करने वाले ये ही सज्जन थे। पार्टी से उनके जुड़ाव का आधार स्पष्ट था। वे कहार बिरादरी से आते थे, जो बिहार की एक अतिपिछड़ी जाति है। इस पृष्ठभूमि से मध्य या उच्च मध्यवर्ग में पहुंचा कोई व्यक्ति अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए और भला कहां जा सकता था। कांग्रेस और बीजेपी से लेकर जनता दल तक ज्यादातर ताकतवर और प्रायः ऊंची जातियों से आए दबंगों का वर्चस्व था, लिहाजा उनका स्वाभाविक जुड़ाव आईपीएफ से ही बन सकता था। अपनी समझ से वे ऐसा कोई काम भी नहीं करते थे जिससे पार्टी को कोई नुकसान हो। लेकिन जिस पार्टी ढांचे के शीर्ष पर शराब के ठेके चलाने वाला व्यक्ति बैठा हो, उसमें किसी पल्लेदार, किसी दर्जी, किसी रिक्शाचालक, नालियों की सफाई करने वाले, सुर्ती बेचने वाले या बक्सा बनाने वाले की पहलकदमी खुलने की उम्मीद भला कैसे की जा सकती थी।
: जड़ों को सींचने की कवायद : जड़ सींचो, फल-फूल सब उसी से मिलेगा। बेगूसराय के एक मरणासन्न बुजुर्ग दलित कम्युनिस्ट की यह बात राजीव के पिता जनार्दन चाचा से होती हुई मुझ तक पहुंची थी। आरा में अपने कामकाज के सूत्रवाक्य के रूप में मैंने इसे ही अपनाने की कोशिश की। आईपीएफ और जनसंगठनों को भूल कर पार्टी को मजबूत बनाने में जुटा। मध्यवर्ग की चिंता छोड़ कर मजदूर यूनियनों के पुनर्गठन की कोशिश की। रिक्शा-ठेला यूनियन से इसकी शुरुआत हुई। बारिश के मौसम में रिक्शाचालकों के लिए स्थायी शेल्टर बनाने की मांग पर एक बड़ा प्रदर्शन भी हुआ। हमारे गोपालजी रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष थे। रिक्शा चलाना अब छोड़ चुके थे लेकिन शहर के रिक्शाचालकों को उनमें पूरा भरोसा था।
नारी-पुरुष संबंधों और कई दूसरे मामलों भी गोपालजी से ज्यादा स्वस्थ्य मूल्यों वाला व्यक्ति मैंने नहीं देखा, लेकिन इस पर बातें बाद में। डिफंक्ट सी ही सही, लेकिन पार्टी की एक पांच सदस्यीय लीडिंग टीम शहर में पहले से मौजूद थी। सभी के जिम्मे इलाके बांट कर पहला कार्यक्रम यह लिया गया कि हर इलाके की मुख्य समस्याएं चुनी जाएं, उनमें से किसी एक पर फोकस किया जाए और उसे हल कराने की हद तक संघर्ष किया जाए। बरसात का मौसम करीब आ रहा था। जिन-जिन मोहल्लों में पार्टी का प्रभाव था, उनमें नागरिक मीटिंगें बुलाई गईं, आम सभा, धरना, प्रदर्शन वगैरह शुरू 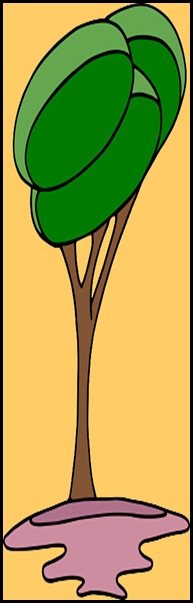 हुए। पता चला कि यह सब पहले भी होता रहा है। औपचारिक कार्यक्रम, जो किसी नतीजे तक नहीं पहुंचते। इसी बीच आरा सेंट्रल जेल में एक घटना घट गई।
हुए। पता चला कि यह सब पहले भी होता रहा है। औपचारिक कार्यक्रम, जो किसी नतीजे तक नहीं पहुंचते। इसी बीच आरा सेंट्रल जेल में एक घटना घट गई।
पिछले ढाई सालों से जेल काट रहे और हाल ही में बक्सर सेंट्रल जेल से ट्रांसफर होकर आए आईपीएफ के भोजपुर जिला अध्यक्ष सुदामा प्रसाद के साथ विरोधी खेमे के कुछ कैदियों ने मारपीट कर दी। जेल के भीतर सुदामा प्रसाद कई समर्थकों के साथ अनशन पर बैठे और हम लोगों ने जेल के बाहर सड़क जाम करके उग्र प्रदर्शन का फैसला किया। यह शहर की मुख्य सड़क थी। थोड़ी ही देर मे पुलिस आ गई। मैं खुद छात्र राजनीति के दिनों की याद करते हुए भाषण दे रहा था, तब तक सामने लाठीचार्ज शुरू हो गया। देखते-देखते हालत यह हुई कि मेरे इर्दगिर्द सिर्फ तीन-चार साथी रह गए थे और सामने पूरा मैदान साफ था। ये तीन-चार लोग भी शायद इसलिए वहां रहे हों क्योंकि इन्होंने तुरंत ही अपने भाषण पूरे किए थे।
पारंपरिक फॉर्मेशन- भाषण देने वाले एक तरफ, भाषण सुनने वाले दूसरी तरफ। हूल-पैंतरे के सिवाय और कोई चारा नहीं था। वहीं खड़े-खड़े मैंने शहर कोतवाल, डीवाईएसपी को माइक से ललकारा कि आप मारपीट करना चाहें, कर लें लेकिन यह मामला बहुत दूर तक जाएगा। शायद पुलिस अफसर को लगा कि लोग वैसे ही भाग रहे हैं, लिहाजा जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग का कोई फायदा नहीं है। या शायद उसे यह लगा हो कि चश्मा लगाए कुछ पढ़ा-लिखा सा लगता महीन-महीन बातों वाला भाषण ठेल रहा यह आदमी लोकल तो नहीं है। लालू यादव का टाइम है, कहीं ऐसा न हो कि यह कुछ सोर्स रुतबे वाला हो और बाद में खामखा कोई झंझट पैदा हो जाए। मेरी बात से एक शब्द पकड़कर उसे चुभलाते हुए उसने कहा कि संवेदनशीलता और संवेदनशून्यता का मतलब हम भी समझते हैं, यह जेल के भीतर का मामला है, जेल प्रशासन से बात कीजिए, सड़क पर बवाल क्यों काट रहे हैं। लब्बोलुआब यह कि प्रशासन को चेतावनी वगैरह देने की औपचारिकता पूरी करके वह कार्यक्रम निपटा दिया गया।
इसके अगले दिन पार्टी लीडिंग टीम की एक्सटेंडेड मीटिंग बुलाई गई और सवाल रखा गया कि यही भोजपुर के क्रांतिकारी लोग हैं जो एक भी लाठी पड़ने से पहले ही भाग खड़े होते हैं। फिर सबके किस्से एक-एक कर सामने आने शुरू हुए। कौन भागा और कौन खड़ा रहा। पता चला कि मीटिंगों में सबसे ज्यादा जला दो मिटा दो की बात करने वाले कॉमरेड बिरजू पुलिस की गाड़ी आते ही खिसक कर एक केले वाले के पास चले गए और कुछ ऐसी मुद्रा में ठेले के करीब खड़े हो गए जैसे ठेला उन्हीं का हो और बेचने वाला किराये पर दुकानदारी कर रहा हो। तय पाया गया कि मीटिंग में नेता बने रहने का कोई मतलब नहीं है। नेता वह जो लड़ाई में आगे चले। जो किसी के कहने पर या किसी को देखकर नहीं, अपने मन की ताकत से युद्ध में डटा रहे। जो जिम्मेदारी ले और जिस पर भरोसा किया जा सके। हमीं को भरोसा नहीं रहेगा तो जनता क्या भरोसा करेगी। अपनी गलतियों का विश्लेषण किया गया।
जिन लोगों को ध्रुव की भूमिका निभानी थी, उन्हें टकराव के हर मौके पर बिखर कर रहना था और आसपास के लोगों को इत्मीनान दिलाना था। लेकिन जब लड़ाई शुरू हो जाए तो बिखरने के बजाय सबको करीब आना था, एक-दूसरे को बचाना था। बीस लोग, दस लोग, पांच लोग ही सही, चट्टान की तरह, केंद्र की तरह एकजुट रहना था। ऐसा एक छोटा सा केंद्र पहली ही लड़ाई में सामने आ गया था, इस उपलब्धि को भी रेखांकित किया गया। नेतृत्व के स्तर पर पाया गया कि हमारी प्लानिंग कमजोर थी। इलाके की बेहतर समझ होनी चाहिए थी। जिम्मेदारियां ज्यादा ठोस होनी चाहिए थी। कहां तक जाना है, यह तय होना चाहिए था।
इस आकस्मिक संघर्ष से मोहल्लों में सफाई और जलनिकास के लिए जारी आंदोलन को काफी बल मिला। चुनाव में हार से सुस्त पड़ी हमारी गीत-नाटक इकाई युवानीति में भी अचानक जान पड़ गई। कार्यकर्ताओं, समर्थकों को लगने लगा कि चुनाव में जीत-हार तो आनी-जानी चीज है। असल चीज है अपनी समस्याओं पर आंदोलन और संघर्ष, जिसकी धुरी के रूप में सीपीआईएमएल उनके साथ खड़ी है। आंदोलन को लेकर अपनी दूसरी मीटिंग में हम लोगों ने यह भी तय किया कि लोगों को अपनी एकजुटता और सक्रियता के छोटे-मोटे फायदे भी मिलने चाहिए। सिर्फ संघर्ष के लिए संघर्ष में उन्हें कोरी नेतागिरी की बू आती है। इसलिए जितने काम जनता की पहल से हो सकते हैं, उतने तत्काल कर देने हैं और जिनके लिए म्युनिस्पालिटी या सरकार की मदद की जरूरत है, उनके लिए लड़ाई जारी रखेंगे। सवाल था, जनता काम करने के लिए कैसे आगे आएगी। आएगी न, हम आएंगे तो साथ-साथ और लोग भी आएंगे। इसी क्रम में कुछ नए समर्थक और हमदर्द भी मिलेंगे। हम लोग कार्यकर्ता हैं। शर्म किस बात की। खुद आगे बढ़कर रास्ते ठीक करेंगे, जितनी भी आसानी से हो सकती हैं, उतनी नालियां दुरुस्त कर देंगे।
करीब महीने भर चले इस आंदोलन का जादुई असर हुआ। शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों में चुनाव के दौरान हमारे और जनता दल के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ टकराव की नौबत आ गई थी। बारिश में होने वाली बदहाली के खिलाफ पार्टी की जमीनी पहल से दूसरे पक्ष के शुद्ध नेताई करने वाले लोग अलग-थलग पड़ गए। इसी दौरान हमने पार्टी की पहली जीबीएम (जनरल बॉडी मीटिंग) की, जिसे मैं संगठन से जुड़े अपने प्रयोगों में सबसे अच्छा और सबसे काम का मानता हूं। पार्टी के सभी स्थायी और उम्मीदवार सदस्यों को इसमें आमंत्रित किया गया। अजेंडा कामकाज की समीक्षा, आय-व्यय का लेखा-जोखा और जिसको जो भी जी में आए, वह सब। एक स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर के इतवार के दिन उसके एक बड़े क्लासरूम में यह मीटिंग हुई। लीडिंग टीम की तरफ से एक साथी ने पिछले तीन महीनों के कामकाज और चंदे-चुटकी पर एक छोटी सी रिपोर्ट रखी।
आधे घंटे की एक पॉलिटिकल रिपोर्ट मैंने रखी, जिसमें रूस में जारी उथल-पुथल, आर्थिक उदारीकरण को लेकर गुपचुप जारी कोशिशों और बिहार की सियासी हलचलों को समेटा गया था। फिर सबसे एक-एक दो-दो रुपये लेकर चाय मंगवा ली गई। असल चीज इसके बाद हुई। लोगों ने अपने इलाके से लेकर घर-बार तक के बारे में बताना शुरू किया। दो रुपये की एक नोटबुक तब मैं हमेशा अपने पास रखता था। वह पूरी की पूरी मिनट्स से भर गई। ब्यौरे और ब्यौरे। रोजी-रोजगार, काम-धंधे से लेकर मियां-बीबी के झगड़ों तक। इसी दौरान पता नहीं क्या खुराफात सूझी, मैंने कहा, मीटिंग में महिलाएं नहीं हैं, क्यों नहीं हैं। हम लोग कम्युनिस्ट हैं लेकिन अपने जीवन में बाकी सबसे अलग कैसे हैं। जिंदगी की लड़ाई से बड़ी कोई लड़ाई नहीं- इसके दोनों पक्ष पता चलने चाहिए। अगली मीटिंग परिवार में स्त्री-पुरुष संबंधों पर रखी जाएगी। उसमें जो लोग भी अपनी पत्नी के साथ आ सकें, आएं, ताकि पता चले कि मूल्यों के धरातल पर हम कहां खड़े हैं।
: क्या आपने कभी पत्नी को पीटा है? : कम्युनिस्ट आंदोलन में ज्यादातर बहसें राजनीतिक, रणनीतिक और कूटनीतिक सवालों पर होती हैं। किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र उठाकर देख लें। अव्वल तो उनमें बहसें ही बहुत कम मिलती हैं और जब-तब मिलती भी हैं तो इससे अलग वहां शायद ही कुछ पढ़ने को मिलता है। मूल्यों के सवाल पहले से हल मान लिए गए हैं। माना जाता है कि जीवन मूल्य और नैतिकता के प्रश्नों पर मार्क्स और एंगेल्स ने, या फिर लेनिन और माओ ने जरूर कहीं न कहीं लिखा होगा, और जरूरत पड़ी तो उसे किसी किताब में खोज कर पढ़ लिया जाएगा। ऐसी समझ से मुझे खुजली होती है। पार्टी में अक्सर नजर आता है कि एक-दूसरे के साथ रिश्तों में हम सामंती या पूंजीवादी मूल्यों को ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेते हैं। शीर्ष कम्युनिस्ट नेताओं को भी कुछ इस तरह देखा जाता है, जैसे दफ्तरों में मातहत लोग अपनी सीआर खराब हो जाने के डर से अपने अफसरों को देखते हैं।
संगठन के भीतर प्रेम के रिश्ते झगड़े और किचाइन का सबब बन जाते हैं। स्त्री कॉमरेडों के प्रति नजरिया छोरों में चलता है। कुछ लोग ऊपर से कुछ जाहिर किए बगैर कंबल ओढ़ कर घी पीने में भरोसा रखते हैं तो कुछ उन्हें देवी तुल्य मानते हैं। इस डर से कि कहीं उनकी शान में कोई गुस्ताखी न हो जाए, उनके सामने लोग अपने व्यवहार में अति सतर्क हो जाते हैं। इस अटपटेपन का नतीजा पार्टी  कमिटियों में स्त्रियों की गैरमौजूदगी में जाहिर होता है, लेकिन वह अलग कहानी है। पहले ही बता चुका हूं कि मेरा निजी जीवन घरेलू तकरारों से भरा रहा है, लिहाजा मेरी यह दिली इच्छा थी कि वास्तविक जीवन में संबंधों की गति को समझूं और उनमें कम्युनिस्ट मूल्यों के लिए कोई जगह बनाऊं। इस क्रम में कम्युनिस्ट मूल्यों के बारे में मेरी समझ भी बदलती है तो बदले। एक सामाजिक प्रेक्षक और कार्यकर्ता के लिए बनी-बनाई धारणाएं टूटने से अच्छी बात भला और क्या हो सकती है।
कमिटियों में स्त्रियों की गैरमौजूदगी में जाहिर होता है, लेकिन वह अलग कहानी है। पहले ही बता चुका हूं कि मेरा निजी जीवन घरेलू तकरारों से भरा रहा है, लिहाजा मेरी यह दिली इच्छा थी कि वास्तविक जीवन में संबंधों की गति को समझूं और उनमें कम्युनिस्ट मूल्यों के लिए कोई जगह बनाऊं। इस क्रम में कम्युनिस्ट मूल्यों के बारे में मेरी समझ भी बदलती है तो बदले। एक सामाजिक प्रेक्षक और कार्यकर्ता के लिए बनी-बनाई धारणाएं टूटने से अच्छी बात भला और क्या हो सकती है।
स्त्री-पुरुष संबंधों को लेकर जिस मीटिंग की बात मैंने पिछली कड़ी में की थी, वह अजित गुप्ता के घर की छोटी सी दालान में हुई थी। अजित जी आईपीएफ के भोजपुर जिला सचिव थे और बाइस महीने जेल में रहने के बाद थोड़े ही दिन पहले छूट कर आए थे। अजित गुप्ता मेरी जिंदगी में आए एक इतने दिलचस्प और ट्रैजिक करैक्टर हैं कि उनके बारे में बात h करने का एक भी मौका मैं छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अभी इतना ही कहकर संतोष करना होगा कि इस मीटिंग में वे शामिल नहीं थे। आग्रह के बावजूद महिलाएं इस मीटिंग में भी मात्र दो ही शामिल हो पाई थीं। अनुपमा, जो बहुत अच्छी अभिनेत्री थी और बोकारो में पार्टी की कार्यकर्ता भी रह चुकी थी, फिलहाल हमारी गीत-नाटक इकाई युवानीति के केंद्रीय व्यक्ति सुनील की पत्नी थी। और आशा, जो अधेड़ उम्र की शिक्षक थीं और आईपीएफ की शहर इकाई में जब-तब सक्रिय रहती थीं।
बाकी ज्यादातर लीडिंग टीम के लोग और विभिन्न मोर्चों के प्रभारी थे। मीटिंग का अजेंडा था- क्या आपने कभी अपनी पत्नी को पीटा है। दोनों महिलाओं का इस अजेंडे पर एतराज था कि अजेंडा अगर यही रखना है तो उन्हें बुलाने का क्या मतलब है- यह तो पहले से ही तय है कि उन दोनों ने अपनी पत्नी को नहीं पीटा है। एतराज मीटिंग में शामिल दो-तीन कुंआरों को भी था, लेकिन अपने कुआंरेपन का हवाला देकर उन्हें मनाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। बातचीत शुरू हुई तो पता चला कि मीटिंग में मौजूद जिन भी लोगों की पत्नियां थीं, वे सभी उनको कभी न कभी या तो पीट चुके थे या छोटी-मोटी चोट लगने की हद तक धक्का दे चुके थे। झगड़े की वजहों की कोई कमी नहीं थी। सभी के जीवन आर्थिक अभाव से भरे हुए थे। जेब में पैसे नहीं हैं। जरूरतें मुंह बाए खड़ी हैं। बच्चों की तरफ से शिकायत मां को ही करनी होती है और अक्सर उसे ही घर चलाने वाले के गुस्से का शिकार भी होना पड़ता है।
इसका अपवाद सिर्फ हमारी रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष गोपाल जी थे, जिनका कहना था कि उन्होंने अपनी पत्नी को कभी नहीं पीटा है, अलबत्ता उनकी पत्नी ने ही एक बार गुस्से में आकर उनपर हाथ उठा दिया था। क्या इसलिए कि गोपाल जी पहले रिक्शा चलाते थे और यह काम भी हाइड्रोसील की समस्या हो जाने के चलते कुछ साल पहले छोड़ चुके थे, जबकि उनकी पत्नी अस्पताल में दाई थीं और रेगुलर तनख्वाह न मिलने के बावजूद नेग-चार के रूप में जैसे-तैसे घर चलाने भर को कमाई कर लेती थीं। गोपाल जी अगर चाहते तो पिटाई के सार्वभौम रिश्तों में आए इस उलटफेर के लिए अपनी आर्थिक मजबूरियों का रोना रो सकते थे। लेकिन मीटिंग में सवाल किए जाने पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि परेशानी होती है तो गुस्सा आ जाता है। पत्नी ने जान-बूझ कर उन पर हाथ नहीं उठाया था और इसका उन्हें बहुत बाद तक अफसोस भी रहा।
सबसे ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब सुनील ने भी एक बार अनुपमा को धक्का देने और उस पर हाथ छोड़ने की बात स्वीकार की। दोनों की शादी तीन-चार साल पहले हुई थी। बच्चा अभी कोई नहीं था। सुनील के माता-पिता दोनों शिक्षक थे। घर भी ठीक-ठाक था, कोई खास आर्थिक परेशानी भी नहीं थी। सुनील ने बताया कि फ्रस्ट्रेशन में ऐसा हो गया था। नौकरी के लिए बीसियों जगह अप्लाई करते हैं, कहीं से कॉल नहीं आती। आती भी है तो कहीं न कहीं मामला फंस जाता है, नौकरी नहीं मिलती। यह एक ऐसा पहलू था, जो मीटिंग में बैठे सभी नौजवानों को खामोश कर गया। होलटाइमर बनने की मानसिकता में उनमें कोई भी नहीं था। क्या एक न एक दिन उनके साथ भी ऐसी स्थिति आनी है। जब अनुपमा की बारी आई तो उसने एक सैद्धांतिक बात कही- फ्रस्ट्रेशन की शिकार औरत ही क्यों होती है। सुनील को फ्रस्ट्रेशन था तो वे अपना हाथ दीवार पर मार लेते, ज्यादा से ज्यादा वह सुसाइड की कोशिश कर सकते थे। लेकिन इनको नौकरी नहीं मिल रही थी तो इन्होंने मुझे क्यों मारा।
एक स्तर पर चीजें मूल्यों पर ही आ गिरती हैं। आर्थिक समस्याएं न हों तो भी क्रोध के आवेग तो आते ही हैं। उनका उठना ही सिरे से रोक दिया जाए, इसका फिलहाल कोई तरीका नहीं है। शायद साइकियाट्री या मेडिकल साइंस भविष्य में इसका कोई तरीका खोज ले, लेकिन क्रोध न आने के कुछ दूसरे खतरे भी होंगे। असल मामला इन आवेगों की दिशा का है। सबसे नजदीकी और सबसे कमजोर लोग ही इनका शिकार बनते हैं। कभी बच्चे, कभी पत्नी, कभी छोटे भाई-बहन, कभी बूढ़े मां-बाप। ऐसा न हो, वे गृहस्वामी के गुस्से के शिकार न बनें, इसके दो ही तरीके हैं। एक तो यह कि वे कमजोर न रह जाएं। उनकी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक स्थिति ऐसी हो कि मुकाबला कर सकें। कई बार ऐसा एक भी मुकाबला समीकरण को हमेशा के लिए बदल देता है। दूसरा तरीका जीवन मूल्यों के बदलाव का है। बहुत कठिन, लेकिन सबसे सुरक्षित। यूं कहें कि बिल्कुल फूलप्रूफ। उस मीटिंग में कम्युनिस्ट होने की एक कसौटी तय हुई। अपने सबसे नजदीकी लोगों के साथ दुख-सुख का ही नहीं, जीवन मूल्यों का भी साझा किया जाए। कुछ इस तरह कि अगले आवेग के वक्त कम्युनिस्ट होने की कसम याद रहे।
बाद में इस कसौटी का विस्तार मैंने धार्मिक लोगों तक किया- यानी पाखंडी धार्मिक लोगों तक नहीं, उन लोगों तक, जो धर्म के आध्यात्मिक अर्थ लेते थे। मेरे परिचितों का दायरा काफी बड़ा रहा है। इसमें रजनीशी, बालयोगेश्वर के अनुयायी, राधास्वामी वाले, अखंड ज्योति वाले, सूफी, लिबरेशन थियोलॉजी और कई दूसरी किस्मों के लोग भी रहे हैं। जीवन मूल्यों की थाह लेने के लिए आज भी मेरे लिए सबसे बड़ी कसौटी ऐंगर मैनेजमेंट ही है- कोई जिस हद तक इसे कर सके, वह उतना आस्थावान। फिर आस्था का रूप चाहे धार्मिक हो या किसी कम्युनिस्ट की तरह नास्तिक। कम्युनिस्ट होने के लिए अतिरिक्त कसौटी संबंधों के ढांचे में बदलाव की है। इन दोनों कसौटियों पर मैं अपना आकलन करूं तो खुद को आज भी खिझा देने की हद तक कच्चा पाता हूं। पति-पत्नी संबंधों के मामले में स्थिति लगभग संतोषजनक कही जा सकती है लेकिन बाकी रिश्तों में- जैसे बच्चे और अपनी मां के साथ के रिश्ते के मामले में ऐसा नहीं कह सकता।
: दीनाजी का किरदार : समूचे हिंदीभाषी क्षेत्र में नक्सल आंदोलन को नजदीक से जानने के लिए भोजपुर से अच्छी और कोई जगह नहीं है। लेकिन इसे जानने की प्रक्रिया में मुझे एक किस्म के मोहभंग से भी गुजरना पड़ा। बतौर कार्यकर्ता यहां मेरी मौजूदगी के पहले साल में पार्टी की कमान दीनाजी के हाथ थी, जो खुद में आंदोलन के एक जीते-जागते स्कूल थे। वे पूर्वी बंगाल के एक जमींदार परिवार से आए थे और देश विभाजन के बाद उनके परिवार ने फाकाकशी की नौबत भी झेली थी। बहादुरी, जिंदादिली और राजनीतिक कौशल की उनके जैसी मिसालें आज तक मुझे कम ही देखने को मिली हैं, लेकिन उनसे निजी बातचीत में पहली बार यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ था कि एक गंभीर आर्थिक आरोप में उन्हें पार्टी की राज्य कमिटी से हटा दिया गया था और बतौर जिला सचिव भी वे लगभग  सस्पेंशन की स्थिति में ही चल रहे थे।
सस्पेंशन की स्थिति में ही चल रहे थे।
कुछ लोगों का आरोप था कि दीनाजी ने पार्टी के पैसे खाए हैं और वे इस आरोप को स्वीकार भी कर चुके थे। भोजपुरी और हिंदी के प्रतिष्ठित कवि और पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति के सदस्य रमाकांत द्विवेदी रमता उनके खिलाफ आरोपों की जांच कर रहे थे और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने दीनाजी को न सिर्फ सभी नेतृत्वकारी पदों से बल्कि पार्टी से भी हटा देने की अनुशंसा की थी। दीनाजी ने सारे आरोपों पर अपनी सफाई देते हुए उनसे अपनी अनुशंसाओं में कुछ नरमी ला देने की गुजारिश की थी लेकिन रमता जी का कहना था कि वे अपनी रिपोर्ट का एक कमा (कॉमा नहीं) भी बदलने को तैयार नहीं हैं।
बाद में दीनाजी ने इस आरोप के बारे में मुझे विस्तार से बताया। बंगाल में रह रहा उनका परिवार उनके घर छोड़ने के बाद छिन्न-भिन्न हो चुका था। उनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी थी और भाई-बहन (कितने थे और कहां, यह मुझे याद नहीं) अपनी-अपनी राह चले गए थे। भूमिगत जीवन में ही पार्टी संपर्कों से दीनाजी की शादी हो गई थी। उनकी ससुराल खड़कपुर में थी और पत्नी पांच-छह साल की एक बेटी के साथ वहीं रहती थीं। पत्नी पार्टी की हमदर्द थीं और उन्हें पता था कि दीनाजी क्या कर रहे हैं (दीनाजी का घर का नाम अरूप पॉल था और उनकी पत्नी की चिट्ठी सुंदर बांग्ला अक्षरों में शुप्रियो ओरूप के संबोधन से शुरू हुआ करती थी) लेकिन अपने परिवार को उन्होंने यही बता रखा था कि उनके पति बिहार में पटना के पास किसी मिल में काम करते हैं।
दीनाजी के सास-ससुर बहुत ही बूढ़े और बीमार थे। किसी गंभीर आर्थिक तंगी में कुछ पैसे घर भेजने के लिए उन्होंने एक छोटा सा, लगभग अहानिकर किस्म का घपला कर डाला था। आरा में अपने जनाधार में पड़ने वाले गांव श्रीटोला में एक पोखरा था, जिसकी मछलियों के लिए हर साल ग्राम पंचायत की तरफ से उसकी नीलामी होती थी। संयोग से उस सीजन में दीनाजी के पास पार्टी लेवी के मद में आए कुछ पैसे थे। पार्टी के ही एक साथी को प्रॉक्सी बनाकर उन्होंने लेवी के पैसे से वह पोखरा नीलामी में ले लिया था। कुल 15 हजार रुपये में बोली छूटी थी। कुछ महीने बाद मछली की बेच से आए पैसों में से पार्टी के पैसे उन्होंने पार्टी के खाते में डाल दिए और पोखरे से हुई कमाई का एक छोटा हिस्सा प्रॉक्सी खरीदार को देकर बाकी हिस्सा अपने अपने घर खड़कपुर भेज दिया था।
1988 में चुनाव लड़ने के फैसले से लेकर 1989 में अपना सांसद चुने जाने और 1991 में उनकी हार के बाद राजनीतिक धक्का लगने तक पार्टी लगातार आगे बढ़ रही थी लिहाजा दीनाजी की गड़बड़ियां भी ढकी हुई थीं। लेकिन धक्का लगते ही सारे समीकरण बदल गए। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भोजपुर के संगठन में मौजूद बाकी खामियां भी दिखाई पड़ने लगीं। दीनाजी के राजनीतिक और सांगठनिक गुणों पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता था, लेकिन कुछ तो वजह थी जो आईपीएफ और बाकी जनसंगठनों के ऊपरी ढांचों में अपराधी और दलाल प्रवृत्ति के लोगों का असर बढ़ गया था।
कोई तो बात थी जो अपने त्याग-बलिदान के गीत गाने वाले दशकों पुराने कार्यकर्ता अपनी जात-बिरादरी की कसमें खाने लगे थे और चुनावी टिकट के लिए पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन कराने की हद तक पहुंच गए थे। 1989 के आम चुनाव के समय हुए बिहटा जनसंहार से लेकर 1991 के मध्य तक हमारे जनाधार के खिलाफ कई बड़े हमले हो चुके थे। कार्यकर्ता बुरी तरह सहमे हुए थे और लालू यादव के चढ़ते सितारे के सामने पार्टी राजनीतिक रूप से भी कहीं खड़ी नहीं हो पा रही थी। ऐसे ही माहौल में सोन नदी के किनारे सहार ब्लॉक के एक गांव में पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें पार्टी महासचिव विनोद मिश्र ने भी शिरकत की।
वह एक ऐतिहासिक बैठक थी और उसी में पहली बार मुझे पता चला कि राजनीति में तख्तापलट कैसे होता है। बाद में अपने अराजनीतिक जीवन में मुझे मीडिया संगठनों और दूसरी जगहों पर ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलीं, लेकिन इसका सबसे ट्रैजिक और उतना ही उज्जवल रूप मुझे उसी समय देखने को मिला। करीब बारह साल से भोजपुर में पार्टी का नेतृत्व संभाल रहे दीनाजी उस बैठक में इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिए गए। उन्हें नए-नए बने जिले बस्तर में पार्टी का काम देखने के लिए कहा गया, ताकि पार्टी के काम का विस्तार हो और बीच-बीच में थोड़ा-बहुत समय वे अपने घर को भी दे सकें। हकीकत यह थी कि यह सिर्फ भाषा का खेल था।
किसी नए जिले में काम करते हुए पार्टी नेताओं के लिए अपना नमक-रोटी चलाना भी मुश्किल रहता है, ऐसे में पार्टी का काम करते हुए अपने घर की मदद वे भला कहां से कर पाते। शाम को जंगल-पानी के लिए जाते हुए दीनाजी ने डबडबाई आंखों और रुंधे हुए गले से हमसे बात की। बोले, मैं पार्टी की सेंट्रल कमेटी में था, फिर राज्य कमेटी में रहा, और अब भोजपुर जिला कमेटी से भी हटा दिया गया, इससे आगे अब मेरा क्या होगा। उनके पीछे उनकी जिम्मेदारी संभालने जा रहे कुणाल जी भी वहीं थे। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों सोचते हैं, अभी आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, दूसरी तरफ भोजपुर का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा है…..। दीनाजी यह सब समझते थे, लेकिन वे जान गए थे कि उनकी जिंदगी पटरी बदल रही है।
मुझे आज भी लगता है कि समय की जरूरत और विनोद मिश्र की तीक्ष्ण सांगठनिक मेधा के बावजूद उनका यह फैसला पार्टी के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ। इसका एक पहलू दीनाजी की मदद के लिए आईपीएफ के बक्सर जिला अध्यक्ष के रूप में अजित गुप्ता को वहां भेजा जाना था, जिसका अंत उनके नए-नए दांपत्त्य जीवन की तबाही, पार्टी से उनके निष्कासन, असाधारण फ्रस्ट्रेशन और अंततः उनकी मृत्यु के रूप में सामने आया। लेकिन इस बारे में कभी बाद में बात होगी। दीनाजी के लिए इसका मतलब साफ था। छह महीने के अंदर वे बक्सर में पार्टी का काम छोड़ कर पूरी तरह खड़कपुर ही शिफ्ट हो गए और वहां बतौर पार्टटाइमर पार्टी की कर्मचारी यूनियनों में काम करते हुए जैसे-तैसे अपना घर-परिवार चलाने लगे। 1992 के अंत में पार्टी की कोलकाता कांग्रेस के बाद हुई राष्ट्रीय रैली में उनसे मुलाकात हुई। सीपीआईएमएल के नंबर दो नेता शंभूजी दीनाजी से अचानक हुई भावविह्वल मुलाकात के बाद मीठी बांग्ला में उनसे बात कर रहे थे। मैं बांग्ला बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन उनके बिखरे-बिखरे शब्द आज भी मेरे कानों में बजते हैं।
शंभूजी- एते पारे देखी छी, आमार दीना कोथाय, आमार दीना कोथाय। (इतनी देर से देख रहा हूं, मेरा दीना कहां है, मेरा दीना कहां है)
दीनाजी- एई दीना शेई दीना की। (यह दीना वही दीना है क्या)
शंभूजी- शेई दीना, शेई दीना- पोरिश्थिति भिन्न। (वही दीना, वही दीना, परिस्थिति भिन्न है)
वह दिन है और आज का दिन है। इन अट्ठारह वर्षों में दीनाजी से फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। पता नहीं आगे फिर कभी होगी भी या नहीं।
: सशस्त्र क्रांतिकारिता के सच : बक्सर में हुई पार्टी जिला कमेटी की पहली ही मीटिंग में ही मेरी मुलाकात दो योद्धाओं से हुई थी। उनमें एक उस समय पार्टी की आर्म्ड यूनिटों की प्रभारी की भूमिका में थे, जबकि दूसरे एक बम विस्फोट में एक आंख और आधे चेहरे की त्वचा गंवा देने के बाद किसी तरह मौत के मुंह से निकल आए थे और एक ब्लॉक में मुख्य पार्टी संगठक का काम देख रहे थे। दूसरे वाले साथी के बारे में बात करने का मौका शायद अपने जेल प्रकरण पर चर्चा के दौरान आए। पहले वाले (जिनका असली नाम मुझे कभी पता नहीं चला और जो नाम चलन में था, उसे भी बदल कर मैं  यहां विष्णु जी रख देता हूं) शुरू में मुझे मीटिंग के इंतजाम में शामिल किसी लोकल लड़के जैसे लगे। कुछ समय बाद मैंने गौर किया कि उनके ऊपरी जबड़े के किनारे वाले दो दांत गायब हैं और उनके हंसने में कोई गहरी बात है। खुल कर हंसते हुए भी उनकी आंखें थोड़ी उदास और वेधती हुई सी लगती थीं। मीटिंग के दौरान परिचय हुआ तो सोच में पड़ गया कि डेढ़ पसली के ये सज्जन क्या खाकर पुलिस और गुंडा गिरोहों से मुठभेड़ में उतरते होंगे। लेकिन समय बीतने के साथ इस तरह के भ्रम दूर होते चले गए।
यहां विष्णु जी रख देता हूं) शुरू में मुझे मीटिंग के इंतजाम में शामिल किसी लोकल लड़के जैसे लगे। कुछ समय बाद मैंने गौर किया कि उनके ऊपरी जबड़े के किनारे वाले दो दांत गायब हैं और उनके हंसने में कोई गहरी बात है। खुल कर हंसते हुए भी उनकी आंखें थोड़ी उदास और वेधती हुई सी लगती थीं। मीटिंग के दौरान परिचय हुआ तो सोच में पड़ गया कि डेढ़ पसली के ये सज्जन क्या खाकर पुलिस और गुंडा गिरोहों से मुठभेड़ में उतरते होंगे। लेकिन समय बीतने के साथ इस तरह के भ्रम दूर होते चले गए।
माओ त्से तुंग ने जनयोद्धाओं के बारे में लिखा है कि उन्हें जनता के बीच पानी में मछली की तरह रहना चाहिए। उनके होने की पहली शर्त ही यही है कि वे बिल्कुल आम आदमी हों। हल्का-फुल्का, इकहरा शरीर, चाल-ढाल, बातचीत में कुछ भी ऐसा न हो जिससे आसानी से उनकी पहचान की जा सके। जरूरत पड़ने पर कई-कई दिन बिना खाए, बिना सोए लगातार चीते की तरह चौकन्ना रह सके, चारो तरफ पड़े घेरे से भी हवा की तरह निकल जाए, ऐसा आदमी ही जनता का युद्ध लड़ सकता है। लड़ाई में उसे बेरहम होना चाहिए, लेकिन आम जीवन में उतना ही संवेदनशील भी होना चाहिए। ऐसे ही एनिग्मा मुझे विष्णु जी हमेशा नजर आए। दो-तीन बार हम आरा की बसों में साथ-साथ गए। संयोगवश एक बार किसी बात को लेकर कंडक्टर से थोड़ी झंझट हो गई। मुझे लगता था कि हम दो लोग हैं, कंडक्टर की गुंडई नहीं चलने देंगे। लेकिन बाद में पता चला कि वहां मैं अकेला ही हूं। विष्णु जी साथ होते हुए भी साथ नहीं थे। वे लगातार अपनी सीट पर ही बैठे रहे और पूरे झगड़े के दौरान एहसास तक नहीं होने दिया कि वे मेरे साथ हैं।
उनसे पहले अपने आंदोलन से जुड़े और भी जनयोद्धाओं से मेरी मुलाकात थी। पटना में मुंशी जी नाम के जिन कमांडर के साथ लगातार चार रात मार्च करने का मौका मिला था, उनका शरीर गठीला और बाल घुंघराले थे। चेहरे से साहस और आक्रामकता टपकती थी। बाद में मुझे लगा कि किसी छापेमारी में उनके लिए आम लोगों के बीच घुल-मिल जाना काफी मुश्किल होता रहा होगा। पालीगंज में थोड़ी देर के लिए अनिल जी उर्फ कउसा से मुलाकात हुई थी, जो इसके अगले साल ही पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में शहीद हो गए (असल में उन्हें राह चलते पकड़ा गया और फर्जी मुठभेड़ में मार डाला गया)। बिहार के गांवों में कउसा कंजी आंख वाले लोगों को कहते हैं और पुलिस में अनिल जी के नाम का खौफ उनके इस उपनाम की शक्ल में ही जाहिर होता था। उनका निशाना इतना पक्का था कि अंधेरी रात में फर्लांग भर दूरी से छान पर पड़े कद्दू में गोली मार सकते थे। लेकिन उनके लिए भी लोगों में घुल-मिल जाना आसान नहीं था। लंबा कद, खिलाड़ियों जैसी चुस्ती और हमेशा चुगली करती रहने वाली कंजी आंखें उन्हें कहीं भी पकड़वा सकती थीं।
बहरहाल, विष्णु जी अब तक देखे गए सारे योद्धाओं से अलग थे। उनका युद्ध कौशल ही नहीं, पूरा व्यक्तित्व उन्हें आदर्श जनयोद्धा बनाता था। काफी समय बाद मुझे पता चला, वे रोहतास जिले में तंतवा (डलिया वगैरह बनाने वाली ) जाति के एक भूमिहीन किसान परिवार से आए हैं। उमर मुझसे करीब दस साल ज्यादा है। शादी हो गई है। पत्नी और एक बेटी कहीं सड़क किनारे मंड़ई डाल के रहती हैं। छोटे-मोटे सामान बनाकर और खेतों में मजदूरी करके गुजारा करती हैं लेकिन कुछ समय पहले उन्हें अपनी मंड़ई भी छोड़नी पड़ गई है। विष्णु जी का अतीत इस वर्तमान से भी कहीं ज्यादा भयानक था। उनके पिता के जीते जी ही गांव के राजपूत जमींदार ने उनकी मां को अपनी रखेल बना लिया था। एक साथी का कहना था कि विष्णु जी असल में जमींदार के ही लड़के हैं और उनके हाई स्कूल तक पढ़ लेने की व्यवस्था उनके कानूनी पिता के बजाय इस जैविक पिता ने ही की थी।
एक दिन विष्णु जी स्कूल से घर लौटे तो देखा कि दरवाजा खुला है। भीतर चारपाई पर उनके जैविक पिता की गला कटी लाश पड़ी है और उसके खून की एक पतली धारा बहती हुई चौखट तक आ गई है। इस किस्से की अपनी पेचीदगियां हैं, जिनके निस्तार की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि विष्णु जी इस बारे में मैं कोई बात नहीं कर सकता था। जिन साथी ने यह कहानी सुनाई थी, उन्होंने बताया कि लाश देखते ही विष्णु जी शॉक में वापस मुड़े और भागते ही चले गए। बाद में उसी खौफ के किसी पल में उनकी मुलाकात पार्टी के किसी साथी से हुई और उन्हें दस्ते में शामिल कर लिया गया। निश्चित रूप से उनकी सोच में जाति उत्पीड़न का बहुत गहरा तत्व मौजूद था, जो कभी-कभी घोर सवर्ण विरोधी दुराग्रहों की शक्ल में भी सामने आता था। मसलन, आरा अस्पताल में एक घायल साथी का इलाज करने से मना कर देने वाले डॉक्टर का पक्ष लेकर खामखा गुंडई करने वाले दुसाध जाति के एक कंपाउंडर को पार्टी के कुछ साथियों ने उसके घर के पास ही घेर कर पीटा तो विष्णु जी ने कहा, ऐसा आप लोग किसी ठाकुर या भूमिहार गुंडे के साथ करते तो पता चल गया होता।
पार्टी के हथियारबंद दायरे के शीर्ष नेता की सोच में मौजूद जाति और वर्ग की इस दुविधा का हमारे आंदोलन को काफी नुकसान उठाना पड़ा। जगदीशपुर के इटाढ़ी गांव में जमीन को लेकर लड़ाई चल रही थी। यहां ज्यादातर जमीनें ठाकुर जाति के भूस्वामियों के पास थीं और साथ में उन्होंने भूमिहीनों को आवंटित ग्राम समाज वगैरह की जमीनों पर भी कब्जा कर रखा था। एक रात इसी पृष्ठभूमि के कुछ लोग जगदीशपुर में बीजेपी की एक चुनावी सभा में शामिल होकर ट्रैक्टर से लौट रहे थे। उसी समय विष्णु जी के नेतृत्व में उन पर हमला हुआ, जिसमें पांच लोग मारे गए। यह घटना मानवीय दृष्टि से तो गलत थी ही, आंदोलन के लिए भी किसी लिहाज से ठीक नहीं थी। बाद में इसे और बेलाउर गांव की इससे मिलती-जुलती एक घटना को आधार बनाकर गठित हुई रणवीर सेना की ठाकुर-भूमिहार गोलबंदी के चलते पार्टी के कई साल बर्बाद हुए। भोजपुर, पटना और जहानाबाद में हमारे जनाधार के सौ से ज्यादा लोग रणवीर सेना के हमलों में मारे गए और पार्टी के कई संभावनाशील नेताओं-कार्यकर्ताओं को अपनी जानें गंवानी पडीं।
इटाढ़ी हमले के अगले दिन ही पार्टी की जिला स्टैंडिंग कमेटी में मैंने इसका विरोध किया लेकिन अगले दिन पर्चा निकाल कर पार्टी प्रवक्ता के रूप में जिम्मेदारी भी ली। इस घटना के पीछे जिला कमेटी का कोई फैसला नहीं था। न ही पार्टी सेक्रेटरी कुणाल जी से इसके बारे में कोई राय ली गई थी। फिर भी कुणाल जी ने इस पर कोई नाराजगी नहीं दिखाई और आलोचना या तारीफ के रूप में सिर्फ इतना कहा कि वर्ग संघर्ष में यह सब होता रहता है। मुझे तब भी लगता था और आज भी लगता है कि कुणाल जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजनीतिक नेतृत्व को कभी भी हथियारबंद ताकतों की हां में हां नहीं मिलानी चाहिए और हथियारों को पूरी सख्ती से राजनीति के नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि इनके इस्तेमाल से होने वाला नुकसान इनसे होने वाले तात्कालिक फायदे की तुलना में कहीं ज्यादा होता है। बहरहाल, इटाढ़ी की घटना के तुरंत बाद आनंद मोहन और प्रभुनाथ सिंह ने इसे लेकर बिहार व्यापी ठाकुर गोलबंदी बनाने का प्रयास किया। आरा की एक आमसभा में उन्होंने मेरा नाम ले-लेकर मेरे खिलाफ आक्रामक भाषण दिए। मार डालूंगा-काट डालूंगा टाइप इन भाषणों के वक्त मैं सभा में ठीक इनके सामने ही खड़ा था और आरा के पत्रकारों को लग रहा था कि अभी कुछ न कुछ बवाल होकर रहेगा।
: सशस्त्र क्रांति – असाध्य आशावाद : अपने यहां सशस्त्र संघर्ष की छवि काफी रोमांटिक-सी रही है। स्वभावतः जुझारू, संघर्षशील लोगों से ज्यादा इसका आकर्षण आम जीवन में लड़ाई-झगड़े से दूर रहने वाले सीधे-सादे लोगों में देखा जाता है। परंपरा से अहिंसक और निहत्थे भारतीय समाज में इसकी वजह खोजना कठिन नहीं है, हालांकि इसके चलते कभी-कभी कुछ अलग ही तरह के गुल खिले हुए दिखाई पड़ते हैं। इलाहाबाद में कुछ समय के लिए हमारे संगठन में सक्रिय हुए एक साथी सुरेंद्र मिश्र छात्र आंदोलन से अलग-थलग रहते हुए प्रायः अंडरग्राउंड सी मुद्रा बनाए रखते थे। उस समय मेरा संगठन से जुड़ाव बनना शुरू ही हुआ था।
संगठन के सारे लोग और उनका किया सारा कुछ तब किसी दिव्य आभा से मंडित जान पड़ता था। उन्हीं दिनों ताराचंद हॉस्टल में किसी लड़के ने हमारे एक साथी अरुण कुमार को पीट दिया तो रात में संगठन की एक टीम उसकी मिजाजपुर्सी करने पहुंची। इस टीम में सुरेंद्र शामिल थे। सशस्त्र संघर्ष के प्रति उनके घोषित लगाव के चलते टीम के पास मौजूद अकेला कट्टा भी उन्हीं के पास था। धौंस-धमकी से बात नहीं बनी। बात लड़ाई-झगड़े तक पहुंची तो सुरेंद्र ने न सिर्फ कट्टा ताना बल्कि गोली भी चला दी। साथियों का कहना था कि इसके बाद उनकी हालत देखने लायक थी। जिस लड़के को गोली लगी, संयोगवश उसे प्राणघातक चोट नहीं पहुंची, लेकिन सुरेंद्र खुद इतने नर्वस हो गए कि चीखने-चिल्लाने लगे। घटना में शामिल लोगों ने बाद में बताया कि हॉस्टल से भागते हुए उन्हें साथ लेकर जाना भारी समस्या हो गया था।
कम्युनिस्ट आंदोलन में इस तरह के रोमांटिक सशस्त्र संघर्ष के लिए भला क्या जगह हो सकती है, लेकिन भारत जैसे सामंती दबदबे वाले देश में न सिर्फ कम्युनिस्ट आंदोलन बल्कि बुनियादी मुद्दों को लेकर चलने वाले किसी भी लंबे आंदोलन के लिए पूरी तरह हथियार छोड़ कर चलना भी एक असंभव कल्पना ही लगता है। देश में शायद ही कोई पार्टी ऐसी हो, जिसके पास समय-समय पर सक्रिय होने वाले हथियारबंद लोगों की जमात न हो, हालांकि इनमें से ज्यादातर अपने को गांधीवादी और अहिंसक ही कहती हैं। आपको एकबारगी यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन एक बार कोशिश करके अपने इर्द-गिर्द व्याप्त किसी भी अन्याय, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कीजिए, अगले ही दिन आपको बुद्ध की तरह महाबोध हो जाएगा।
आश्चर्यजनक रूप से पुलिस भी अपने यहां ताकतवर लोगों के गुंडा गिरोह की तरह काम करती है, हालांकि पुलिस के आने से पहले ही आप रिश्तेदारी में या पैसे लेकर काम करने वाले किसी गुंडे के हाथों पिट चुके होते हैं। इस मुश्किल से निपटने का एक रास्ता सीधे, भले, गरीब और कमजोर लोगों को जुझारू बनाने, उन्हें पारंपरिक हथियारों से लैस करने का होता है, जिस पर मैंने सचेत ढंग से आरा शहर में काम किया और इसमें कुछ कामयाबी भी हासिल की। लेकिन बात जब कम्युनिस्ट आंदोलन और सशस्त्र संघर्ष के आपसी रिश्ते की होती है तो सशस्त्रीकरण के इस मॉडल को सिर्फ बचाव की रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है।
चीन की क्रांति से प्रेरणा लेते हुए अपने यहां सशस्त्र संघर्ष की तीन पांतों की कल्पना की जाती है। एक, जन मिलिशिया, यानी पारंपरिक हथियारों से लैस आम जनता जो वर्ग संघर्ष के दौरान जमींदारों और पूंजीपतियों के गुंडों से इन हथियारों के जरिए अपना बचाव करती है। दो, स्थानीय दस्ता, यानी परिष्कृत हथियारों से लैस योद्धाओं की एक छोटी इकाई जो जनता के बीच घुलमिल कर रहती है, जन मिलिशिया को प्रशिक्षित करती है और शासक वर्ग के अलावा जब-तब पुलिस से भी मुकाबले के लिए तैयार रहती है। तीन, चलायमान सेना, जो लड़ाई के उन्नत दौर में बड़े इलाकों में मार्च करती है, स्ट्रेटेजी बनाकर युद्ध लड़ती है और राष्ट्रीय सेना को परास्त कर देने के इरादे से काम करती है। रूस में ऐसी संरचनाएं क्रांति के बाद अस्तित्व में आई थीं, जबकि चीन में ये क्रांति से पहले भी करीब बीस साल तक वजूद में रहीं।
भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के आसपास हुए तेलंगाना और तेभागा के संघर्षों में सशस्त्र ढांचा जन मिलिशिया तक ही सीमित था। (तेलंगाना में कहीं-कहीं निजाम के रजाकारों से निपटने के लिए स्थानीय दस्ते भी बनाए गए थे।) लेकिन नक्सलबाड़ी के आंदोलन के लगभग शुरुआती दौर में ही फौज से लड़ने लायक चलायमान सेना के गठन की बात होने लगी थी। इसके तार चीन की सांस्कृतिक क्रांति में माओ त्से तुंग के नजदीकी समझे जाने वाले एक विवादास्पद करैक्टर लिन पियाओ की एक थीसिस से जुड़ते हैं, जिसके मुताबिक तीसरी दुनिया में क्रांति की स्थितियां हमेशा बनी रहती हैं। सत्तर के दशक में लिन पियाओ (संभवतः) एक प्रायोजित विमान दुर्घटना में इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनकी अजीब प्रस्थापना आज भी बारूदी सुरंग की शक्ल में जहां-तहां फटती रहती है।
बंगाल में नक्सलबाड़ी की पराजय के बाद नक्सल आंदोलन ने सशस्त्र संघर्ष का सबसे गहरा प्रयोग भोजपुर में ही किया। सत्तर के दशक में कुछ समय तक तो यहां हमला करो और डटे रहो का आत्मघाती सिद्धांत भी अमल में लाया गया था, जिसका नतीजा कई होनहार कार्यकर्ताओं और नेताओं की शहादत के रूप में देखने को मिला। सोलह कच्चे घरों को सुरंग से जोड़कर पहले पुलिस, फिर बीएसएफ और फिर भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट के साथ 105 घंटे मुकाबला करने के किस्से भी यहां सुने-सुनाए जाते हैं। बहुआरा गांव में हुई इस लड़ाई की दिनमान में छपी हुए एक रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है।
लेकिन मेरे भोजपुर पहुंचने तक ये सारी बातें किस्से-कहानियों में ही सिमट कर रह गई थीं। सेना और पुलिस से मुकाबला करना यहां करीब बीस वर्षों से पार्टी का अजेंडा नहीं रह गया था, क्योंकि क्रांतिकारी परिस्थितयां हमेशा मौजूद होने और अपनी मर्जी से जब चाहे तब क्रांति कर देने के विभ्रम से पार्टी अस्सी दशक की शुरुआत में ही मुक्त हो गई थी। (अपनी हथियारबंद कार्रवाइयों को लेकर इधर लगातार चर्चा में रह रही सीपीआई (माओवादी) की सोच आज भी वहीं है। हथियारों का इस्तेमाल वर्ग संघर्ष या जन संघर्ष को आगे बढ़ाने में करने के बजाय वह सेना और पुलिस पर हमला करते हुए चीन की तरह मुक्त क्षेत्र बनाने में कर रही है।)
सशस्त्र संघर्ष को लेकर पार्टी की समझ बदलने की बात सुनने में जितनी आसान लगती है, व्यवहार में यह उतनी ही मुश्किल साबित हुई। नक्सल आंदोलन के संस्थापक चारु मजूमदार ने कभी कहा था कि 1975 तक भारत अर्ध सामंती, अर्ध औपनिवेशिक बेड़ियों से आजाद हो जाएगा। 1972 में चारु मजूमदार शहीद हो गए। पुलिस और मिलिट्री के दमन के सामने आंदोलन बिखर गया। काफी दिनों तक हालत यह थी कि लोगों को पता तक नहीं था कि कौन कहां है। इसके बावजूद 1975 की शुरुआत से ही जो भी नक्सलवादी जहां भी था, उसने यह सोचकर वहीं लड़ाई में अपना सबकुछ झोंक दिया कि किसी न किसी चमत्कार से सन 75 के अंत तक देश में क्रांति जरूर हो जाएगी।
भोजपुर में सशस्त्र संघर्ष से जुड़े इस तरह के असाध्य आशावाद के कई अवशेष मेरे वहां रहते हुए भी जब-तब दिख जाते थे। चलायमान सेना की अवधारणा काफी पहले छोड़ दी गई थी। हथियारबंद दस्ते थे लेकिन पार्टी का जोर अब जुझारू जन आंदोलन खड़ा करने और इसके लिए बचाव के उपाय के रूप में जन मिलिशिया बनाने पर था। दस्तों में मौजूद योद्धाओं की मुख्य भूमिका स्थानीय संगठक और जन मिलिशिया के प्रशिक्षक की तय की गई थी, लेकिन उनकी तैयारी इस तरह की नहीं थी।
ग्रामीण गरीब जनता में इन योद्धाओं के प्रति गहरा लगाव और सम्मान मौजूद था, लेकिन रात बारह बजे राइफल लिए घूमने वाले व्यक्ति की अपनी छवि छोड़ना इनके लिए आसान नहीं था। कुल मिलाकर उनकी स्थिति दुविधापूर्ण थी। योद्धा बने रहने के लिए उनका उन्नत हथियारों में दक्ष होना, ड्रिल करना और हर रोज दस-पंद्रह किलोमीटर दौड़ना जरूरी था, जबकि संगठक बनने के लिए उनसे गहराई से पार्टी लाइन का अध्ययन करने, धीरज रखने, दो बात सुनकर गम खा जाने की अपेक्षा की जाती थी। हालात ऐसे थे कि दोनों में से कुछ भी उनसे हो नहीं पा रहा था और उनमें से ज्यादातर दिनोंदिन खराब योद्धा और खराब संगठक बनने की तरफ बढ़ रहे थे। मुझे नहीं पता कि इस स्थिति से उन्हें किसी बिंदु पर उबारा जा सका या नहीं। भोजपुर से आने वाली सूचनाएं इस संबंध में मुझे ज्यादा आशान्वित नहीं कर पाई हैं।
मेरी तरफ से उनके हालात बदलने में कोई खास योगदान नहीं हो पाया। मेरा कार्यक्षेत्र शहर में होने के चलते उनके साथ मेरा सीधे कोई जुड़ाव नहीं था। एक-दो बार आरा मोफस्सिल क्षेत्र में उनकी जरूरत पड़ी तो कोऑर्डिनेशन का काम जैसे-तैसे हो गया। लेकिन योद्धाओं की कार्यशैली बदलने का काम बहुत बड़ा था और इसे वही अंजाम दे सकता था, जिनके पास दिन-रात उनके साथ रहने का तजुर्बा हो। दीनाजी यह काम कर सकते थे लेकिन पारिवारिक मजबूरियों के चलते उनका रास्ता बदल गया। उनकी जगह लेने वाले कुणाल जी कुछ अपनी पृष्ठभूमि और कुछ इच्छाशक्ति की कमी के चलते इस काम को बहुत आगे नहीं बढ़ा सके।
….जारी…
 चंद्रभूषण को उनके जानने वाले चंदू या चंदू भाई के नाम से पुकारते हैं. चंदू भाई हिन्दी के वरिष्ठ पत्रकार हैं. इलाहाबाद, पटना और आरा में काम किया. कई जनांदोलनों में शिरकत की. नक्सली कार्यकर्ता भी रहे. ब्लाग जगत में इनका ठिकाना ”पहलू” के नाम से जाना जाता है. सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर बहुआयामी सरोकारों के साथ प्रखरता और स्पष्टता से अपनी बात कहते हैं. इन दिनों दिल्ली में नवभारत टाइम्स से जुड़े हैं. चंदू भाई से यह डायरी लिखवाने का श्रेय वरिष्ठ पत्रकार और ब्लागर अजित वडनेरकर को जाता है. अजित जी के ब्लाग ”शब्दों का सफर” से साभार लेकर इस डायरी को यहां प्रकाशित कराया गया है.
चंद्रभूषण को उनके जानने वाले चंदू या चंदू भाई के नाम से पुकारते हैं. चंदू भाई हिन्दी के वरिष्ठ पत्रकार हैं. इलाहाबाद, पटना और आरा में काम किया. कई जनांदोलनों में शिरकत की. नक्सली कार्यकर्ता भी रहे. ब्लाग जगत में इनका ठिकाना ”पहलू” के नाम से जाना जाता है. सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर बहुआयामी सरोकारों के साथ प्रखरता और स्पष्टता से अपनी बात कहते हैं. इन दिनों दिल्ली में नवभारत टाइम्स से जुड़े हैं. चंदू भाई से यह डायरी लिखवाने का श्रेय वरिष्ठ पत्रकार और ब्लागर अजित वडनेरकर को जाता है. अजित जी के ब्लाग ”शब्दों का सफर” से साभार लेकर इस डायरी को यहां प्रकाशित कराया गया है.