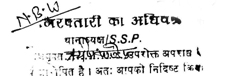![]() : विद्रोही चेतना और नोस्टेल्जिया : प्रेम में पागल होने को मैं एक काव्योक्ति भर समझता था। कॉमन सेंस इससे आगे बढ़ने की इजाजत आज भी नहीं देता। लेकिन राजीव को देखकर ही मैंने जाना कि इस दुनिया में प्रेम में सचममुच पागल हो जाने वाले लोग भी मौजूद हैं। सुनने और पढ़ने में यह अच्छा लगता है, लेकिन उस दिन ट्रेन से उतर जाने के साथ ही जाहिर हुई राजीव की न्यूरोसिस ने खुद उसका और उसके परिवार का जो हाल किया, उसे याद कर आज भी मन में लहर सी उठती है।
: विद्रोही चेतना और नोस्टेल्जिया : प्रेम में पागल होने को मैं एक काव्योक्ति भर समझता था। कॉमन सेंस इससे आगे बढ़ने की इजाजत आज भी नहीं देता। लेकिन राजीव को देखकर ही मैंने जाना कि इस दुनिया में प्रेम में सचममुच पागल हो जाने वाले लोग भी मौजूद हैं। सुनने और पढ़ने में यह अच्छा लगता है, लेकिन उस दिन ट्रेन से उतर जाने के साथ ही जाहिर हुई राजीव की न्यूरोसिस ने खुद उसका और उसके परिवार का जो हाल किया, उसे याद कर आज भी मन में लहर सी उठती है।
एक रात राजेंद्र नगर के रसोई वाले कमरे में मैं जर्मन नाजीवाद पर विलियम एल. शीरर की क्लासिक राइज ऐंड फाल ऑफ थर्ड राइख में डूबा हुआ था। अचानक लगा, कमरे के बाहर कोई चल रहा है।  करीब दो बजने वाले थे। दरवाजा खोलकर बाहर झांकता, इससे पहले ही आवाज आई- अबे भुषणा, चाय बना। मैंने कहा तुम इतनी रात में कैसे आ गए। घर लौट जाओ। राजीव बाबू गेट फांद कर आए थे और गेट फांद कर ही लौट गए। इसके अगले दिन ही घर वालों को उन्हें रांची मेंटल हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, लेकिन वहां से लौटने के कई महीने बाद तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की।
करीब दो बजने वाले थे। दरवाजा खोलकर बाहर झांकता, इससे पहले ही आवाज आई- अबे भुषणा, चाय बना। मैंने कहा तुम इतनी रात में कैसे आ गए। घर लौट जाओ। राजीव बाबू गेट फांद कर आए थे और गेट फांद कर ही लौट गए। इसके अगले दिन ही घर वालों को उन्हें रांची मेंटल हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, लेकिन वहां से लौटने के कई महीने बाद तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की।
ऐसी ही थी राजीव की न्यूरोसिस, जिसका दौरा पड़ने के बाद उनकी स्मरण शक्ति और संवेदना घटने के बजाय कहीं ज्यादा बढ़ जाया करती थी। उनकी एक खासियत यह भी थी कि प्रेम में अपनी नाकामी को तरह-तरह से रेशनलाइज करने की कोशिश करते थे- न जाने किसके लिए, और क्यों। मसलन यह कि सोना नीत्शे को पसंद करती थी- जरा सोचो, कोई पढ़ा-लिखा इंसान भला नीत्शे को पसंद कर सकता है। या फिर यह कि उसकी सोच का वर्ग चरित्र ही ऐसा नहीं था कि वह किसी से प्रेम कर सके। कुछ साल बाद राजीव अपने मौसा जी के परिवार के साथ रहने अमेरिका गए। घर वालों ने उन्हें नौकरी या कारोबार की उम्मीद में वहां भेजा था, लेकिन इन झंझटों से वे काफी आगे निकल आए थे। मुझे लगता है कि उनके अमेरिका जाने की सबसे बड़ी वजह उनके जेहन में यही रही होगी कि सोना चाहे जिसके भी साथ और जिस भी हाल में हो, लेकिन वहां कहीं राह चलते वह उन्हें जरूर दिख जाएगी। इधर काफी समय से राजीव के साथ मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन बचपन से लेकर आज तक मेरे मित्रों में वह अकेले ही हैं, जिनके साथ मैं घंटों बिना कुछ बोले आनंद से बैठा रह सकता हूं।
हमारे पटना पहुंचने के कोई साल भर बाद, 1989 के मई महीने में पार्टी ने जनमत के तीनों रंगरूटों विष्णु राजगढ़िया, इरफान और मुझे अलग-अलग इलाकों में हफ्ते भर के लिए किसान संघर्ष के इलाकों में हथियारबंद दस्तों के साथ रहने के लिए भेजा। विष्णु को जहानाबाद, इरफान को नालंदा और मुझे पटना ग्रामीण के पुनपुन, नौबतपुर और पालीगंज अंचलों में रहने के लिए भेजा गया। दरअसल, गांव भेजे जाने वालों में पटना और आसपास के पार्टी से जुड़े कुल दस नौजवान शामिल थे और मेरे ग्रुप में मेरे अलावा अलग-अलग मोर्चों पर काम करने वाले दो-तीन और लोग भी थे। विष्णु और इरफान ने बाद में अपने जो तजुर्बे बताए, वे कुछ खास नहीं थे, लेकिन मेरे लिए यह हफ्ता जिंदगी का एक असाधारण अनुभव साबित हुआ। आज भी इसके कुछ क्षणों की याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके दो-तीन साल बाद भोजपुर के अपने राजनीतिक जीवन में हथियारबंद नक्सली योद्धाओं के साथ रहना आए दिन की बात हो गई, लेकिन एक के बाद एक लगातार चार रातें लुंगी खुंटियाए हुए, छाती पर जिंदा ग्रेनेड टांगे, निपट अंधेरे में बगैर चश्मे के गेहूं, मटर और अरहर की खुत्थियों पर बिना दम लिए आठ-आठ मील भागना, बीच में कोई रोशनी दिख जाने पर किसी मेंड़ के किनारे कलटी मार लेना और खतरा निकल जाने का सिग्नल मिलने पर अगले जवान के साए के पीछे दोबारा दौड़ लगा देना जीवन में बस वही एक बार मई 1989 में ही हुआ।
मुझे नौबतपुर पहुंचने के लिए सिर्फ एक दुकान का पता दिया गया था। एक बच्चे ने वहां से मुझे पास के एक गांव में पहुंचा दिया। लोगों ने मुझे वहां एक लोटा पानी दिया और शाम तक घर में रहने को कहा। रात में एक साथी वहां से हमें लिवा कर सड़क के पार दूसरे गांव में ले गए। बारह बजे के आसपास खबर मिली कि दस्ते के लोग आ गए हैं। हम लोग वहां जाकर उनसे मिले। कमांडर ने हमें मार्च के कुछ नियम समझाए। पहला यह कि कंठ और जुबान से नहीं, सिर्फ सांसों में बात करें। आपके पास चमकने वाली कोई चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे चेन वाली घड़ी, चश्मा, नग वाली अंगूठी वगैरह। जरूरत पड़ने पर झुकने या लेट जाने में आसानी हो, इसके लिए पैंट के बजाय लुंगी पहन कर चलना ठीक रहेगा। खुले में मार्च करते वक्त सभी लोग एक दूसरे से लगभग पचास गज की दूरी बना कर चलेंगे और बिल्कुल एक सीध में नहीं चलेंगे।फिर उन्होंने हमें पिन वाले मिलिट्री ग्रेनेड के इस्तेमाल का तरीका बताया। कहा कि पिन खींचने के सात सेकंड के अंदर यह फट जाएगा, लिहाजा एक तो इसे पिन निकालने के तुरंत बाद न फेंकें, ताकि कहीं दुश्मन उसे उठाकर दोबारा आप पर ही न चला दे। और कम से कम तीस गज (नब्बे फुट) दूर फेंकें, ताकि कहीं खुद ही इसके शिकार न हो जाएं। और अंतिम हिदायत यह कि ग्रेनेड का इस्तेमाल या तो कमांडर के आदेश पर करें, या सिर्फ तब, जब यकीन हो जाए कि आदेश देने वाला या राइफल चलाने वाला एक भी साथी अब जिंदा नहीं बचा है। उनकी आखिरी बात हालत खराब करने वाली थी। लेकिन फौज तो फौज है। उसके नियम हमेशा सबसे बुरी संभावना को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। गांव के छोर पर फुसफुसाहटों की शक्ल में लगी यह पूरी क्लास महज पंद्रह मिनट में निपट गई। फिर बाहर से आए लोगों के कंधों पर आड़े-तिरछे टंगने वाली थैलियों में रखे ग्रेनेड कमांडर ने खुद अपने हाथ से टांगे। दस्ते के साथियों से रात भर का कार्यक्रम तय किया और आगे तीन, पीछे दो योद्धाओं के बीच शहर से आए हम तीन लोग भी आगे बढ़ चले।
राइज एंड फाल आफ थर्ड राइख… वीडियो देखने के लिए क्लिक करें- The Rise and Fall…..
बाद में इस यात्रा को लेकर लिखी गई मेरी रिपोर्ट सशस्त्र किसान संघर्ष के इलाके में चार दिन काफी चर्चित हुई और जनमत में प्रकाशित संग्रहणीय सामग्रियों में एक बनी। राजकिशोर, हरिवंश और नीलाभ जैसे महत्वपूर्ण हिंदी बौद्धिकों ने इसे पढ़कर जनमत में अपनी प्रतिक्रियाएं भेजीं। अमेरिका से अंग्रेजी कवि, उपन्यासकार अमिताभ कुमार ने इसी रिपोर्ट पर जनमत में अपनी पहली चिट्ठी भेजी और बाद में यह हमारी स्थायी मैत्री का आधार बना। बांग्ला में हुए इसके अनुवाद को भी काफी प्रशंसा मिली, हालांकि मगही के कुछ गीतों के बांग्लाकरण में अर्थ का अनर्थ हो गया था। पहली बार हाथों में घातक हथियार थामने की सनसनी, अजीब समय और अटपटी जगहों में अजनबी लोगों से मुलाकात का रोमांच इस यात्रा का सिर्फ एक पहलू था। इसकी सबसे बड़ी बात थी भारत के सबसे गरीब ग्रामीण तबकों में खदबदाते बागी असंतोष, उनकी विद्रोही चेतना से एक ऐसे नौजवान का साक्षात्कार, जिसके पास अपने अनुभवों को आम दायरे में लाने की ख्वाहिश थी, और इन्हें बयान करने की कोई रटी-रटाई शब्दावली नहीं थी। भारतीय समाज में सबसे कम कमाई करने वाले, सबसे उत्पीड़ित, थके, पिछड़े और शिक्षा से वंचित तबके में एक विस्फोटक शक्ति और जीवन की एक गहरी समझ मौजूद है, इसका आभास मुझे उसी समय हुआ था। इसी का असर था, जो मुझे शहरी जीवन छोड़ कर गांव की ओर लौट जाने में कोई हिचक नहीं हुई। यह बात और है कि समय और दूरी ने इस तबके के साथ मेरे लगाव को अभी महज एक नोस्टैल्जिया तक सिमटा दिया है।
: गुंडे का इंटरव्यू और दंगे की एक शाम : अक्टूबर-नवंबर 1989 में आम चुनावों के लिए माहौल बनना शुरू हुआ। आईपीएफ ने पहली बार इस चुनाव में पूरी ताकत से उतरने का फैसला किया था। पार्टी ढांचे की ओर से जनमत को फीडबैक यह मिला कि पत्रिका के सारे वितरक चुनाव अभियान में जुटे होंगे लिहाजा इस दौरान न तो पत्रिका बिक पाएगी और न वसूली हो पाएगी। जनमत संपादक मंडल के सामने भी यह सवाल था कि पार्टी की इतनी बड़ी पहलकदमी में अपनी तरफ से वह क्या योगदान करे। लिहाजा फैसला हुआ कि दो महीने के लिए पत्रिका का प्रकाशन स्थगित कर दिया जाए और इस बीच टेब्लॉयड साइज में चार पन्नों का अखबार निकाला जाए, जो हो तो प्रचार सामग्री लेकिन इतनी प्रोपगंडा नुमा न हो कि आम पाठक उसे हाथ भी न लगाना चाहें। इस रणनीति के तहत पूरी टीम तितर-बितर कर दी गई। रामजी राय की देखरेख में प्रदीप झा और संतलाल को अखबार छापने की जिम्मेदारी मिली। महेश्वर और इरफान एक प्रचार फिल्म बनाने में जुटे। विष्णु राजगढ़िया को जहानाबाद, पटना और नालंदा के चुनाव क्षेत्रों को कवर करने भेजा गया और मुझे पुराने शाहाबाद जिले के चार संसदीय क्षेत्रों आरा, विक्रमगंज, सासाराम और बक्सर का चुनाव देखने के लिए कहा गया। इस फैसले की विचारधारा और राजनीति चाहे जितनी भी मजबूत रही हो, लेकिन इसके बाद चीजों को पटरी पर लाने में काफी समय लगा। खासकर इसके करीब डेढ़ साल बाद जब साप्ताहिक रूप में पत्रिका का प्रकाशन बंद करने का फैसला हुआ तो लगा कि इसमें कुछ न कुछ भूमिका 1989 के चुनावों में टीम बिखेरने की भी जरूर रही होगी।
बिहार की जमीनी राजनीति या रीयल पोलिटिक किस चिड़िया का नाम है, इसका अंदाजा मुझे पहली बार इस चुनावी सक्रियता के दौरान ही लगा। इसकी शुरुआत मैंने एक बौद्धिक रिपोर्टर के रूप में की थी, लेकिन इसका अंत होते-होते मैं बाकायदा एक जमीनी कायर्कर्ता बन चुका था। आरा में अपनी रिहाइश के दूसरे-तीसरे दिन ही मुझे विश्वनाथ यादव का इंटरव्यू करना पड़ा, जो शहर का एक माना  हुआ गुंडा था और कई तरह की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। आईपीएफ का प्रभाव नक्सल आंदोलन का मूल आधार समझे जाने वाले दलितों में था और मध्यवर्ती जातियों में कोइरी बिरादरी का भी उसे अच्छा समर्थन प्राप्त था। चुनाव में जीत-हार यादवों के एक हिस्से के समर्थन पर निर्भर करती थी, लिहाजा पार्टी हर कीमत पर उन्हें पटाने में जुटी थी। विश्वनाथ यादव से नजदीकी इसी रणनीति का एक हिस्सा थी। वह बाकायदा एक गुंडा है, इसका कोई अंदाजा मुझे नहीं था। अपनी समझ से चुनाव से जुड़े काफी आसान सवाल मैंने उससे पूछे, लेकिन यह अनुभव उसके लिए इतना विचित्र था कि उससे कुछ बोलते नहीं बना। यह जानकारी मुझे बहुत बाद में हुई कि आरा में उस चुनाव के दौरान कैसे-कैसे लोग के साथ मैंने इतनी आस्था से काम किया था। शराब की दुकान चलाने वाले, सिनेमा का टिकट ब्लैक करने वाले, तिनतसवा खेलाने वाले, ट्रेन से सामान उठाकर भाग जाने वाले, रंगदारी टैक्स वसूलने वाले। ऐसे-ऐसे लोग, जिन्हें लाइन पर लाने या पार्टी से बाहर करने में मात्र डेढ़ साल बाद मेरे पसीने छूट गए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आरा शहर में वह चुनाव एक जन आंदोलन था।
हुआ गुंडा था और कई तरह की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। आईपीएफ का प्रभाव नक्सल आंदोलन का मूल आधार समझे जाने वाले दलितों में था और मध्यवर्ती जातियों में कोइरी बिरादरी का भी उसे अच्छा समर्थन प्राप्त था। चुनाव में जीत-हार यादवों के एक हिस्से के समर्थन पर निर्भर करती थी, लिहाजा पार्टी हर कीमत पर उन्हें पटाने में जुटी थी। विश्वनाथ यादव से नजदीकी इसी रणनीति का एक हिस्सा थी। वह बाकायदा एक गुंडा है, इसका कोई अंदाजा मुझे नहीं था। अपनी समझ से चुनाव से जुड़े काफी आसान सवाल मैंने उससे पूछे, लेकिन यह अनुभव उसके लिए इतना विचित्र था कि उससे कुछ बोलते नहीं बना। यह जानकारी मुझे बहुत बाद में हुई कि आरा में उस चुनाव के दौरान कैसे-कैसे लोग के साथ मैंने इतनी आस्था से काम किया था। शराब की दुकान चलाने वाले, सिनेमा का टिकट ब्लैक करने वाले, तिनतसवा खेलाने वाले, ट्रेन से सामान उठाकर भाग जाने वाले, रंगदारी टैक्स वसूलने वाले। ऐसे-ऐसे लोग, जिन्हें लाइन पर लाने या पार्टी से बाहर करने में मात्र डेढ़ साल बाद मेरे पसीने छूट गए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आरा शहर में वह चुनाव एक जन आंदोलन था।
मुसलमान मेहनतकश वर्गों की ऐसी संघर्षशील एकता और ऐसी एकजुट राजनीतिक चेतना, जिसका जिक्र उत्तर भारत में मुझे देखने को दूर, कभी कहीं सुनने या पढ़ने तक को नहीं मिला। इसका असर आरा शहर पर भी पड़ा। बिहार और पूरे देश में माहौल बहुत ही खराब होने के बावजूद मैंने इस शहर में करीब दो महीने की अपनी उस रिहाइश में कोई सांप्रदायिक नारा तक लगते नहीं सुना। सांप्रदायिकता की दृष्टि से भी 1989 के उन अंतिम महीनों का कोई जोड़ खोजना मुश्किल है। आजाद भारत के इतिहास का वह अकेला दौर है, जब कांग्रेस और बीजेपी लगभग बराबरी की ताकत से हिंदू वोटों के लिए लड़ रही थीं और इसके लिए किसी भी हद तक जाने में उन्हें कोई गुरेज नहीं था। सरकारी मशीनरी के फासिज्म की हद तक सांप्रदायिक हो जाने का जो मामला पिछले कुछ सालों से गुजरात में देखा जा रहा है, उससे कहीं बुरा हाल इसका मैंने बिहार में, खासकर इसके सासाराम शहर में देखा है। चुनावी माहौल में एक दिन खबर फैली कि शहर के फलां मठ पर एक बहुत बड़ा हिंदू जमावड़ा होने वाला है। मैंने देखा तो नहीं लेकिन सुनने में आया कि पूड़ियों के लिए रात से ही कई कड़ाह चढ़े और उनसे सुबह तक पूड़ियां निकलती रहीं। हमारा चुनाव कार्यालय शहर के मुस्लिम इलाके में था। दोपहर में पार्टी की प्रचार जीप शहर में- दंगाइयों होशियार आईपीएफ है तैयार- जैसे नारे लगाती निकली। जीप में पीछे मैं भी बैठा हुआ था…और अचानक चारो तरफ से हम विराट हिंदू जुलूस से घिर गए। गनीमत थी कि शहर में ज्यादातर लोगों को आईपीएफ के बारे में कुछ खास मालूम नहीं था। हमने माइक बंद किया, चुपचाप जीप से उतरे और किनारे खड़े हो गए। जुलूस मुस्लिम इलाके में पहुंच कर आराम से खड़ा हो गया और खुलेआम हाथों में कट्टा-चाकू लिए, सिर पर गेरुआ बंडाना बांधे कुछ लोग किनारे के मुस्लिम मुहल्लों में घुस गए। फिर भीड़ के बीच से रास्ता बनाकर एक आदमी को कंधे पर उठाए कुछ लोग चिल्लाते हुए दौड़े कि मुसलमानों ने इस आदमी को बम मार दिया है। उस पर उड़ेला गया डिब्बा भर लाल रंग कुछ ज्यादा ही लाली फैलाए हुए था। फिर दुकानें लूटने का सिलसिला शुरू हुआ। बेखटके शटर तोड़-तोड़ कर लोग टीवी, रेडियो, घड़ियां वगैरह ले जा रहे थे। जीप किसी तरह मोड़ कर गलियों-गलियों निकलने में हमें एक घंटा लग गया। लेकिन अपने चुनाव कार्यालय हम फिर भी नहीं पहुंच सकते थे। चिंता थी कि शाहनवाज जी और दूसरे मुस्लिम साथी वहां किस हाल में होंगे।
मुझे तो सासाराम के रास्ते भी नहीं पता थे। मैं वहां गया ही पहली बार था। रजाई की दुकान करने वाले एक साथी के पीछे-पीछे हम किसी तरह वहां पहुंचे तो दफ्तर का माहौल भी सांप्रदायिक होने के करीब था। कुछ समर्थक जोर-शोर से यह चर्चा कर रहे थे कि भला मुसलमानों को जुलूस पर बम मारने की क्या जरूरत थी। शाहनवाज जी स्थानीय वकील थे और दबंग पठान बिरादरी से आते थे। आईपीएफ से उनका संपर्क पिछले दो-तीन महीनों का ही था। उनके साथ दो-तीन और मुस्लिम समर्थक भी थे। हमने अलग से उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि घर की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वह ज्यादा भीतर पड़ता है। किसी तरह बाहर-बाहर ही पड़ोस के किसी मुस्लिम गांव में निकल जाएं तो मामला निपट जाएगा। हम लोगों ने ऐसा ही किया। सारे मुस्लिम साथी बीच में बैठे। बाकी लोग जीप में किनारे-किनारे लद गए और इर्द-गिर्द उठ रहे शोर के बीच किसी तरह शाम के झुटपुटे में हम शहर से बाहर निकल गए। दूर जाने पर जगह-जगह से उठता घना, काला ऊंचा धुआं शहर में जारी विनाश की कमेंट्री करता लगा। बाद में पता चला, शेरशाह सूरी की स्मृतियों से जुड़े शहर के कई ऐतिहासिक स्मारक उस दिन की दंगाई आग में स्वाहा हो गए और शहर के सीमावर्ती इलाकों पर नजर गड़ाए लोगों ने मुस्लिम परिवारों के वहां से हटते ही उनपर कब्जा कर लिया।
: दिल्ली के लिए चालान कटा : तय योजना के मुताबिक जनमत के लिए पहले दो हफ्तों में चुनावी कवरेज पूरा करके मुझे आरा में ही रुक जाना था। वहां पार्टी सेक्रेटरी दीना जी थे, जिनके बारे में दो साल पहले मैंने बम की शिक्षा शीर्षक से एक पोस्ट लिखी थी। एक ऐसे हंसमुख, जिंदादिल योद्धा, जिनकी छाप मन से कभी नहीं जाएगी। विभाजन के समय पूर्वी बंगाल से आकर इस तरफ बसे एक बड़े जमींदार परिवार के दीना जी का असली नाम अरूप पॉल था। नक्सल आंदोलन के शुरुआती दौर में ही इसके साथ उनका जुड़ाव बना था और कॉमरेड विनोद मिश्र के अंगरक्षक के रूप में वे सत्तर के दशक में चीन हो आए थे। भोजपुर में एक दशक से ज्यादा समय तक अंडरग्राउंड रहने के बाद उन्होंने चुनावी दौर में ही खुले में काम करना शुरू किया था, लेकिन बोली-बानी के रचाव और जिले के चप्पे-चप्पे तक उनकी पहुंच के चलते आम लोग उनको किसी ठेठ भोजपुरिया की तरह ही जानने लगे थे।
बिना किसी विचार-विमर्श के दीना जी ने आरा शहर में चुनाव प्रचार के नए रूपों की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी और मतदान संपन्न होने के बाद काउंटिंग हॉल में रह कर काउंटिंग का काम देखने का भी। इलाहाबाद में मेरी छात्र राजनीति की पृष्ठभूमि शायद उनके इस फैसले की वजह रही हो। लेकिन चुनाव नतीजे आते, इसके पहले ही एक बहुत ही भयानक घटना भोजपुर में घटित हो गई। सोन नदी के किनारे तरारी ब्लॉक के बिहटा गांव में स्थानीय भूस्वामियों का वहां के मजदूरों के साथ काफी समय से विवाद चल रहा था। इसका एक जातिगत पक्ष भी था। ब्लॉक प्रमुख ज्वाला सिंह के नेतृत्व में गांव के राजपूतों की तरफ से यह नियम बनाया गया कि पिछड़ी और दलित जातियों के टोलों में बाहर से जो भी रिश्तेदार आएंगे, उनका नाम-पता उन्हें एक रजिस्टर में दर्ज करना होगा। कहा गया कि गांव में नक्सलियों की आवक रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है।
यह तनाव चुनाव के दिन गैर-क्षत्रिय मतदाताओं को बूथों से भगाने और फिर प्रतिक्रिया में मारपीट के रूप में जाहिर हुआ। इसका अंत यह हुआ कि पास के ही एक गांव में मौजूद लिबरेशन के एक सशस्त्र दस्ते ने दिन में ही निकलकर मारपीट कर रहे लोगों पर फायर झोंक दिया, जिसमें तीन-चार लोगों की मौत हो गई। आरा में हम लोगों को इस घटना की सूचना थी और पार्टी ने आसपास के  गांवों में अपने समर्थकों को जवाबी हमले से सजग रहने को भी कह दिया था। लेकिन भोजपुर में इससे पहले राजनीतिक घटनाक्रम में सामूहिक जनसंहार की कोई घटना नहीं हुई थी, लिहाजा पार्टी स्थिति की गंभीरता का सही अनुमान नहीं लगा सकी। काउंटिंग हॉल में मेरी ड्यूटी लगने के बाद दो दिन और एक रात तो मुझे देश-दुनिया का कुछ पता नहीं रहा। वह चुनाव हम लोग जीत गए। किसान नेता रामेश्वर प्रसाद भारत के नक्सली आंदोलन के पहले सांसद बन गए। लेकिन इसकी खुशी काउंटिंग हॉल से बाहर निकलते ही काफूर हो गई, जब पता चला कि बिहटा में तीस से ज्यादा पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई है और उनकी लाशें पास की नहर में दूर तक उतरा रही हैं।
गांवों में अपने समर्थकों को जवाबी हमले से सजग रहने को भी कह दिया था। लेकिन भोजपुर में इससे पहले राजनीतिक घटनाक्रम में सामूहिक जनसंहार की कोई घटना नहीं हुई थी, लिहाजा पार्टी स्थिति की गंभीरता का सही अनुमान नहीं लगा सकी। काउंटिंग हॉल में मेरी ड्यूटी लगने के बाद दो दिन और एक रात तो मुझे देश-दुनिया का कुछ पता नहीं रहा। वह चुनाव हम लोग जीत गए। किसान नेता रामेश्वर प्रसाद भारत के नक्सली आंदोलन के पहले सांसद बन गए। लेकिन इसकी खुशी काउंटिंग हॉल से बाहर निकलते ही काफूर हो गई, जब पता चला कि बिहटा में तीस से ज्यादा पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई है और उनकी लाशें पास की नहर में दूर तक उतरा रही हैं।
जनमत में अपने रुटीन पर वापस लौट आने के बाद भी जाती तौर पर मेरे कई महीने भोजपुर और उसमें भी बिहटा के इर्दगिर्द घूमते-टहलते बीते। इस बीच विष्णु राजगढ़िया को दिल्ली से रिपोर्टिंग और वहां राजनीतिक कामकाज में रामेश्वर जी की मदद की भूमिका दी गई। इससे जनमत में मैनपॉवर थोड़ा कम हो गया और टीम के भीतर जिस एक व्यक्ति से मेरा कोऑर्डिनेशन सबसे अच्छा था, उसकी कमी भी मुझे बहुत खली। विष्णु खुद में वन मैन आर्मी किस्म के इंसान हैं और जब वे आसपास होते हैं तो जिंदगी काफी हल्की लगने लगती है। लेकिन सिर्फ छह महीने में यह नई व्यवस्था भी गड़बड़ाने लगी। शायद दिल्ली में विष्णु की राजनीतिक व्यस्तताएं काफी बढ़ गई थीं और जनमत में उनका आउटपुट संतोषजनक नहीं रह गया था। नतीजा यह हुआ कि 1990 का जून आते-आते उन्हें पटना रवानगी का हुक्म हुआ और उनकी जगह पर दिल्ली के लिए मेरा चालान काट दिया गया।
दिल्ली आने से मेरा कोई विरोध नहीं था। बल्कि यह सोचकर अच्छा ही लगा कि सोच-समझ को नए धरातल पर ले जाने में शायद इससे कुछ मदद मिले। लेकिन भोजपुर ने कोई एक ऐसी लुत्ती मन में लगा दी थी कि महानगर के अकेलेपन के साथ तालमेल बिठाना कुछ ज्यादा ही मुश्किल लग रहा था। यहां बतौर सांसद रामेश्वर जी को मिले फ्लैट 40, मीनाबाग के ही एक कमरे से दीपंकर भट्टाचार्य (अभी सीपीआईएमएल के महासचिव) लिबरेशन निकालते थे, आशुतोष उपाध्याय (अभी हिंदुस्तान में असिस्टेंट एडिटर और बुग्याल ब्लॉग के कर्ताधर्ता) इस काम में उन्हें सहयोग देते थे और शाहिद अख्तर (फिलहाल पीटीआई भाषा के वरिष्ठ पत्रकार) रामेश्वर जी के संसदीय सहायक की भूमिका निभाते थे। यहां गणेशन जी (असली नाम कॉमरेड श्रीनिवासन) भी थे, जो नक्सल आंदोलन की शुरुआत से ही इसकी अगुआ पांत में थे और तमिलनाडु के संगठन में कुछ समस्या पैदा हो जाने के बाद से पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे थे। यहां वैचारिक एकता के बावजूद भावना के स्तर पर सभी की अलग-अलग दुनिया थी और जनमत के काम में मैं यहां बिल्कुल तनहा था। लेकिन संयोग से यही वह नाटकीय समय था जब 40, मीनाबाग के बमुश्किल दो किलोमीटर के दायरे में अगले डेढ़ दशक के लिए भारत की राजनीति का खाका रचा जा रहा था।
: मंडल-कमंडल की राजनीति : अगर आप कभी दिल्ली में विज्ञान भवन के सामने से गुजरे हों तो शायद उसके ठीक सामने बने दोतल्ला एमपी फ्लैटों पर भी आपकी नजर गई हो। 40, मीनाबाग इन्हीं में से एक फ्लैट का पता है। इसके बिल्कुल पास में नेशनल म्यूजियम चौराहे के दूसरी तरफ पड़ने वाला बंगला रामविलास पासवान का है, जिसके सामने से होते हुए सिर्फ दो सौ कदम चलकर आप 10, जनपथ पहुंच जाएंगे। यह जगह 1990 में आज जितनी चर्चित भले न रही हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का सबसे खास पता यह तब भी हुआ करती थी। एम.जे. अकबर उस समय कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे और आम रिवाज के मुताबिक हर खास प्रेस ब्रीफिंग के बाद प्रेस हैंडआउट पत्रकारों के पास तक पहुंचाने के बजाय उसकी प्रतियां हवा में उछाल दिया करते थे। मीडिया के प्रति कांग्रेस की रुखाई का यह हाल तब था जब संसद में उसकी सीटें 412 के आकाश से गिरकर सीधे 191 के पाताल में पहुंच गई थीं। दरअसल, कांग्रेसी नेताओं को पूरा यकीन था कि उनकी जगह लेने वाली वीपी सिंह सरकार 1977 की मोरारजी सरकार से भी ज्यादा मरियल थी और केंद्र में उनकी वापसी कुछ गिने-चुने महीनों 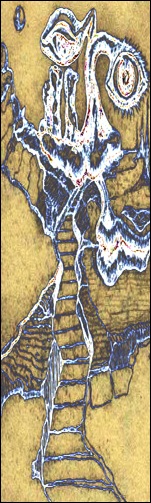 बाद केक-वाक सरीखी ही होने वाली थी। यह बात और है कि इतिहास ने इस बार उन्हें काफी बेरहमी से गलत साबित किया।
बाद केक-वाक सरीखी ही होने वाली थी। यह बात और है कि इतिहास ने इस बार उन्हें काफी बेरहमी से गलत साबित किया।
मेरे दिल्ली पहुंचने के दो-तीन महीने भीतर की ही बात है। ठीक से याद नहीं आ रहा कि महीना जुलाई था या अगस्त। हरियाणा में मेहम नाम की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे थे। इधर बीजेपी, उधर लेफ्ट के समर्थन वाली संयुक्त मोर्चा सरकार में किंग मेकर कहलाने वाले चौधरी देवीलाल के बड़े बेटे ओमप्रकाश चौटाला इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे। उनकी पुरानी पार्टी लोकदल के ही एक बागी उम्मीदवार आनंद डांगी ने उन्हें चुनौती दे रखी थी। इस चुनाव को कवर करने के लिए ही मैंने हरियाणा की अपनी पहली यात्रा की थी। बाद में पता चला कि मेहम में कर्फ्यू जैसी स्थिति बनाकर और लगभग सारे ही बूथों पर कब्जा करके चौटाला ने चुनाव जीत लिया। सरकार के भीतर से इसके खिलाफ पहली आवाज उठाने वाले यशवंत सिन्हा थे, जो तीन-चार महीनों बाद चंद्रशेखर के पीछे-पीछे देवीलाल के साथ जाने वाले शायद पहले नेता भी बने।
अजीब समय था। 1977 में जब जनता पार्टी सरकार बनी थी तब मैं बच्चा ही था, लेकिन सुना है, उसका हाल भी कमोबेश जनता दल के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार जैसा ही था। हम लोग आईएनएस बिल्डिंग के सामने संजय चौरसिया की चाय की दुकान पर जनता दल के छुटभैया नेताओं से गपास्टक करते तो वे लगभग लगातार ही वीपी सिंह को गालियां देते नजर आते। आस्तीन का सांप है, किसी को भी टिकने नहीं देगा। जो भी इसका साथ देगा, उसे बेइज्जत करने में इसको एक मिनट नहीं लगेगा। मेहम कांड को लेकर जनता दल के भीतर बहस शुरू हुई तो चौधरी देवीलाल ने अपने एक इंटरव्यू में अरुण नेहरू को हाथी कह दिया। अरुण नेहरू वीपी सिंह से अड़ गए कि सरकार में आप अब या तो देवीलाल को रख लें या मुझे ही रख लें। अगस्त में जारी इस बवाल का पहला अध्याय सितंबर के पहले ही हफ्ते में उप प्रधानमंत्री पद से देवीलाल की विदाई के साथ समाप्त हुआ।
जहां तक ध्यान आता है, 7 सितंबर 1990 को बोट क्लब पर वीपी सिंह को जवाब देने के लिए देवीलाल, कांशीराम और प्रकाश सिंह बादल की एक संयुक्त रैली हुई। बहुत ही उपद्रवी और भयानक किस्म की जाट प्रधान रैली। सनसनी थी कि शरद यादव तमाम पिछड़ा सांसदों के साथ अभी आते ही होंगे। इब तो यहीं खड़े-खड़े वीपी सिंह की सरकार पलट जाएगी और राजा का बाजा बजा दिया जाएगा। छुटभैये नेता भाषण पर भाषण दिए जा रहे थे ताकि चौस्साब की तकरीर थोड़ी देर से ही शुरू हो और इसकी शुरुआत वे सरकार पलटने की घोषणा के साथ ही कर सकें। लेकिन शरद नहीं आए तो नहीं आए। राजनीतिक कद उनका तब भी कमोबेश अभी जितना ही था, लेकिन जनता दल के भीतरी समीकरण कुछ इस तरह के बने हुए थे कि यूपी और बिहार के पिछड़ावादी नेता देवीलाल के पीछे एकजुट थे और संसद में सेकंड इन कमांड के रूप में उनका नेतृत्व शरद यादव के पास था।
करीब 1 बजते-बजते रैली में आए लोगों को और खासकर रैली कवर करने गए पत्रकारों को पता चल गया कि पर्दे के पीछे खेल हो चुका है। बारह साल पहले मोरारजी देसाई ने चौधरी चरण सिंह की गैर-सवर्ण राजनीति को पैदल करने के लिए जिस मंडल कमिशन का गठन किया था, उसकी बरसों से धूल खा रही रिपोर्ट की अनुशंसाएं लागू करने का फैसला वीपी सिंह ने देवीलाल को पैदल करने के लिए इन्हीं दो-तीन दिनों में कर लिया था। सभी लोग समझ चुके थे कि उस दिन बाजा असलियत में वीपी का नहीं, किसी और का ही बजा था। रैली में फ्रस्टेशन का माहौल था। काफी तोड़फोड़ भी हुई। बोट क्लब पर राजनीतिक रैलियां बंद होने की पृष्ठभूमि दरअसल ताऊ की इस रैली ने ही तैयार की थी। शाम को अपनी रपट का मसाला जुटाने और ताऊ का हाल पता करने मैं उनके आवास 1, वेलिंगटन क्रिसेंट रोड गया। विशाल बंगले के बाहर मारुति 800 गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी, जो तब तक नव धनाढ्य तबकों की पहचान मानी जाती थी। किसी बड़े अखबार का ठप्पा अपने पर था नहीं। नेताओं के बंगलों पर जाने में दिक्कत तो मुझे हमेशा ही होती थी। इस बार भी हुई लेकिन जैसे-तैसे भीतर चला गया तो वहां पता चला- ताऊ तो अंटा (अफीम की गोली) लेकर सो गया है। तू ऐसा कर, आ जा कल-परसों कभी भी। हो जावेगी बात दो-चार मिन्ट।
अगले दिन तक दिल्ली की सियासी शतरंज पर ताऊ की हैसियत वजीर तो क्या प्यादे की भी नहीं रह गई थी। कुछ लोगों ने इसकी व्याख्या 1, वेलिंगटन क्रिसेंट रोड की मनहूसियत के रूप में की और इसका नतीजा यह हुआ कि इसके बाद से बड़े नेताओं ने इस शानदार बंगले में रहना ही बंद कर दिया। बहरहाल, 8 सितंबर को संसद की अनेक्सी में लालू यादव के आने की चर्चा थी। देवीलाल के समर्थक वहां जमा थे। उन्हें उम्मीद थी कि ताऊ ने जिस आदमी के लिए वीपी सिंह से सीधे पंगा लिया, उनके खासुलखास रामसुंदर दास के हाथ से बिहार की गद्दी छीन कर उसे सौंप दी, कम से कम वह तो इस मौके पर ताऊ का साथ जरूर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होना था। अनेक्सी में किसी ताऊ समर्थक ने नारेबाजी की शक्ल में जैसे ही लालू यादव पर गद्दारी की तोहमत लगाई, वे हाथ में जूता लेकर दो कदम आगे बढ़ आए- हरे स्साला, मारेंगे जुत्ता से दिमाक सही हो जाएगा। यह उत्तर भारत में पहली बार सच्चे अर्थों में एक पिछड़ा उभार की शुरुआत थी, जिसके निशाने पर पारंपरिक ऊंची जातियों के अलावा अभी तक उत्तर भारत में अ-सवर्ण राजनीति का नेतृत्व करते आ रहे जाट भी थे।
इसके ठीक अगले दिन, या शायद 10 सितंबर 1990 को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने अक्टूबर महीने में सोमनाथ से राम रथयात्रा शुरू करने और 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंच कर बाबरी मस्जिद की जगह भव्य राम मंदिर बनाने के लिए कारसेवा शुरू कर देने की घोषणा कर दी। उस समय अखबारों का हल्ला देखकर लगता था कि यह तो शुद्ध बकवास है। कहां धाव-धूप कहां मांग-टीक। अभी साल भर पहले तक तो बोफोर्स की मारी कांग्रेस देश भर में मंदिर बनवाने का माहौल बनाए हुए थी। अब मंडल का हल्ला शुरू हुआ तो ये सज्जन अपना अलग चनाजोर गरम बेचने निकल पड़े। इतना तो साफ था कि मंडल से शुरू हुआ अगड़ा-पिछड़ा विभाजन हिंदू एकता वाली बीजेपी की मुहिम के खिलाफ जाएगा। इसे रोकने के लिए उसके नेता कुछ न कुछ तो करेंगे ही। लेकिन इसके ggजवाब में वे इतने आनन-फानन में एक आक्रामक अभियान छेड़ देंगे, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। किसी मुहिम का राजनीतिक औचित्य होना एक बात है, लेकिन यह काम क्या इस तरह बच्चों की डिबेट की तर्ज पर तुर्की-ब-तुर्की स्टाइल में संभव है।
बीजेपी का दफ्तर उस समय पत्रकारों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ करता था। पार्टियों की प्रेस ब्रीफिंग का टाइम आम तौर पर चार बजे का ही होता था लेकिन बीजेपी दफ्तर में ब्रीफिंग साढ़े चार बजे हुआ करती थी। सबसे खास बात यह थी कि बीजेपी की ब्रीफिंग में उस समय हर दिन मिठाई मिलती थी। लिहाजा कांग्रेस और जनता दल की बीट कवर करने वाले रिपोर्टर भी उधर से थोड़ा जल्दी  निकल कर बीजेपी कार्यालय पहुंचने की कोशिश करते थे। थोड़ी दूर स्थित वीएचपी कार्यालय पर ब्रीफिंग रेगुलर नहीं होती थी लेकिन जब होती थी तो मिठाइयां वहां तीन-चार पीस मिलती थीं। आडवाणी की मंदिर घोषणा के ठीक बाद वीएचपी दफ्तर में महंथ अवैद्यनाथ और अशोक सिंघल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पत्रकार भूमिका में होने के बावजूद एक कार्यकर्ता की असाध्य खुजली के साथ मैंने उनसे पूछा कि आप लोग इस समाज के बुजुर्ग लोग हैं, मंदिर मुद्दे पर देशव्यापी यात्रा से समाज में उत्तेजना फैलेगी, लोग मारे जाएंगे, इस बारे में क्या आपने कुछ सोचा है। अवैद्यनाथ ने इसका जवाब घांव-मांव ढंग से दिया- हमको इससे कोई मतलब नहीं, जो होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, वैसे आप किस अखबार से हैं। उनके जवाब से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगली सीट पर बैठे कई स्वनामधन्य पत्रकार मेरे साथ गाली-गलौज पर उतारू हो गए और यूएनआई वार्ता से जुड़े मेरे मित्र विनोद विप्लव को बीच-बचाव करना पड़ा।
निकल कर बीजेपी कार्यालय पहुंचने की कोशिश करते थे। थोड़ी दूर स्थित वीएचपी कार्यालय पर ब्रीफिंग रेगुलर नहीं होती थी लेकिन जब होती थी तो मिठाइयां वहां तीन-चार पीस मिलती थीं। आडवाणी की मंदिर घोषणा के ठीक बाद वीएचपी दफ्तर में महंथ अवैद्यनाथ और अशोक सिंघल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पत्रकार भूमिका में होने के बावजूद एक कार्यकर्ता की असाध्य खुजली के साथ मैंने उनसे पूछा कि आप लोग इस समाज के बुजुर्ग लोग हैं, मंदिर मुद्दे पर देशव्यापी यात्रा से समाज में उत्तेजना फैलेगी, लोग मारे जाएंगे, इस बारे में क्या आपने कुछ सोचा है। अवैद्यनाथ ने इसका जवाब घांव-मांव ढंग से दिया- हमको इससे कोई मतलब नहीं, जो होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, वैसे आप किस अखबार से हैं। उनके जवाब से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगली सीट पर बैठे कई स्वनामधन्य पत्रकार मेरे साथ गाली-गलौज पर उतारू हो गए और यूएनआई वार्ता से जुड़े मेरे मित्र विनोद विप्लव को बीच-बचाव करना पड़ा।
मंडल और मंदिर के नारों के बीच अपनी अलग पहचान के साथ सीपीआई एमएल लिबरेशन ने 8 अक्टूबर 1990 को न सिर्फ अपनी बल्कि दिल्ली की भी अब तक की विशालतम रैलियों में से एक का आयोजन किया। समाज में संकीर्ण यथास्थितिवादी पहचानों के बल पर राजनीति करने वाली शक्तियों के सामने एक उभरती वाम राजनीतिक शक्ति की ओर से यह बड़ी चुनौती थी। लेकिन इसकी तैयारियों के क्रम में ही यह स्पष्ट हो गया था कि पार्टी के लिए समाज में बन रहे नए तनावों का सामना करना बहुत ही मुश्किल होगा। दिल्ली और कुछ अन्य महानगरों में मंडल अनुशंसाओं के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हो रहे थे। खास तौर पर बिहार में इसका जवाब मंडल समर्थक उग्रता के जरिए दिया जा रहा था। सीपीआई एमएल लिबरेशन का स्टैंड मंडल अनुशंसाओं के पक्ष में था, हालांकि इसके साथ में वह अपनी यह व्याख्या भी जोड़ती थी कि इससे समाज में कोई बुनियादी बदलाव नहीं होने वाला है। ऐसे उत्तेजना भरे माहौल में बीजेपी ने देश भर में अपना कमंडल घुमाकर उग्र सवर्ण प्रतिक्रिया को उसमें समेट लेने की पूरी कोशिश की। वह शायद अपनी मुहिम में कामयाब भी हो जाती लेकिन 1991 में हुए आम चुनावों के ऐन बीच में राजीव गांधी की हत्या से उपजी असुरक्षा और सहानुभूति की लहर ने उसका खेल पूरा नहीं होने दिया और 89 सीटों से आगे बढ़कर उसकी गाड़ी 120 पर अटक गई।
….जारी…
 चंद्रभूषण को उनके जानने वाले चंदू या चंदू भाई के नाम से पुकारते हैं. चंदू भाई हिन्दी के वरिष्ठ पत्रकार हैं. इलाहाबाद, पटना और आरा में काम किया. कई जनांदोलनों में शिरकत की. नक्सली कार्यकर्ता भी रहे. ब्लाग जगत में इनका ठिकाना ”पहलू” के नाम से जाना जाता है. सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर बहुआयामी सरोकारों के साथ प्रखरता और स्पष्टता से अपनी बात कहते हैं. इन दिनों दिल्ली में नवभारत टाइम्स से जुड़े हैं. चंदू भाई से यह डायरी लिखवाने का श्रेय वरिष्ठ पत्रकार और ब्लागर अजित वडनेरकर को जाता है. अजित जी के ब्लाग ”शब्दों का सफर” से साभार लेकर इस डायरी को यहां प्रकाशित कराया गया है.
चंद्रभूषण को उनके जानने वाले चंदू या चंदू भाई के नाम से पुकारते हैं. चंदू भाई हिन्दी के वरिष्ठ पत्रकार हैं. इलाहाबाद, पटना और आरा में काम किया. कई जनांदोलनों में शिरकत की. नक्सली कार्यकर्ता भी रहे. ब्लाग जगत में इनका ठिकाना ”पहलू” के नाम से जाना जाता है. सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर बहुआयामी सरोकारों के साथ प्रखरता और स्पष्टता से अपनी बात कहते हैं. इन दिनों दिल्ली में नवभारत टाइम्स से जुड़े हैं. चंदू भाई से यह डायरी लिखवाने का श्रेय वरिष्ठ पत्रकार और ब्लागर अजित वडनेरकर को जाता है. अजित जी के ब्लाग ”शब्दों का सफर” से साभार लेकर इस डायरी को यहां प्रकाशित कराया गया है.