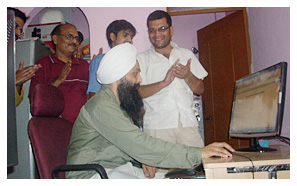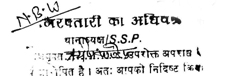मृणाल पांडेय के आलेख ‘बदलती अखबारी दुनिया और पत्रकारिता की चुनौतियां‘ के जवाब में भड़ास4मीडिया के पास देश भर के सैकड़ों पत्रकारों ने अपने विचार भेजे हैं। जवाब हम देंगे सीरीज की शुरुआत संजय कुमार सिंह के आलेख से की गई थी। अब बेंगलोर के वेब जर्नलिस्ट दिनेश श्रीनेत ने मृणाल द्वारा उठाए गए बिंदुओं का एक-एक कर जवाब देने की कोशिश की है। जवाब हम देंगे सीरिज में आगे भी पाठकों के लेखों व विचारों को पेश किया जाएगा। –एडिटर, भड़ास4मीडिया
मृणाल पांडेय के आलेख ‘बदलती अखबारी दुनिया और पत्रकारिता की चुनौतियां‘ के जवाब में भड़ास4मीडिया के पास देश भर के सैकड़ों पत्रकारों ने अपने विचार भेजे हैं। जवाब हम देंगे सीरीज की शुरुआत संजय कुमार सिंह के आलेख से की गई थी। अब बेंगलोर के वेब जर्नलिस्ट दिनेश श्रीनेत ने मृणाल द्वारा उठाए गए बिंदुओं का एक-एक कर जवाब देने की कोशिश की है। जवाब हम देंगे सीरिज में आगे भी पाठकों के लेखों व विचारों को पेश किया जाएगा। –एडिटर, भड़ास4मीडिया
नोम चोमस्की को सही मानें या मृणाल पांडेय को !
मृणाल कहिन : कहने को कहा जा सकता है कि इंटरनेट, सर्च इंजिनों तथा ब्लॉग साइट्स के युग में मीडिया का कलेवर अब बदलेगा ही। और आज नहीं तो कल हिंदी पट्टी में भी लोगबाग नेट तथा केबल पर ही अखबार पढ़ेंगे। लेकिन क्या आप जानते हें कि आज भी इंटरनेट पर 85 प्रतिशत खबरों का स्रोत प्रिंट मीडिया ही है। वजह यह, कि सर्च इंजिन गूगल हो अथवा याहू, दुनियाभर में अपने मंजे हुए संवाददाताओं की बड़ी फौज तैनात करने की दिशा में अभी किसी इंटरनेट स्रोत ने खर्चा नहीं किया है। और वह करे भी, तो रातोंरात अखबार के कुशल पत्रकारों जैसी टीम वह खड़ी नहीं कर सकेंगे।
मेरा मत : यह बात पत्रकारिता के किसी छोटे-मोटे स्कूल से निकलने वाला स्टूडेंट कहता तो शायद अच्छा लगता, मगर मृणाल पांडेय जैसी ‘संपादक+लेखक+विचारक’ यह कह रही हैं तो आश्चर्य होता है। यथार्थ इतना एकतरफा नहीं होता। शायद उन्हें पोर्टल की अवधारणा के बारे में पता नहीं है। पोर्टल की शुरुआत इंटरनेट संजाल पर उपयोगी सूचनाओं को एक जगह लाने से हुई थी। मगर रायटर्स और एपी जैसी समाचार वायर्ड सर्विस देने वाली एजेंसियां तेजी से इंटरनेट को ध्यान में रखकर खुद को डेवलप कर रही हैं। किसी भी माध्यम का विकास एक संक्रमण काल से होकर कर गुजरता है। उसके बाद ही उसकी वास्तविक तस्वीर सामने आती है। क्या पता, आने वाले समय में एसोसिएटेड प्रेस या रायटर्स इंटरनेट पर सबसे बड़े समाचार नेटवर्क के रूप में सामने आ जाएं। संस्थानों का विकास एकरेखीय नहीं होता है। इलेक्ट्रानिक कंप्यूटर के अस्तित्व में आने से पहले आईबीएम काम कर रही थी। क्या वे बता सकती हैं कि किस अखबार के पास अपने संवाददाताओं की फौज है। वे सभी समाचार एजेंसियों पर निर्भर हैं। जहां तक बहु-संस्करणीय अखबारों के नेटवर्क की बात है तो ये उनके क्षेत्रीय कलेवर के चलते है, न कि खबरों के चयन के लिए। इस वक्त पूरी दुनिया की न्यूज इंडस्ट्री में खर्चे घटाने की कवायद चल रही है, पत्रकार हटाए जा रहे हैं, ब्यूरो बंद किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ गूगल जैसी हजारों वेब कंपनियां ब्लागों, वेबसाइटों, पोर्टलों को मुफ्त में पैदा करने की सुविधा देकर रोजाना लाखों नागरिकों को जर्नलिस्ट बना रही हैं और सूचना देने-लेने के नए माध्यमों को विकसित कर रही हैं।
मृणाल कहिन : बड़े अखबारों और वरिष्ठ संवाददाताओं से पाठक, नागरिक संगठन या सरकारें भले ही कई मुद्दों पर मतभेद रखें, इसमें शक नहीं कि युद्ध से लेकर बैंकिंग तक के घोटालों, रोमानिया तथा भारत से लेकर श्रीलंका तक में अलोकतांत्रिक घटनाओं तथा लोकतांत्रिक चुनावों और पर्यावरण तथा खाद्यसुरक्षा स्थिति की बाबत जन-जन तक बारीक जानकारियां पहुंचा कर मानवहित में विश्वव्यापी जनसमर्थन जुटाने का जो काम बड़े अखबारों के संवाददाताओं ने दुनिया भर में किया है, उसके बिना आज दुनिया में लोकतंत्र और मानवाधिकार काफी हद तक मिट चुके होते।
मेरा मत : वाह-वाह, एक नई बात पता चली! दुनिया में लोकतंत्र और मानवाधिकार की रक्षा के लिए जमीनी संघर्ष करने वाले जननेताओं और जनांदोलनों का कोई योगदान नहीं है? इसे बचाए रखा तो कुछ उद्योगपतियों की पूंजी से और लाभ के उद्येश्य से निकलने वाले अखबारों ने! इस बारे में अमेरिकी विचारक नोम चॉमस्की का मानना है कि मीडिया एक ऐसा बाजार तंत्र है जिसकी दिशा लाभ तय करता है। मालिक मीडिया की विषय वस्तु तय करता है, और यह प्रोपेगंडा किया जाता है कि इस विषय पर जनता के बीच सहमति है। वे बताते हैं कि किस तरह अमरीकी सरकार अपनी हमलावर कार्यवाहियों के लिए आम जनों की सहमति का ”उत्पादन” करती है। उनके ही शब्दों में- सहमति का ”उत्पादन” कई तरीकों से किया जाता है, जिनमें प्रमुख है मीडिया का अत्यंत चालाकी से इस्तेमाल। अब नोम चोमस्की को सही मानें या मृणाल पांडेय को ! जहां तक इंटरनेट की बात है तो उसने सिटिजन जर्नलिज्म जैसी क्रांतिकारी अवधारणा को सामने रखा है। खबर पढ़ने वाला अपनी राय दे सकता है, किसी मुद्दे पर अपना मत प्रदान कर सकता है और खुद लिख भी सकता है। दक्षिण कोरिया की वेबसाइट ‘ओह माई न्यूज’ का नारा था- ‘हर नागरिक एक रिपोर्टर है’। इस वेबसाइट ने 50 हजार से ज्यादा स्वतंत्र नागरिक पत्रकार तैयार किए और वहां के रुढ़िवादी राजनीतिक माहौल में हस्तक्षेप कर उसके खिलाफ जनमत तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। ब्लाग मीडिया के सामने एक नई चुनौती है। बहुत से ब्लागर्स ने लोकतांत्रिक या भागीदारी पत्रकारिता को चुनकर खुद को एक मुख्यधारा मीडिया के सामने विकल्प के तौर पर खड़ा किया है। दनिया के तमाम मीडिया विशेषज्ञ ब्लाग के विस्तार को सूचनाओं के बाजारीकरण के खिलाफ एक विद्रोह के रूप में देखते हैं। यह ब्लागर्स की वजह से हुआ कि 2006 में टाइम मैगजीन ने ‘यू’ को पर्सनैलिटी आफ द ईयर चुना, ‘यू’ मतलब आम नागरिक जो अपनी बात कह सकता है।
मृणाल कहिन : खबरिया चैनल तथा ब्लॉग एक हद तक खबरों या गॉसिप की भूख मिटा सकते हैं, लेकिन चैनलों की तुलना में अखबारों की कवरेज बहुआयामी होती है। उसमें सिर्फ स्टोरी ही नहीं, उसका वरिष्ठ संवाददाताओं तथा संपादकों द्वारा बाकायदा विश्लेषण और उसकी अदृश्य पृष्ठभूमि से जुड़े तमाम तरह के ब्योरे और जानकारियां भी मौजूद होते हैं। इंटरनेट की भाषायी पाठकों तक अभी वैसी पहुंच भी नहीं बनी है, जैसी कि अंग्रेजी पाठकों की।
मेरा मत : यह बात भी भ्रामक है। इंटरनेट एक ज्यादा लोकतांत्रिक माध्यम है। यहां आप के लिखे पर कुछ ही घंटों के भीतर टिप्पणियों की भरमार लग सकती है और यह सभी भाषाओं में हो रहा है। दक्षिण भारत ने इंटरनेट को एक भाषाई माध्यम के रूप में एक्स्प्लोर किया है। हिन्दी इतने प्रभावशाली ढंग से इंटरनेट परिदृश्य में उभरकर सामने आई है कि गूगल और याहू जैसी कंपनियां अपना एक बड़ा वक्त अनुवाद और लिप्यांतरण की तकनीकी के शोध में खर्च कर रही हैं जो कि वास्तव में हमारी सरकार को खर्च करना चाहिए। हम यह जानते हैं कि इसके पीछे इन बड़ी कंपनियों का मकसद पैसा कमाना है मगर आने वाले दिनों में ये बदलाव करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। हकीकत यह है कि अंग्रेजी अखबारों की देखा-देखी लाइफस्टाइल और सिनेमा पर सामग्री परोसने की होड़ में शामिल हिन्दी पत्रकारिता का सारा कंटेट दोयम दर्जे का और इंटरनेट से चुराया हुआ होता है। जाहिर है, वेब से कंटेंट चोरी का यह मसला संपादकों के संज्ञान में अच्छी तरह होता है।
मृणाल कहिन : हिन्दी पत्रकारों ने छोटे-बड़े शहरों में मीडिया में खबर देने या छिपाने की अपनी शक्ति के बूते एक माफियानुमा दबदबा बना लिया है। और पैसा या प्रभाववलय पाने को वे अपनी खबरों में पानी मिला रहे हैं। सरकारी नियुक्तियां, तबादलों और प्रोन्नतियों में बिचौलिया बनकर गरीबों से पैसे भी वे कई जगह वसूल रहे हैं, और भ्रष्ट सत्तारूढ़ मुफ्त में नेताओं को ओबलाइज करके उनसे सस्ते या जमीनी और खदानी पट्टे हासिल कर रहे हैं, इसके भी कई चर्चे हैं। चूंकि एक मछली भी पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, हिन्दी में कई अच्छे पत्र और पत्रकारों की उपस्थिति के बावजूद हमारे यहां आम जनता के बीच भाषायी पत्रकारों का नाम बार-बार अप्रिय विवादों में उछलने से अब उनकी औसत छवि बहुत उज्ज्वल या आदरयोग्य नहीं है।
मेरा मत : यह कौन तय करेगा कि एक कस्बे में बैठा पत्रकार भ्रष्ट है और बडे़ स्तर पर उद्योगपतियों और राजनेताओं से सांठगांठ करने वाले प्रधान संपादक, स्थानीय संपादक, सहायक संपादक और प्रिंसिपल कारोस्पाडेंट आदि साखदार, पगड़ी वाले, ईमानदार और उज्जवल छवि वाले हैं। मृणाल पांडेय ने खुद सारी पत्रकारिता बिरादरी को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक कुलीन पत्रकार और दूसरे छोटे-मोटे छुटभैये, उठाईगिरे, भ्रष्ट, कुत्ता टाइप पत्रकार, जो कुलीन पत्रकारों को देखकर अपने ब्लाग मे भौंक रहे हैं। इनका बस चले तो ब्लागस्पाट और वर्डप्रेस जैसी होस्टिंग देने वाली साइट्स को ही बंद करा दें। एक अखबार के संपादक को कतई गवारा नहीं है कि इन ब्लाग्स पर कोई खुद को अभिव्यक्त करे। कीचड़ हर किसी पर तो नहीं उछलता, जहां उछल रहा है वहां कुछ तो गड़बड़ होगी ही, नहीं होगी तो फिर घबराने की क्या बात है?