आज जुझारू पत्रकार हैं पर योग्य संपादक व जुझारू प्रबंधन का अभाव : एक भरोसेमंद मीडिया साइट के अनुसार अभी हाल में दो महिला पत्रकार बुरी तरह उलझ पड़ी। एक का आरोप था कि दूसरी ने अपने दोस्त की मदद लेकर उसका स्टोरी आइडिया एकाधिक बार चुराया था। मामला पुलिस तक गया। बाद में रफा-दफा करवा दिया गया। एक अन्य अखबार ने अपनी साइट पर पहले एक नकली स्टोरी डाली, फिर उसे भी टीपने वाले चैनलों ने अखबारी साइटों के नाम सप्रमाण छापे।
नक्सल प्रभावित एक पूर्वी राज्य के बड़े अखबार ने (कथित तौर से सरकारी विज्ञापनों की एवज में) अपने प्रमुख संवाददाता की एक महत्वपूर्ण रपट श्रृंखला रुकवा दी जो राज्य के कुछ बड़े अफसरों को (नक्सली निरोधक प्रकोष्ठ के एक गुप्त अकाउंट में) हेराफेरी के आरोप तले कठघरे में खड़ा करवा सकती थी। उधर प्रेस काउंसिल ने देश के दो बड़े अखबारों के संदर्भ में चुनाव काल में पैसा लेकर खबरें छापने के इल्जाम सही पाए और उन पर समुचित कार्रवाई के लिए कागज चुनाव आयोग को भेज दिए हैं।
कुल मिला कर खबर अच्छी नहीं है। सूचना और संप्रेषण में अभूतपूर्व तरक्की के युग में अखबारों से वे ठोस, खोजपूर्ण और विश्वसनीय खबरें लगातार गायब हो रही हैं, जिनकी मार्फत हम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र की खबरें और अदालती सुनवाइयों और व्यवस्था के साफ-सुथरे खुलासे, नगर और ग्राम निकायों में कामकाज निबटाई या ठहराव की बाबत महत्वपूर्ण ब्योरे, वित्तीय नीतियों के गठन और संशोधन की सूचनाएं और जन जीवन पर असर डालने वाले हर तरह से संसदीय फैसलों का चरण दर चरण खुलासा पाते रहे हैं। राज समाज से बेझिझक जवाब तलब करने वाली ऐसी खबरें तादाद में कम होते हुए भी हर तरह की पत्रकारिता की धुरी हैं। और उनसे सिर्फ मीडिया में काम करने वाले या सत्ता में बैठे लोगों की नहीं, बल्कि आम पाठक की बुद्धि भी हर दिन अपने चारों तरफ की दुनिया में हो रही घटनाओं से सही तरह जुड़ पाती है।
इन हार्ड खबरों को कुछ मीडिया-मालिक भले गैरजरूरी और अपठनीय करार दे चुके हों, सच तो यह है कि वे जब भी (अक्सर अखबारों और न्यूज एजेंसियों के ही) अनुभवी और समर्पित पत्रकारों द्वारा महीनों की मेहनत से जुटाए ठोस प्रामाणिक ब्योरों और गंभीर शोध के वजन के साथ उजागर होती हैं, मिनटों में नेट से लेकर टिवटर तक हर तरह के मीडिया में प्रमुखता से छा जाती हैं। उन्हीं के प्रमाण से उस दिन के संपादकीय लेख लिखे जाते हैं, उस सत्र की संसदीय जिरहें चलती हैं, रुकी तफतीश शुरू होती है, जांच आयोग बिठाए जाते हैं। खबरों की इस दुनिया का नेता या अभिनेता भी कई बार बकवास करार दे चुके हैं, पर उनसे लेकर कामेडी मंच पर मीडिया की हंसी उड़ाने वाले मसखरों तक किसी की भी बात खबर के संदर्भ बिना नहीं बनती। तब क्या वजह है कि हमें हाल के दिनों में रुचिका, जेसिका लाल से लेकर नितीश कटारा हत्याकांड तक कई संगीन मामलों में पेशेवर पत्रकारों की तुलना में मृतक की मित्र, बहन या मां जांच का अस्पताल से अदालत तक कहीं अधिक बेझिझक निडरता से पीछा करती दिखाई दी।
दरअसल, आज सत्ता के दबाव ही नहीं, खुद अनेक बड़े मीडिया संस्थानों के नए आर्थिक दर्शन और उनकी व्यवस्था से बढ़ती करीबी ने पेशेवर पत्रकारों के लिए ईमानदारी से खबरों का संधान करना और संपादकों के लिए दबंगई से उनको छापना बड़ा मुश्किल बना डाला है। इसमें दो राय नहीं कि लगातार अच्छी खबरें जुटाना एक महंगा, जोखिम भरा और श्रमसाध्य सौदा है। इसके लिए मीडिया संस्थान को सिर्फ कुशल, अनुभवी पत्रकार नहीं, एक ईमानदार धैर्यवान संपादक, जो अपने संवाददाताओं को जरूरी शोध और समाचार आकलन के लिए जरूरी संसाधन दिलवाए, फिर विवाद उठने पर (जो कि अनिवार्य है) अपनी खबर संवाददाता के पक्ष में तन कर भी खड़ा रहे और कोई भी कीमत चुका कर अखबार के सत्य का पहरुआ बना रहने वाला दमदार प्रबंधन भी चाहिए।
आज जुझारू पत्रकार हैं, पर हम सब देख रहे हैं कि शेष दो तत्वों में काफी हद तक लोचा लग चुका है। कभी-कभार किसी अरुंधति, पी साईनाथ या तीस्ता सीतलवाड की (मूलत: एक्टिविस्ट) कलम से ही सच्ची खोजपरक खबर सामने आ पाती है। जब तक अखबार, खबरिया चैनल, सर्चइंजिन या ब्लॉग सब सानिया की शादी या आइपीएल की बरबादी जैसी ‘खबरों’ पर ‘ब्रेकिंग न्यूज’ की चिप्पी लगा संपादकीयों और पैनल चर्चाओं में उन्हीं की जुगाली करते रहते हैं। अमेरिका में सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक, लास एंजलीस टाइम्स, का हश्र हमें इस प्रक्रिया की खतरनाक अंतिम परिणति दिखाता है।
खबरों का गर्वीला गढ़ रहा यह अखबार आज दिवालिया है। 1881 से यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक और खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में तो रिपोर्टरों के लिए मानक माना जाता था। पर 1995 में अखबार का प्रबंधन बदला और इसकी बागडोर नई चाल के बाजार विशेषज्ञ मार्क विलिस के हाथों में आई। उसने कहना शुरू किया कि आखिर अखबार या सुबह के नाश्ते में खाए जाने वाले सीरियल कि निर्माण या बिक्री में फर्क क्यों हो? क्यो दोनों ही महज पैसा कमाने के लिए बने उपभोक्ता उत्पाद नहीं? फिर विलिस ने अखबार में आज हार्ड खबर कौन पढ़ता है सिवा पत्रकारों के,-कह कर कंपनी के खर्चे घटाने की मुहिम छेड़ी और ब्यूरो के आधे से ज्यादा वरिष्ठ पत्रकारों की छुर्ष कर डाली। इसी के साथ नए उपभोक्ता की बदलती रुचि का हवाला देकर संपादकीय की सलाह के खिलाफ मार्केटिंग टीम के निर्देश तले मनोरंजन प्रधान हल्की-फुल्की खबरों से अखबार को भर दिया गया।
मीडिया जगत में ‘सीरियल किलर’ नाम से नवाजे गए विलिस की रणनीति अधिक पाठक या पैसा दिलवाने में जब नाकाम रही, तब 1999 में अखबार ने रेवेन्यू साझेदारी के नाम पर खेल स्टेडियम बनाने वाली एक कंपनी से समझौता किया। जब पत्रकारों को पता चला कि उनके अखबारों में एक खास खेल परिशिष्ट सिर्फ इसलिए शुरू किया गया है कि उसमें उनकी विशेषज्ञता की ब्रांडिंग द्वारा खेल खबरों को झुका कर उस कंपनी के हर उत्पाद को बढ़िया घोषित किया जा सके तो त्यागपत्रों का सिलसिला शुरू हो गया। आखिरकार विलिस तो विदा कर दिए गए पर अच्छे पत्रकारों से रिक्त अखबार अंतत: 2008 में दिवालिया घोषित कर दिया गया।
आईपीएल के हश्र और उपरोक्त वाकए से हमको सबक लेना चाहिए। सत्ता और सत्तावान तो हर युग में, हर देश में अपनी जरूरतें करने को साम-दाम-दंड अपना कर हर कमाऊ संगठन के लीवरों को अपने कब्जे में कर लेने की जुगत भिड़ाते रहे हैं, पर प्रबुद्ध और अंतरात्मावान मालिक जब तक उनको क्षेत्र की बुनियादी गुणवक्ता का अतिक्रमण नहीं करने देते, संस्थान बचे रहते हैं। हां, वाशिंगटन पोस्ट की संपादक-व्यवस्थापक कैथरीन ग्राहम ने जरूर कहा था कि अपनी जरूरत लायक पैसा कमाना आजाद पत्रकारिता की बुनियादी शर्त है, लेकिन बहुत जल्द, बहुत ज्यादा कमाई दुह लेने के फेर में पत्रकारिता की बुनियादी मर्यादाओं को नजरअंदाज कर खतरनाक व्यावसायिक फैसले करना, खबर पाने-देने के जरूरी खर्चों में लगातार कटौतियां करने के साथ इवेंट मैनजमेंट और प्रबंधन के बोनस सरीखी विवादास्पद मदों पर कमाई न्योछावर करना परतंत्रता और पतन की गारंटी बन सकता है। साभार : जनसत्ता














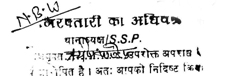
govind goyal.sriganganagar
April 18, 2010 at 5:50 am
jandar,shandar,damdar. ekdam sachchi suchchi bat.narayan narayan
Rakesh bhartiya
April 18, 2010 at 10:32 am
16 aanney such hai bhi…….kya khub lhika hai !! 99 percent papers ka abb yahi haall hai
Sunit
April 20, 2010 at 7:52 am
जिस पूर्वी राज्य के अखबार में प्रमुख संवाददाता की खबर रोकने की बात मृणाल पांडे कह रही हैं, उस अखबार में उस समय प्रधान संपादक मृणाल पांडे खुद थीं। मृणाल पांडे खुद को कैसे इस जिम्मेदारी से अलग कर सकती हैं। दरअसल, सुनी-सुनाई और घटिया पत्रकारों की कही बातों को सही मानकर कलम घिसना नहीं शुरू कर देना चाहिए। मृणाल जी जिस संपादक ने खबर रोकी वह संपादक खुद कितने मामलों में फंसा दिखाई दे रहा है। आपको भी सब खबर थी लेकिन आपने उसे कभी हटाने की हिम्मत नहीं की।
बाहर बैठकर आरोप लगाना और सिद्धांत बघारना ठीक नही है। पहले यह देखिए आपके समय में उस पूर्वी राज्य में उस महान संपादक ने क्या-क्या सदकर्म किए और उनका जवाब अपने किसी लेख में दीजिए। इंतजार रहेगा…..
shashi chaturvedi
April 22, 2010 at 4:52 am
Sau baat kee ek baat , mrinal ji ke samay men he is tarrar ptrkaar kee rapat chhpee thee , unke jane ke baad na sirf shesh kadiyan naheen chhpne dee gyeen , bulki us patrkaar ko bhee ( shayad vigyapan dataon kee ahat bhavnaon ka khayal karte huey ) chandigarh sthanatarit ker diya gaya , jiske baad shayad unhoney isteefa de diya hai . . Apnee nijee eershya mein tathyon kee andekhee to na karein bhai sahib !