पंकज मिश्रा-
जय भीम की एडिटिंग जबरदस्त है , बांधे रखती है | बेहद लाउड फ़िल्म है , हिंसा के दृश्यों से जुगुप्सा पैदा होती है इसे थोड़ा हल्का किया जा सकता था , हिंसा की मेसेजिंग के नए टूल ढूंढने की जरूरत है ताकि बिना खून खराबे के भी हिंसा की भयावहता दिखाई जा सके जैसे की निराला ने लिखा था ” मार खा रोई नही”.
यथार्थ को जस का तस परोस देना किसी भी कला रूप की कमी मानी जाती है | यथार्थ चित्रण इस तरह हो कि उसके इम्पैक्ट की विभीषिका बिना विभत्स हुए बिना जुगुप्सा के भी उतना ही दहला दे.
पुलिस के साजिशाना चरित्र को जरूर दिखाया गया मगर जैसे ही वह expose होती है उसका इतना meek surrender गले से नही उतरता | व्यवस्था इतनी आसानी से सरेंडर नही करती | फ़िल्म में न्यायपालिका को बेहद न्यायप्रिय , मानवीय और सम्वेदनशील दिखाया गया है परंतु वास्तविक जीवन मे वह भी व्यवस्था का ही एक अंग होती है | न्यायपालिका व्यवस्था से विच्छिन्न नही बल्कि उससे अभिन्न होती है | यह द्वैत भी आसानी से पचने वाला नही है | वैसे देखने और गुनने लायक फ़िल्म है … ऐसी और फिल्में बननी चाहिए.
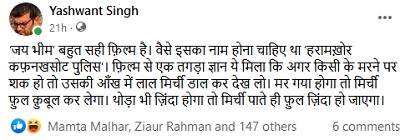
Rangnath Singh-
‘जय भीम’ प्रेरणादायक फिल्म है। वकील चंद्रू का चरित्र वैसा ही है जैसे अन्धेरे बन्द कमरे में जलता एक दीया। इस व्यवस्था में एक व्यक्ति अपने प्रयास से चन्द लोगों को भी न्याय दिला सके तो वह हमारे लिए प्रेरणास्रोत है। इस तरह के नायकों को सामने लाने वाली फिल्में जितनी अधिक बनें, उतना अच्छा।
जज चन्द्रू का इसी हफ्ते छपा एक साक्षात्कार पढ़ा। उन्हें आपातकाल के दौर में समझ आ गया था कि काले कोट में वो ज्यादा बेहतर तरीके से वंचितों-शोषितों के लिए आवाज उठा सकते हैं। उनका फैसला सही भी साबित हुआ। वकील और फिर जज के तौर पर आज वो एक बड़ी अवाम के रोल मॉडल के रूप में हमारे सामने हैं।
इसी बीच रामगोपाल वर्मा की ‘रक्तचरित्र’ देखी। वह फिल्म भी जातीय संघर्ष को केंद्र में रखकर कही गयी अपराध कथा लेकिन उसका स्टाइल मसाला फिल्मों वाला है। दोनों फिल्मों में साझी चीज यह है कि दोनों में ही पुलिस अपराधियों का साथ देती है।
Sanjeev Chandan-
जय भीम: सिनेमा और यथार्थ
जय भीम फिल्म देखी। यह अम्बेडकरवादी फिल्म तो कतई नहीं हैं, लेकिन शीर्षक है तो कई कारणों से उसके करीब है। एक डायलाग भी है बाबा साहेब अम्बेडकर को भूला दिए जाने को लेकर। वामपन्थी मिजाज से जितना अम्बेडकरवादी हुआ जा सकता है उतना है, या संविधान में, क़ानून में विश्वास के हिसाब से भी, अन्यथा तो लाल झंडे स्पष्ट कर देते हैं फिल्म और इसके नायक की विचारधारा।
यह दलित-आदिवासी संघर्ष की अबतक की कोई महान फिल्म भी नहीं हैं, फार्मूला ज्यादा है।
जिन दिनों वर्धा में टाइम्स की पत्रकारिता कर रहा था उन दिनों सूचना मिली कि कुछ घूमंतू जाति के लोगों को पुलिस उठा ले गई। कहां, ले गई? न वर्धा के थानेदार को मालूम, न एसपी को। उन्हें लग भी नहीं रहा था कि वे पता करें। जैसे रुटीन सा हो। आन्ध्रा की पुलिस थी। हम खबर करते रहे, लेकिन उनका पता न चला। यह भी पता चला कि ऐसे पिक अप का इस्तेमाल कई पेंडिंग केसेज को निपटाने में होता है।
फिल्म की कहानी ऐसे ही आदिवासियों के रैन्डम पिक अप को लेकर है। यथार्थ है। पीड़ित आदिवासी हैं या मुसहर हैं। फिल्म में दिखाये जीवन वाले लोग उत्तर भारत में मुसहर होते हैं, जो शिड्यूल्ड कास्ट माने जाते है- मार्जिन पर जीने वाला मजदूर् समूह। उनकी लडाई लड़ने वाला कोई गैर दलित है, जो क़ानून और सडक पर संघर्ष में विश्वास रखता है।
जो कोर्ट है, वकील का काम है, उसका जीवन है वह इतना मेलो ड्रामा वाला नहीं होता है, जैसा दिखाया गया है। ऐसे आदिवासियों के वास्तविक संघर्ष के साथी वकील हमारे मित्र हैं। सुरेन्द्र गडलिंग जेल में हैं। निहाल सिंह भीमा कोरेगांव सहित ऐसे अनेक केस लड़ रहे हैं। हैबियस कार्पस का एक केस लडने की नौबत तो आ गई कि उनके ऑफिस से ही पुलिस दो आदिवासियों को उठा ले गई। नागपुर हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार कोर्ट की एक बेंच रविवार को बैठी।
यथार्थ का यह वकील आदिवासी ही है, अम्बेडकरवादी और मार्क्सवादी भी है। मुझे फिल्म देखते हुए नायक की जगह वे दिखते रहे और यथार्थ व फिक्शन का फर्क भी दिखता रहा। फिल्मों की सीमा है कि कोर्ट रूम पर बनी फिल्मों का हर नायक वकील जग्गा जासूस भी हो जाता है।
Abhishek Srivastava-
‘जय भीम’ क्यों देखें… शुरुआती आधे घंटे की जबरदस्त चटान के बाद किसी तरह लय बनी, तक जाकर ‘जय भीम’ निपटी। इस बीच बार-बार गोविंद निहलानी के किरदार भीखू लहानिया, भास्कर कुलकर्णी, दुशाने, भोंसले, डॉक्टर पाटील आदि याद आते रहे।
पूरे सवा दो घंटे मैं सोचता रहा कि काश, ये निर्देशक एक भी किरदार- वकील से लेकर डॉक्टर, समाजकर्मी और नेता तक- उस मेयार का रच पाता जो आज से चालीस साल पहले ‘आक्रोश’ में निहलानी ने कर दिखाया था। एजेंडाबद्ध रचनाकर्म कितना लाउड और लाचार हो सकता है, ‘जय भीम‘ इसका बेहतरीन उदाहरण है। इसे मिल रही अतिरिक्त चर्चा इस समाज के रचनात्मक रूप से भ्रष्ट और जातिगत स्तर पर रूढ़ व ध्रुवीकृत हो जाने का सबूत है।
‘जय भीम‘ और ‘आक्रोश‘ में अंतर क्या है?
‘जय भीम’ की तरह ‘आक्रोश’ के केंद्र में भी आदिवासी थे। वहाँ भी एक समाजकर्मी था। एक वकील था। एक पब्लिक प्रासिक्यूटर था। पुलिस थी। नेता थे। अन्याय था। अन्याय के खिलाफ कानूनी संघर्ष था। दोनों फिल्में सच्ची घटना पर आधारित हैं। अंतर क्या है? चालीस साल पहले दिखाया गया भ्रष्टाचार कार्यपालिका से लेकर न्यायपालिका तक सबको कठघरे में खड़ा करता है और आदिवासी को अकेला छोड़ देता है।
2021 में 1995 की घटना पर दिखाया गया भ्रष्टाचार न्यायपालिका को डिस्काउंट दे देता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि ‘जय भीम’ का नायक चंदरू अम्बेडकरवादी है और कानून के रास्ते अन्याय का प्रतिकार करने में यकीन रखता है (जिसका किरदार निभाने वाले हीरो सुरिया को ‘यादव’ जाति का बताकर प्रचारित किया जा रहा है)? तीनों जज भी बड़े भले हैं। निहलानी को अन्याय का प्रतिकार दिखाने के लिए ‘भीम’ के नाम की जरूरत नहीं थी, बल्कि सरकारी वकील दुशाने यानि अमरीश पुरी वहाँ खुद आदिवासी समुदाय से होते हुए अन्याय का पोषक था। ये अपने समय से बहुत आगे की बात थी।
‘जय भीम’ के निर्देशक आदि बहुत भले हैं। यथार्थवादी सिनेमा का पर्याय केवल रोते हुए चेहरे और चीख-चिल्लाहट को समझते हैं; 1995 में कुर्ता पहने और झोला लटकाए एक पत्रकार को हाथ में गन माइक लिए रिपोर्टिंग करते दिखाते हैं; नायक वकील को विशुद्ध दक्षिण भारतीय फिल्मों जैसा सुपरमैन दिखाते हैं और अदालत में सुनवाई के दौरान घूमते हुए नंगे बच्चे दिखाते हैं। हो सकता है कि ये शायद उतने भले भी न हों चूंकि आदिवासी पृष्ठभूमि की कहानी में इन्होंने एक ओर नायक को अम्बेडकरवादी दिखाया है तो दूसरी ओर गाँव के शोषक सामंत की जाति छुपा ली है। चूंकि दक्षिण भारत के जाति समीकरण का मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, इसलिए मोटे तौर पर लगता है कि फिल्म की पूरी डिजाइन आदिवासी अस्मिता को दलित प्रतीकों (और ओबीसी विमर्श) के भीतर पचा ले जाने की है। ठीक वैसे ही जैसे एक खास किस्म का ओबीसी विमर्श दलित अस्मिता के साथ घालमेल कर के उसे को-ऑप्ट करने में लगा रहता है। फिल्म में जाति संघर्ष की जटिलता को एक मोटी बाइनरी में बदल दिया गया है। ऐसा सरलीकरण 1995 में भी अपेक्षित नहीं था। पता नहीं ये चालाकी है या भोलापन! निहलानी इस मामले में बहुत ईमानदार थे।
एक समस्या और दिखी जिससे लेखक-निर्देशक पर शक होता है। जिस पुलिस अधिकारी को (प्रकाश राज) दूसरे नायक और आदिवासियों के हितैषी के रूप में स्थापित किया गया है, उसकी समझ ये है कि कभी-कभी गणतंत्र को कायम रखने के लिए तानाशाही जरूरी होती है। दिलचस्प ये है कि इसी अधिकारी के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित करने की सिफारिशी पर्ची भरी अदालत में जजों के पास खुद नायक भेजता है।
बहरहाल, ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन मुझे बुनियादी रूप से ‘जय भीम’ से ये शिकायत है कि पूरी फिल्म इतनी लाउड और नाटकीय होने के बावजूद मुझे छू नहीं पाती। इसके मुकाबले सैराट या फैन्ड्री या फिर पेरूमल, कोर्ट, मसान आदि कहीं ज्यादा संवेदनशील हैं और देखने वाले को संवेदनशील बनाती भी हैं। इस श्रेणी में श्याम बेनेगल की ‘अंकुर’ अमर है। ‘आक्रोश’ को मैं ‘अंकुर’ के ही क्लासिक विस्तार के रूप में देखता हूँ। इस परंपरा में ‘जय भीम’ कहीं नहीं अंटती है, न अंटनी चाहिए।
मेरा खयाल है कि ‘जय भीम’ इसलिए देखी जानी चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि अन्याय की किसी भी घटना पर इस हल्के और एजेंडाबद्ध तरीके से तो फिल्म बिल्कुल नहीं बननी चाहिए।
अरविंद शेष-
‘जय भीम’ को मैंने इस फिल्म के इस सीन और डायलॉग के जरिए समझा-
एक सीन में अदालत में चंद्रू जोरदार तरीके से भारी पड़ता है तो अदालत में ‘सिस्टम रिप्रेजेंटेटिव’ की भूमिका में दिखने वाला एक वकील चंद्रू की तारीफ करता है और कहता है कि तुम मास्टर स्ट्रोक खेल गए और ये केस तुम्हारे फेवर में आ चुका है, तब चंद्रू कहता है-
“मुझे ऐसा लग रहा कि मैं कोई गलती कर रहा हूं! …नहीं सर, अगर आपको मुझ पर इतना भरोसा है तो मतलब कि मैं पक्का कोई गलती कर रहा हूं! कुछ तो ऐसा है, जिसे मैं नहीं देख पा रहा हूं!”
“जय भीम” की तारीफ कहां-कहां से हो रही है, कौन-कौन कर रहा है, इस पर नजर डालिए, गौर करिए और “जय भीम” के इस दृश्य और डायलॉग को याद कीजिए!
व्यवस्था के कब्जेदार और वंचितों के दुश्मन जब व्यवस्था के वंचितों की किसी लड़ाई की तारीफ करने लगें, उनकी जीत को लेकर भरोसा जताने लगें तो यह इस बात का इशारा है कि वह लड़ाई आखिरकार व्यवस्था के ही हक में जाएगी!
इसलिए “जय भीम” का यह दृश्य और डायलॉग मेरी नजर में बेहद अहम है!
तकरीबन बीस साल बाद ‘आक्रोश’ फिर देखा! इसलिए कि आजकल इसकी चर्चा ‘जय भीम’ के संदर्भ में हो रही है! गोविंद निहलानी, ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह और अमरीश पुरी वाली ‘आक्रोश’ ने बीस साल पहले हिला दिया था!
रात देखा तब समझ में आया कि आज ‘जय भीम’ इसकी तुलना क्यों की जा रही है… ‘जय भीम’ से बेहतर बताते हुए!
ऐसी तारीफें कई बार किसी अनदेखी कर दी गई चीजों पर से पर्दा उठाने की प्रेरणा देती हैं! ‘जय भीम’ के समांतर ‘आक्रोश’ गड़बड़ है!
विद्वानीयत के कारोबारी मेरे वे मित्र फिर कहेंगे कि इसकी समझदारी लापता हो गई है!
हालांकि मैं ‘जय भीम’ पर बहुत मुग्ध नहीं हूं, लेकिन इसके कई दृश्यों में निर्देशक और इसके कुछ कलाकारों ने बेमिसाल भाव पैदा किया!
