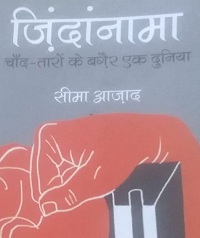

Priya Darshan : वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नहीं, मनमोहन सिंह और पी चिदंबरम का दौर था। 6 फरवरी 2010 को मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार सीमा आज़ाद दिल्ली के पुस्तक मेले से ढेर सारी किताबें ख़रीद कर ट्रेन से इलाहाबाद लौट रही थीं। स्टेशन पर पति विश्वविजय लेने आए हुए थे। दोनों बाहर निकलने को थे कि अचानक एक गाड़ी आई, उसमें से 10-12 लोग उतरे और उन्होंने पति-पत्नी को गाड़ी के भीतर जबरन घसीट लिया।
वह एसटीएफ़- यानी स्पेशल टास्क फोर्स- की टीम थी। इसके बाद अगले दो साल से ऊपर का समय पति-पत्नी को जेल में काटना पड़ा। बाहर आकर दोनों ने यह कहानी लिखी है जो अब ‘ज़िंदांनामा’ के नाम से दो किताबों की शक्ल में प्रकाशित हुई है।
इन दोनों किताबों में सीमा आज़ाद और विश्वविजय ने बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरह उनके ख़िलाफ़ केस बनाया गया, उनके बयान तोड़े-मरोड़े गए, क़ानून का मनमाने ढंग से इस्तेमाल हुआ और और एक ऐसी कहानी गढ़ी गई जिसमें दोनों खूंखार माओवादी बना दिए गए। ऐसा नहीं कि ये बहुत नाटकीय ब्योरों वाली किताबें हों जिनमें पुलिस यंत्रणा के डरावने दृश्य हों। लेकिन फिर भी ये किताबें डराती हैं। डर के साथ एक उदासी पैदा करती हैं। याद दिलाती हैं कि हमने सुरक्षा के नाम पर कैसा अमानुषिक तंत्र खड़ा कर लिया है। अंग्रेजों के ज़माने वाले जनविरोधी क़ानूनों से लैस और लगभग उसी संस्कृति में प्रशिक्षित हमारी कानूनी एजेंसियां जैसे जनता को अपना दुश्मन समझती हैं और इंसाफ़ की मांग को बग़ावत। उनका काम जैसे यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी नागरिक अपने अधिकार मांगने की हिम्मत न करे, दूसरों के न्याय की कोई लड़ाई न लड़े। इन दो लोगों को दो साल तक एक फ़र्ज़ी मुक़दमे में फंसा कर रखा गया, सुप्रीम कोर्ट तक इनकी ज़मानत नहीं होने दी गई, निचली अदालत से दोनों को उम्रक़ैद की सज़ा भी हो गई।
यह जिनके साथ घटा, उन्हीं को तोड़ने वाला वाकया नहीं था। यह दरअसल दूसरों के लिए भी उदाहरण था कि नागरिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने का हश्र क्या हो सकता है। यह अनायास नहीं था कि आने वाले दिनों में सीमा आज़ाद और विश्वविजय के मित्रों की संख्या कम होती चली गई। जब वे कचहरी में आते थे तो एसटीएफ़ के लोग उन पर दबाव बनाते थे, उनकी तस्वीर लेते थे। अब इस व्यवस्था में किसको यह पूछने की हिम्मत है कि क्या उसकी तस्वीर लेना उसकी निजता का उल्लंघन नहीं है?
बहरहाल, इन दोनों लेखकों ने अपनी जेल-कथा विस्तार से लिखी है- ख़ास कर सीमा आज़ाद ने- और इन्हें पढ़ते हुए अगर एक स्तर पर डर और अवसाद पैदा होता है तो दूसरे स्तर पर हिम्मत भी मिलती है। सीमा आज़ाद ने जेल के भीतर की दुनिया विस्तार से दिखाई है। यह दुनिया फिर से याद दिलाती है कि हमारी व्यवस्था में अन्याय की जड़ें कितनी गहरी हैं। यह भी याद आता है कि अन्याय का सिलसिला सबसे ज्यादा घातक सबसे कमज़ोर आदमी के लिए होता है। लेकिन अगर आप उस कमज़ोर आदमी के पक्ष में न खड़े हो सकें तो देर-सबेर यह आपको भी अपनी चपेट में ले सकता है। जेलों की बंद दुनिया में अपराधी जैसे बनाए जाते हैं- भ्रष्टाचार, क्रूरता और हिंसा के साथ-साथ लगभग अमानवीयता को छूती बदइंतज़ामी किसी को मनुष्य रहने लायक नहीं छोड़ती। इन हालात में आप बीमार पड़ते हैं, आप अवसादग्रस्त हो सकते हैं, आप तनाव में ख़ुदकुशी तक कर सकते हैं। या अगर आप इन सब से बच निकलें तब भी किसी सनक, किसी पिनक में कोई आपको मार सकता है।
विश्वविजय और सीमा आज़ाद लेकिन फिर कैसे बचे रहे? इस सवाल के दो जवाब दोनों किताबों में मिलते हैं। एक तो ज़िंदगी की अपनी खूबसूरत ढिठाई है जो हर हाल में अपने लिए एक रास्ता, एक झरोखा खोल लेती है। सीमा आज़ाद बताती हैं कि जेल के भीतर की दुनिया में भी किस तरह ज़िंदगी अपने रास-रंग, पर्व-त्योहार सब खोज और मना लेती है। यह कुछ दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वहां बच्चे जन्म लेते हैं, बड़े हो जाते हैं और इस दौरान अपने जीने, खेलने और हंसने का सामान भी जुटा लेते हैं।
विश्वविजय और सीमा आज़ाद के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात है। ज़िंदगी के अलावा यह विचार की ताकत है जो उनको बचाए हुए है। वे वहां किताबें पढ़ते हैं। उन्हें अवतार सिंह पाश, धूमिल, बर्टोल्ट ब्रेख्त और पाब्लो नेरुदा बचाए रखते हैं। वे अपनी बैरक में भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारियों की तस्वीरें लगाते हैं और याद करते हैं कि उन्होंने अपने लक्ष्य के लिए कैसे कैसे-कैसे कष्ट सहे। यह स्मृति है जो उनको बचाती है। वे कविताएं लिखते हैं, टिप्पणियां लिखते हैं और इस बात को याद रखते हैं कि वे पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
ये दोनों किताबें पढ़ी जानी चाहिए- इसलिए नहीं कि इनमें दो लोगों के निजी संघर्ष की एक गाथा मौजूद है, बल्कि इसलिए कि इनमें वह विडंबना भी साफ़-साफ़ दिखाई पड़ती है जो हमारे देश में लगातार बड़ी होती जा रही है- यहां न्याय दुष्कर हुआ है, दूसरों के लिए बोलना ख़तरनाक और क़ानून लगातार कड़े होते जा रहे हैं।
जिस यूएपीए- यानी अनलॉफुल ऐक्टिविटीज प्रीवेंशन ऐक्ट के तहत सीमा आज़ाद और विश्वविजय को पकड़ा गया था, उसे पिछले दिनों कुछ और ताक़त दे दी गई है। अब इस क़ानून के तहत किसी को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। कहने की ज़रूरत नहीं कि अगर उन दिनों यह संशोधन हो गया होता तो शायद विश्वविजय और सीमा आज़ाद भारतीय राष्ट्र-राज्य की नज़र और उसके रिकॉर्ड में आतंकवादी होते।
क्या इत्तिफ़ाक़ है कि सीमा और विश्वविजय की गिरफ़्तारी के क़रीब 9 साल बाद सीमा के भाई और उनकी पत्नी को भोपाल के एक घर से गिरफ़्तार किया गया है। उन पर भी माओवादी होने का इल्ज़ाम है। सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि पिछली लड़ाई के अनुभव से कुछ सबक लेते हुए शायद यह परिवार इस बार कहीं ज़्यादा बेहतर लड़ाई लड़ सकेगा। लेकिन अब हालात अब पहले से ज्यादा बुरे हैं, सत्ता की बर्बरता और बदनीयती पहले से ज्यादा स्पष्ट है और मानवाधिकार के मोर्चे पर लड़ाई लगातार कमज़ोर की जा रही है। यह एक उदास करने वाला दृश्य है लेकिन ये किताबें भरोसा दिलाती हैं कि लड़ाई जितनी तीखी होगी, लड़ने के उतने ही नए तरीके निकलते जाएंगे।
‘ज़िंदांनामा’ फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की किताब का नाम है। ज़ाहिर है, लेखकों ने यह नाम रख कर एक परंपरा से अपने-आप को जोड़ा है। इस मोड़ पर फ़ैज़ फिर याद आते हैं:
यूं ही उलझती रही है ज़ुल्म से ख़ल्क
न उनकी रस्म नई है न अपनी रीत नई।
यूं ही हमने खिलाए हैं आग में फूल
न उनकी हार नई है न अपनी जीत नई।
लेकिन यह शेर पढ़ना और उद्धृत करना जितना आसान है, इसे जीना और मुमकिन बनाना उतना ही मुश्किल- यह बात भी ये किताबें कई तरह से याद दिलाती हैं।
वरिष्ठ पत्रकार प्रिय दर्शन की एफबी वॉल से.
